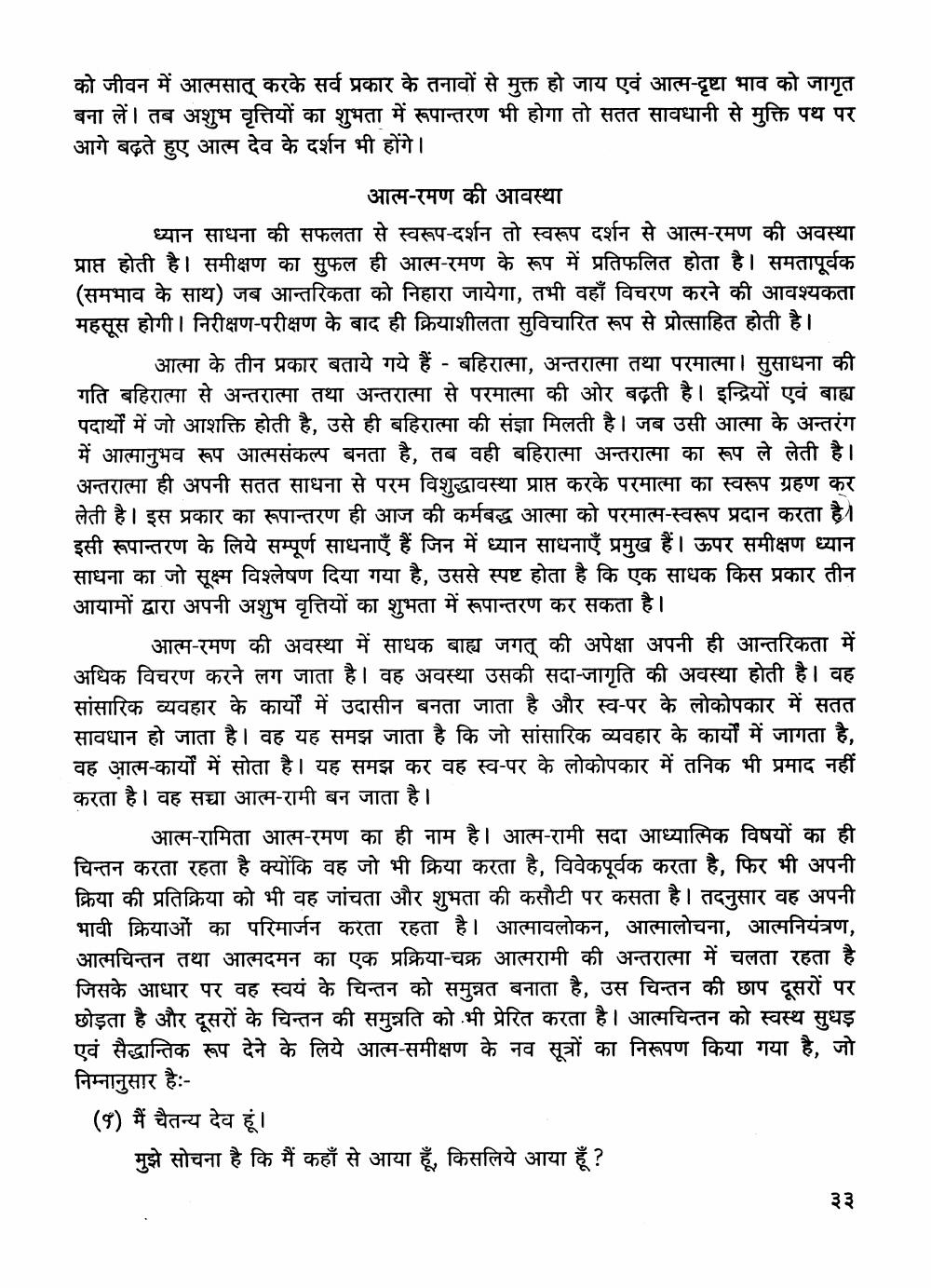________________
को जीवन
आत्मसात् करके सर्व प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाय एवं आत्म-दृष्टा भाव को जागृत बना लें। तब अशुभ वृत्तियों का शुभता में रूपान्तरण भी होगा तो सतत सावधानी से मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते हुए आत्म देव के दर्शन भी होंगे ।
आत्म- रमण की आवस्था
ध्यान साधना की सफलता स्वरूप-दर्शन तो स्वरूप दर्शन से आत्म- रमण की अवस्था प्राप्त होती है। समीक्षण का सुफल ही आत्म-रमण के रूप में प्रतिफलित होता है । समतापूर्वक (समभाव के साथ) जब आन्तरिकता को निहारा जायेगा, तभी वहाँ विचरण करने की आवश्यकता महसूस होगी। निरीक्षण-परीक्षण के बाद ही क्रियाशीलता सुविचारित रूप से प्रोत्साहित होती है ।
आत्मा के तीन प्रकार बताये गये हैं- बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा । सुसाधना की गति बहिरात्मा से अन्तरात्मा तथा अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ती है । इन्द्रियों एवं बाह्य पदार्थों में जो आशक्ति होती है, उसे ही बहिरात्मा की संज्ञा मिलती है। जब उसी आत्मा के अन्तरंग में आत्मानुभव रूप आत्मसंकल्प बनता है, तब वही बहिरात्मा अन्तरात्मा का रूप ले लेती है। अन्तरात्मा ही अपनी सतत साधना से परम विशुद्धावस्था प्राप्त करके परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार का रूपान्तरण ही आज की कर्मबद्ध आत्मा को परमात्म स्वरूप प्रदान करता है। इसी रूपान्तरण के लिये सम्पूर्ण साधनाएँ हैं जिन में ध्यान साधनाएँ प्रमुख हैं। ऊपर समीक्षण ध्यान साधना का जो सूक्ष्म विश्लेषण दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि एक साधक किस प्रकार तीन आयामों द्वारा अपनी अशुभ वृत्तियों का शुभता में रूपान्तरण कर सकता है।
आत्म- रमण की अवस्था में साधक बाह्य जगत् की अपेक्षा अपनी ही आन्तरिकता में अधिक विचरण करने लग जाता है। वह अवस्था उसकी सदा - जागृति की अवस्था होती है । वह सांसारिक व्यवहार के कार्यों में उदासीन बनता जाता है और स्व-पर के लोकोपकार में सतत सावधान हो जाता है। वह यह समझ जाता है कि जो सांसारिक व्यवहार के कार्यों में जागता है, वह आत्म- कार्यों में सोता है। यह समझ कर वह स्व-पर के लोकोपकार में तनिक भी प्रमाद नहीं करता है । वह सच्चा आत्म-रामी बन जाता है ।
आत्म-रामिता आत्म- रमण का ही नाम है। आत्म-रामी सदा आध्यात्मिक विषयों का ही चिन्तन करता रहता है क्योंकि वह जो भी क्रिया करता है, विवेकपूर्वक करता है, फिर भी अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया को भी वह जांचता और शुभता की कसौटी पर कसता है । तदनुसार वह अपनी भावी क्रियाओं का परिमार्जन करता रहता है। आत्मावलोकन, आत्मालोचना, आत्मनियंत्रण, आत्मचिन्तन तथा आत्मदमन का एक प्रक्रिया चक्र आत्मरामी की अन्तरात्मा में चलता रहता है जिसके आधार पर वह स्वयं के चिन्तन को समुन्नत बनाता है, उस चिन्तन की छाप दूसरों पर छोड़ता है और दूसरों के चिन्तन की समुन्नति को भी प्रेरित करता है। आत्मचिन्तन को स्वस्थ सुधड़ एवं सैद्धान्तिक रूप देने के लिये आत्म-समीक्षण के नव सूत्रों का निरूपण किया गया है, जो निम्नानुसार है:
(१) मैं चैतन्य देव हूं।
मुझे सोचना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसलिये आया हूँ ?
३३