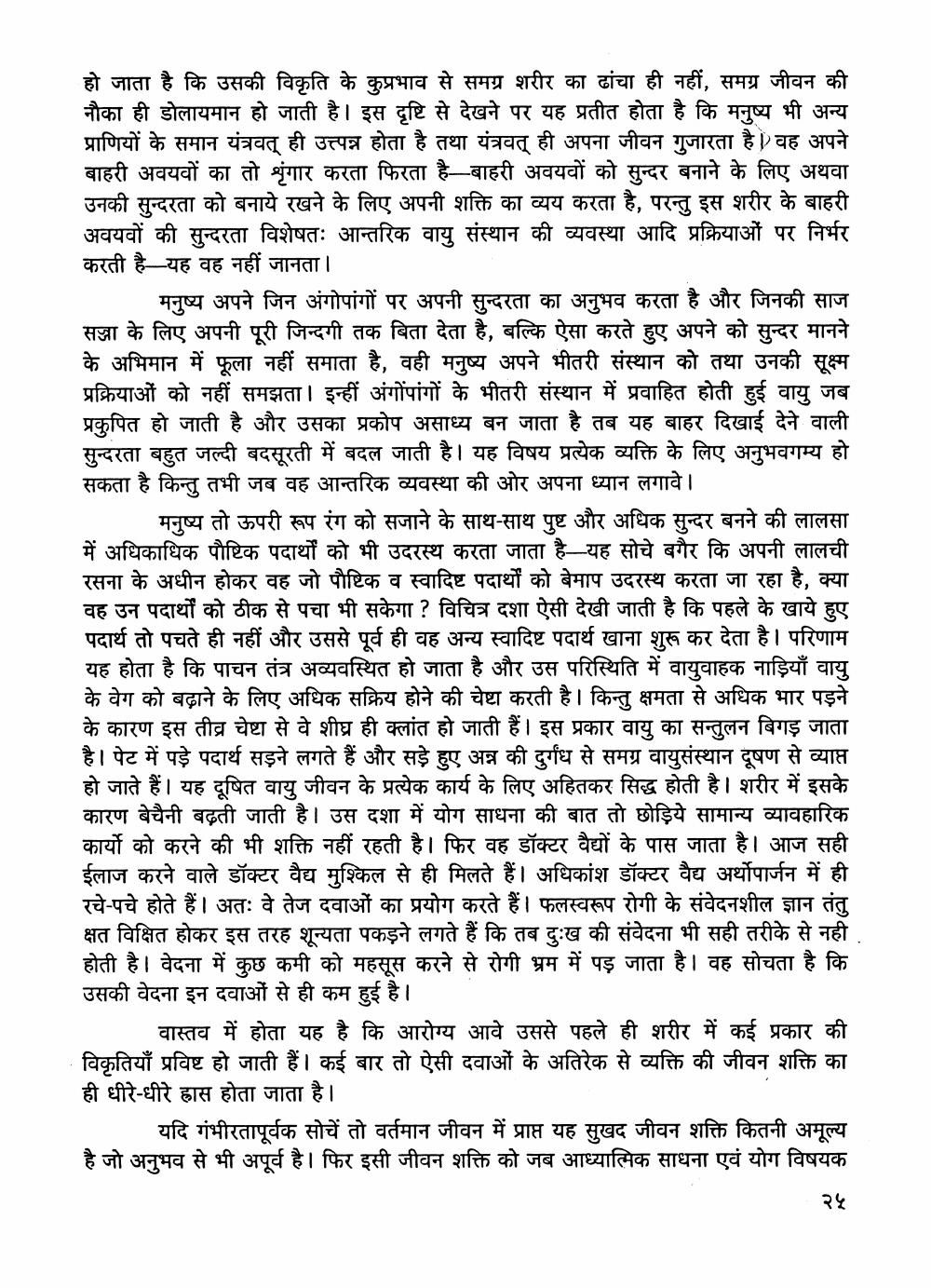________________
हो जाता है कि उसकी विकृति के कुप्रभाव से समग्र शरीर का ढांचा ही नहीं, समग्र जीवन की नौका ही डोलायमान हो जाती है । इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि मनुष्य भी अन्य प्राणियों के समान यंत्रवत् ही उत्त्पन्न होता है तथा यंत्रवत् ही अपना जीवन गुजारता है। वह अपने बाहरी अवयवों का तो शृंगार करता फिरता है—बाहरी अवयवों को सुन्दर बनाने के लिए अथवा उनकी सुन्दरता को बनाये रखने के लिए अपनी शक्ति का व्यय करता है, परन्तु इस शरीर के बाहरी अवयवों की सुन्दरता विशेषतः आन्तरिक वायु संस्थान की व्यवस्था आदि प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है - यह वह नहीं जानता ।
मनुष्य अपने जिन अंगोपांगों पर अपनी सुन्दरता का अनुभव करता है और जिनकी साज सज्जा के लिए अपनी पूरी जिन्दगी तक बिता देता है, बल्कि ऐसा करते हुए अपने को सुन्दर मानने के अभिमान में फूला नहीं समाता है, वही मनुष्य अपने भीतरी संस्थान को तथा उनकी सूक्ष्म प्रक्रियाओं को नहीं समझता। इन्हीं अंगोपांगों के भीतरी संस्थान में प्रवाहित होती हुई वायु जब प्रकुपित हो जाती है और उसका प्रकोप असाध्य बन जाता है तब यह बाहर दिखाई देने वाली सुन्दरता बहुत जल्दी बदसूरती में बदल जाती है । यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुभवगम्य हो सकता है किन्तु तभी जब वह आन्तरिक व्यवस्था की ओर अपना ध्यान लगावे ।
मनुष्य तो ऊपरी रूप रंग को सजाने के साथ-साथ पुष्ट और अधिक सुन्दर बनने की लालसा में अधिकाधिक पौष्टिक पदार्थों को भी उदरस्थ करता जाता है—यह सोचे बगैर कि अपनी लालची रसना के अधीन होकर वह जो पौष्टिक व स्वादिष्ट पदार्थों को बेमाप उदरस्थ करता जा रहा है, क्या वह उन पदार्थों को ठीक से पचा भी सकेगा ? विचित्र दशा ऐसी देखी जाती है कि पहले के खाये हुए पदार्थ तो पचते ही नहीं और उससे पूर्व ही वह अन्य स्वादिष्ट पदार्थ खाना शुरू कर देता है । परिणाम यह होता है कि पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है और उस परिस्थिति में वायुवाहक नाड़ियाँ वायु के वेग को बढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय होने की चेष्टा करती है । किन्तु क्षमता से अधिक भार पड़ने के कारण इस तीव्र चेष्टा से वे शीघ्र ही क्लांत हो जाती हैं। इस प्रकार वायु का सन्तुलन बिगड़ जाता है। पेट में पड़े पदार्थ सड़ने लगते हैं और सड़े हुए अन्न की दुर्गंध से समग्र वायुसंस्थान दूषण से व्याप्त हो जाते हैं । यह दूषित वायु जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए अहितकर सिद्ध होती है। शरीर में इसके कारण बेचैनी बढ़ती जाती है। उस दशा में योग साधना की बात तो छोड़िये सामान्य व्यावहारिक कार्यो को करने की भी शक्ति नहीं रहती है । फिर वह डॉक्टर वैद्यों के पास जाता है। आज सही ईलाज करने वाले डॉक्टर वैद्य मुश्किल से ही मिलते । अधिकांश डॉक्टर वैद्य अर्थोपार्जन में ही रचे-पचे होते हैं। अतः वे तेज दवाओं का प्रयोग करते हैं । फलस्वरूप रोगी के संवेदनशील ज्ञान तंतु क्षत विक्षित होकर इस तरह शून्यता पकड़ने लगते हैं कि तब दुःख की संवेदना भी सही तरीके से नही होती है। वेदना में कुछ कमी को महसूस करने से रोगी भ्रम में पड़ जाता है। वह सोचता है कि उसकी वेदना इन दवाओं से ही कम हुई है ।
वास्तव में होता यह है कि आरोग्य आवे उससे पहले ही शरीर में कई प्रकार की विकृतियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं। कई बार तो ऐसी दवाओं के अतिरेक से व्यक्ति की जीवन शक्ति का ही धीरे-धीरे ह्रास होता जाता है।
यदि गंभीरतापूर्वक सोचें तो वर्तमान जीवन में प्राप्त यह सुखद जीवन शक्ति कितनी अमूल्य है जो अनुभव से भी अपूर्व है। फिर इसी जीवन शक्ति को जब आध्यात्मिक साधना एवं योग विषयक
२५