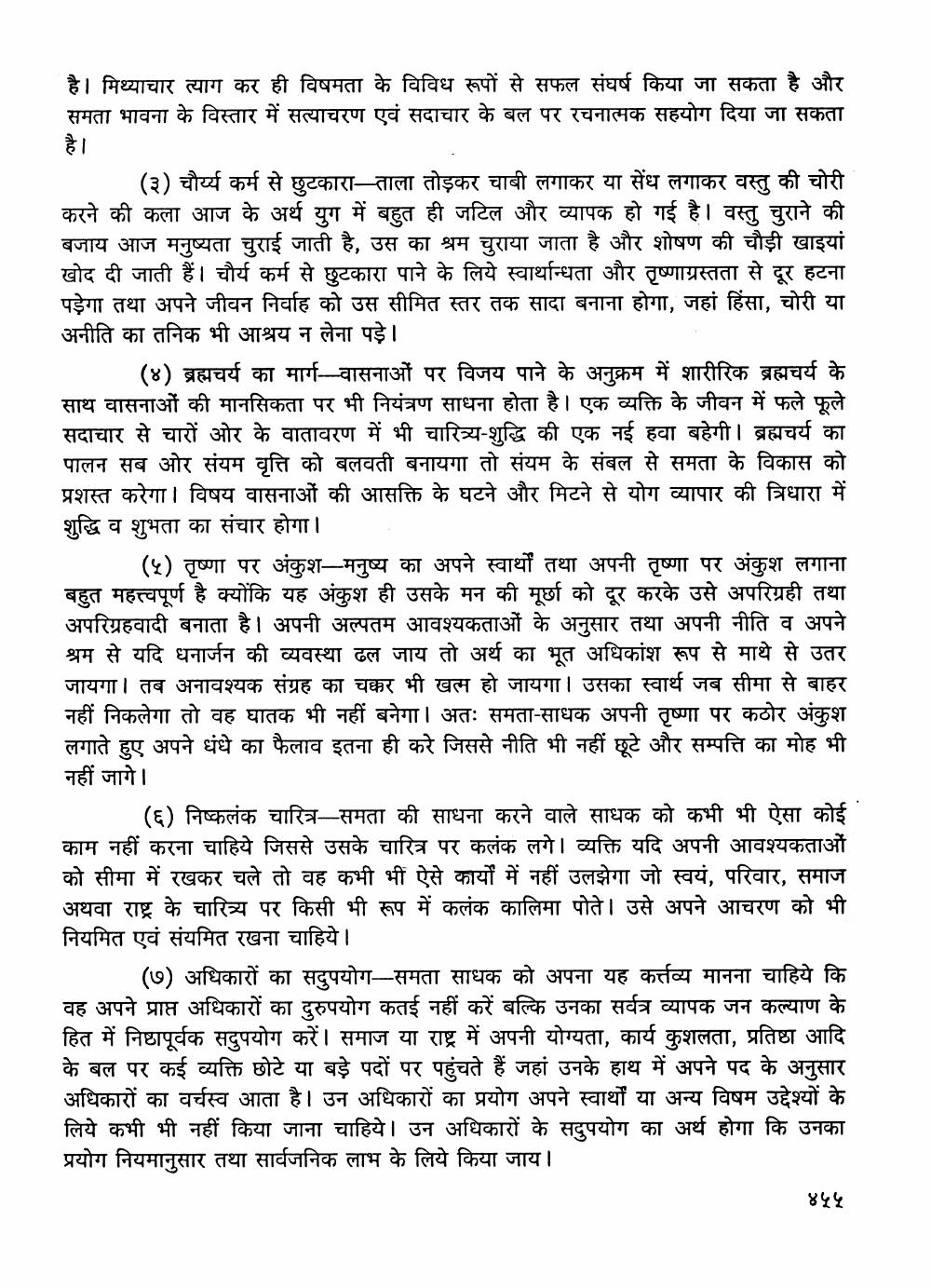________________
है। मिथ्याचार त्याग कर ही विषमता के विविध रूपों से सफल संघर्ष किया जा सकता है और समता भावना के विस्तार में सत्याचरण एवं सदाचार के बल पर रचनात्मक सहयोग दिया जा सकता
(३) चौर्य्य कर्म से छुटकारा ताला तोड़कर चाबी लगाकर या सेंध लगाकर वस्तु की चोरी करने की कला आज के अर्थ युग में बहुत ही जटिल और व्यापक हो गई है। वस्तु चुराने की बजाय आज मनुष्यता चुराई जाती है, उस का श्रम चुराया जाता है और शोषण की चौड़ी खाइयां खोद दी जाती हैं। चौर्य कर्म से छुटकारा पाने के लिये स्वार्थान्धता और तृष्णाग्रस्तता से दूर हटना पड़ेगा तथा अपने जीवन निर्वाह को उस सीमित स्तर तक सादा बनाना होगा, जहां हिंसा, चोरी या अनीति का तनिक भी आश्रय न लेना पड़े।
(४) ब्रह्मचर्य का मार्ग वासनाओं पर विजय पाने के अनुक्रम में शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ वासनाओं की मानसिकता पर भी नियंत्रण साधना होता है। एक व्यक्ति के जीवन में फले फूले सदाचार से चारों ओर के वातावरण में भी चारित्र्य-शुद्धि की एक नई हवा बहेगी। ब्रह्मचर्य का पालन सब ओर संयम वृत्ति को बलवती बनायगा तो संयम के संबल से समता के विकास को प्रशस्त करेगा। विषय वासनाओं की आसक्ति के घटने और मिटने से योग व्यापार की त्रिधारा में शुद्धि व शुभता का संचार होगा।
(५) तृष्णा पर अंकुश-मनुष्य का अपने स्वार्थों तथा अपनी तृष्णा पर अंकुश लगाना बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अंकुश ही उसके मन की मूर्छा को दूर करके उसे अपरिग्रही तथा अपरिग्रहवादी बनाता है। अपनी अल्पतम आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपनी नीति व अपने श्रम से यदि धनार्जन की व्यवस्था ढल जाय तो अर्थ का भूत अधिकांश रूप से माथे से उतर जायगा। तब अनावश्यक संग्रह का चक्कर भी खत्म हो जायगा। उसका स्वार्थ जब सीमा से बाहर नहीं निकलेगा तो वह घातक भी नहीं बनेगा। अतः समता-साधक अपनी तृष्णा पर कठोर अंकुश लगाते हुए अपने धंधे का फैलाव इतना ही करे जिससे नीति भी नहीं छूटे और सम्पत्ति का मोह भी नहीं जागे।
(६) निष्कलंक चारित्र—समता की साधना करने वाले साधक को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे उसके चारित्र पर कलंक लगे। व्यक्ति यदि अपनी आवश्यकताओं को सीमा में रखकर चले तो वह कभी भी ऐसे कार्यों में नहीं उलझेगा जो स्वयं, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र के चारित्र्य पर किसी भी रूप में कलंक कालिमा पोते। उसे अपने आचरण को भी नियमित एवं संयमित रखना चाहिये।
(७) अधिकारों का सदुपयोग–समता साधक को अपना यह कर्त्तव्य मानना चाहिये कि वह अपने प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग कतई नहीं करें बल्कि उनका सर्वत्र व्यापक जन कल्याण के हित में निष्ठापूर्वक सदुपयोग करें। समाज या राष्ट्र में अपनी योग्यता, कार्य कुशलता, प्रतिष्ठा आदि के बल पर कई व्यक्ति छोटे या बड़े पदों पर पहुंचते हैं जहां उनके हाथ में अपने पद के अनुसार अधिकारों का वर्चस्व आता है। उन अधिकारों का प्रयोग अपने स्वार्थों या अन्य विषम उद्देश्यों के लिये कभी भी नहीं किया जाना चाहिये। उन अधिकारों के सदुपयोग का अर्थ होगा कि उनका प्रयोग नियमानुसार तथा सार्वजनिक लाभ के लिये किया जाय।
४५५