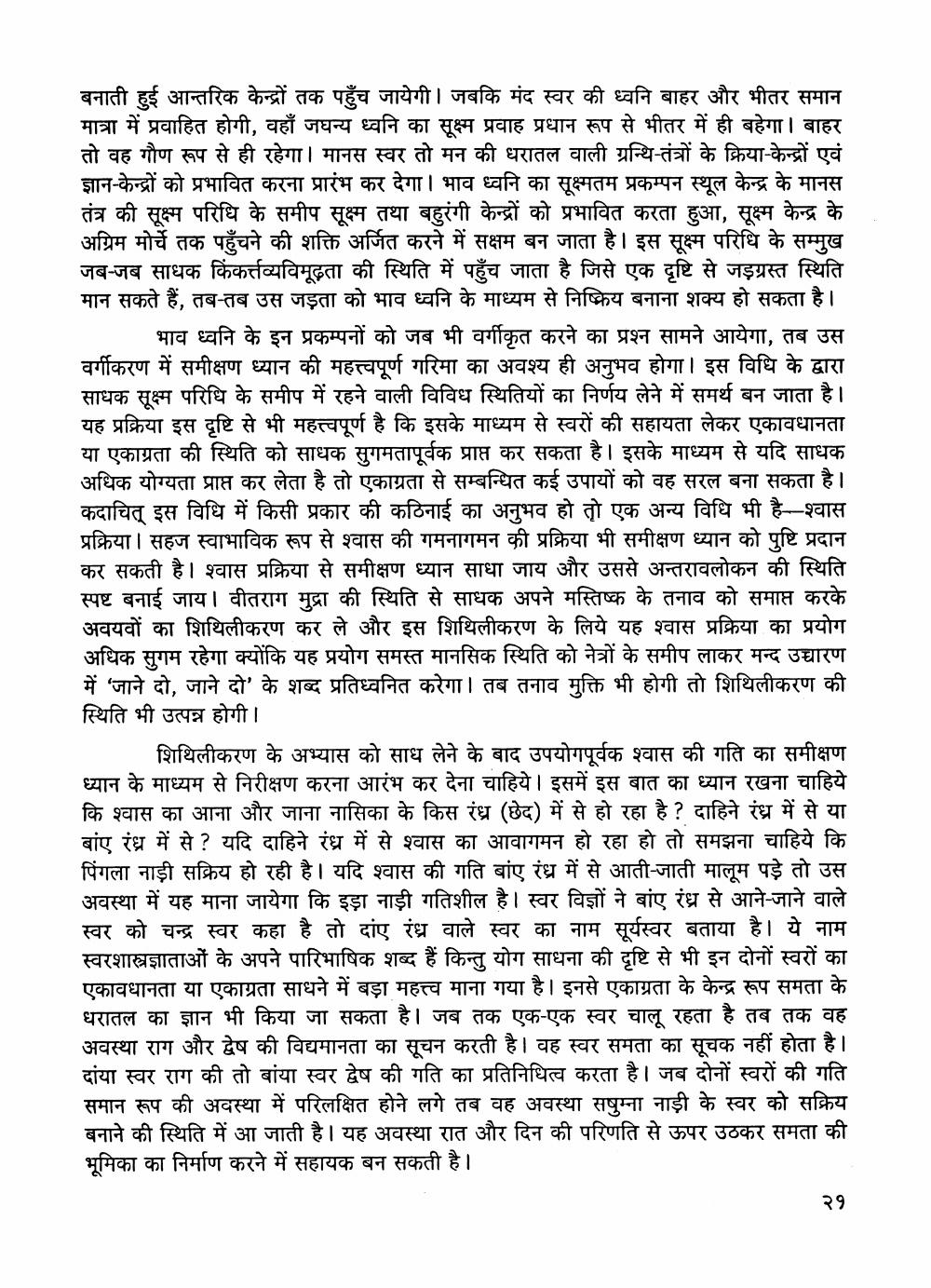________________
बनाती हुई आन्तरिक केन्द्रों तक पहुँच जायेगी। जबकि मंद स्वर की ध्वनि बाहर और भीतर समान मात्रा में प्रवाहित होगी, वहाँ जघन्य ध्वनि का सूक्ष्म प्रवाह प्रधान रूप से भीतर में ही बहेगा। बाहर तो वह गौण रूप से ही रहेगा। मानस स्वर तो मन की धरातल वाली ग्रन्थि-तंत्रों के क्रिया-केन्द्रों एवं ज्ञान-केन्द्रों को प्रभावित करना प्रारंभ कर देगा। भाव ध्वनि का सूक्ष्मतम प्रकम्पन स्थूल केन्द्र के मानस तंत्र की सूक्ष्म परिधि के समीप सूक्ष्म तथा बहुरंगी केन्द्रों को प्रभावित करता हुआ, सूक्ष्म केन्द्र के अग्रिम मोर्चे तक पहुँचने की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बन जाता है। इस सूक्ष्म परिधि के सम्मुख जब-जब साधक किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में पहुँच जाता है जिसे एक दृष्टि से जड़ग्रस्त स्थिति मान सकते हैं, तब-तब उस जड़ता को भाव ध्वनि के माध्यम से निष्क्रिय बनाना शक्य हो सकता है।
भाव ध्वनि के इन प्रकम्पनों को जब भी वर्गीकृत करने का प्रश्न सामने आयेगा, तब उस वर्गीकरण में समीक्षण ध्यान की महत्त्वपूर्ण गरिमा का अवश्य ही अनुभव होगा। इस विधि के द्वारा साधक सूक्ष्म परिधि के समीप में रहने वाली विविध स्थितियों का निर्णय लेने में समर्थ बन जाता है। यह प्रक्रिया इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से स्वरों की सहायता लेकर एकावधानता या एकाग्रता की स्थिति को साधक सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से यदि साधक अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो एकाग्रता से सम्बन्धित कई उपायों को वह सरल बना सकता है। कदाचित् इस विधि में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो तो एक अन्य विधि भी है-श्वास प्रक्रिया । सहज स्वाभाविक रूप से श्वास की गमनागमन की प्रक्रिया भी समीक्षण ध्यान को पुष्टि प्रदान कर सकती है। श्वास प्रक्रिया से समीक्षण ध्यान साधा जाय और उससे अन्तरावलोकन की स्थिति स्पष्ट बनाई जाय । वीतराग मुद्रा की स्थिति से साधक अपने मस्तिष्क के तनाव को समाप्त करके अवयवों का शिथिलीकरण कर ले और इस शिथिलीकरण के लिये यह श्वास प्रक्रिया का प्रयोग अधिक सुगम रहेगा क्योंकि यह प्रयोग समस्त मानसिक स्थिति को नेत्रों के समीप लाकर मन्द उच्चारण में 'जाने दो, जाने दो' के शब्द प्रतिध्वनित करेगा। तब तनाव मुक्ति भी होगी तो शिथिलीकरण की स्थिति भी उत्पन्न होगी।
शिथिलीकरण के अभ्यास को साध लेने के बाद उपयोगपूर्वक श्वास की गति का समीक्षण ध्यान के माध्यम से निरीक्षण करना आरंभ कर देना चाहिये । इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये
वास का आना और जाना नासिका के किस रंध्र (छेद) में से हो रहा है? दाहिने रंध्र में से या बांए रंध्र में से? यदि दाहिने रंध्र में से श्वास का आवागमन हो रहा हो तो समझना चाहिये कि पिंगला नाडी सक्रिय हो रही है। यदि श्वास की गति बांए रंध्र में से आती-जाती मालूम पड़े तो उस अवस्था में यह माना जायेगा कि इड़ा नाड़ी गतिशील है। स्वर विज्ञों ने बांए रंध्र से आने-जाने वाले स्वर को चन्द्र स्वर कहा है तो दांए रंध्र वाले स्वर का नाम सूर्यस्वर बताया है। ये नाम स्वरशास्त्रज्ञाताओं के अपने पारिभाषिक शब्द हैं किन्तु योग साधना की दृष्टि से भी इन दोनों स्वरों का एकावधानता या एकाग्रता साधने में बड़ा महत्त्व माना गया है। इनसे एकाग्रता के केन्द्र रूप समता के धरातल का ज्ञान भी किया जा सकता है। जब तक एक-एक स्वर चालू रहता है तब तक वह अवस्था राग और द्वेष की विद्यमानता का सूचन करती है। वह स्वर समता का सूचक नहीं होता है। दांया स्वर राग की तो बांया स्वर द्वेष की गति का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों स्वरों की गति समान रूप की अवस्था में परिलक्षित होने लगे तब वह अवस्था सषुम्ना नाड़ी के स्वर को सक्रिय बनाने की स्थिति में आ जाती है। यह अवस्था रात और दिन की परिणति से ऊपर उठकर समता की भूमिका का निर्माण करने में सहायक बन सकती है।