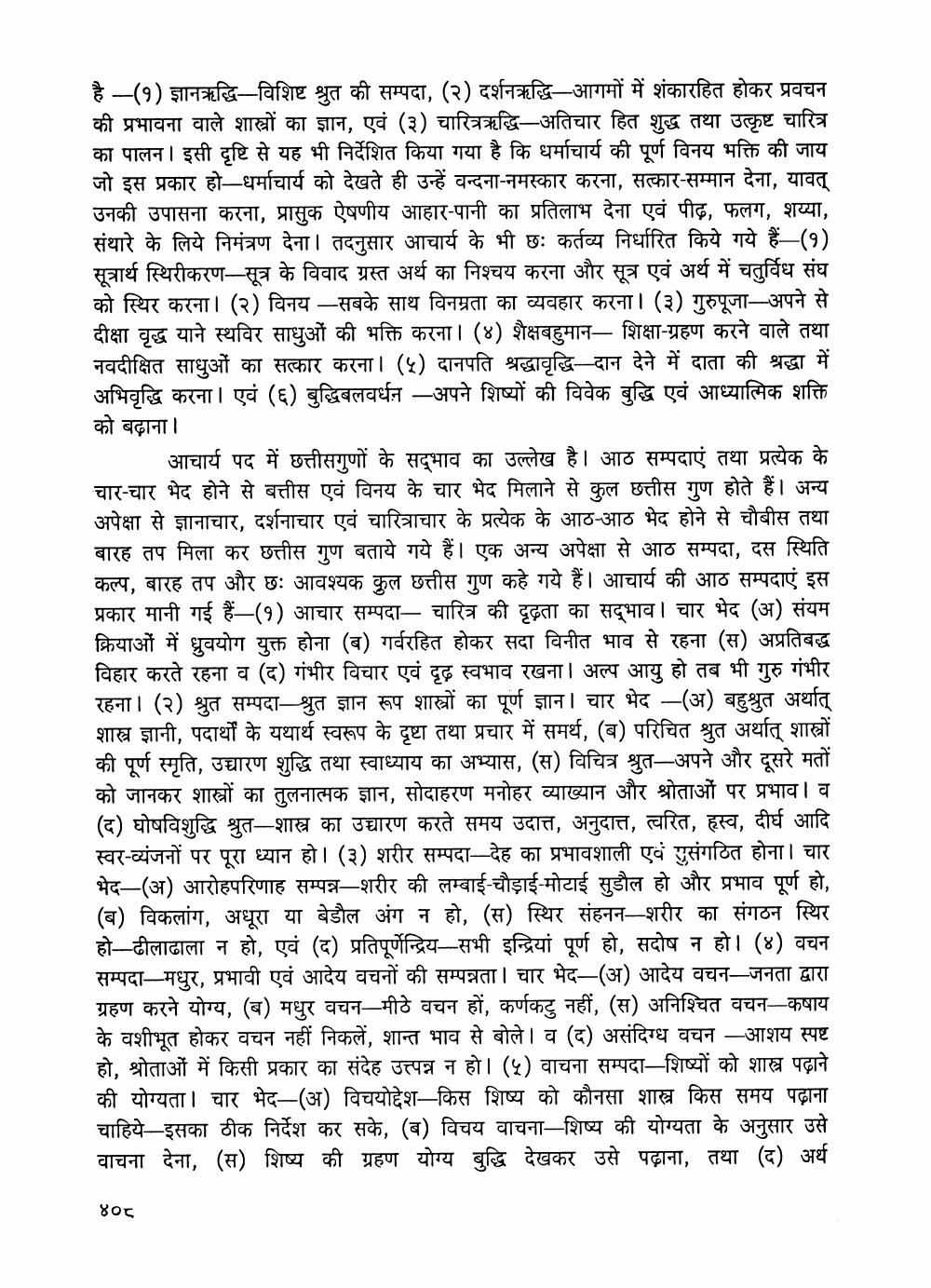________________
है – (१) ज्ञानऋद्धि-विशिष्ट श्रुत की सम्पदा, (२) दर्शनऋद्धि-आगमों में शंकारहित होकर प्रवचन की प्रभावना वाले शास्त्रों का ज्ञान, एवं (३) चारित्रऋद्धि-अतिचार हित शुद्ध तथा उत्कृष्ट चारित्र का पालन। इसी दृष्टि से यह भी निर्देशित किया गया है कि धर्माचार्य की पूर्ण विनय भक्ति की जाय जो इस प्रकार हो-धर्माचार्य को देखते ही उन्हें वन्दना-नमस्कार करना, सत्कार-सम्मान देना, यावत् उनकी उपासना करना, प्रासुक ऐषणीय आहार-पानी का प्रतिलाभ देना एवं पीढ़, फलग, शय्या, संथारे के लिये निमंत्रण देना। तदनुसार आचार्य के भी छः कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं—(१) सूत्रार्थ स्थिरीकरण-सूत्र के विवाद ग्रस्त अर्थ का निश्चय करना और सूत्र एवं अर्थ में चतुर्विध संघ को स्थिर करना। (२) विनय —सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करना। (३) गुरुपूजा-अपने से दीक्षा वृद्ध याने स्थविर साधुओं की भक्ति करना । (४) शैक्षबहुमान— शिक्षा-ग्रहण करने वाले तथा नवदीक्षित साधुओं का सत्कार करना। (५) दानपति श्रद्धावृद्धि दान देने में दाता की श्रद्धा में अभिवृद्धि करना । एवं (६) बुद्धिबलवर्धन -अपने शिष्यों की विवेक बुद्धि एवं आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना।
__ आचार्य पद में छत्तीसगुणों के सद्भाव का उल्लेख है। आठ सम्पदाएं तथा प्रत्येक के चार-चार भेद होने से बत्तीस एवं विनय के चार भेद मिलाने से कुल छत्तीस गुण होते हैं। अन्य अपेक्षा से ज्ञानाचार, दर्शनाचार एवं चारित्राचार के प्रत्येक के आठ-आठ भेद होने से चौबीस तथा बारह तप मिला कर छत्तीस गुण बताये गये हैं। एक अन्य अपेक्षा से आठ सम्पदा, दस स्थिति कल्प, बारह तप और छः आवश्यक कुल छत्तीस गुण कहे गये हैं। आचार्य की आठ सम्पदाएं इस प्रकार मानी गई हैं—(१) आचार सम्पदा- चारित्र की दृढ़ता का सद्भाव । चार भेद (अ) संयम क्रियाओं में ध्रुवयोग युक्त होना (ब) गर्वरहित होकर सदा विनीत भाव से रहना (स) अप्रतिबद्ध विहार करते रहना व (द) गंभीर विचार एवं दृढ़ स्वभाव रखना। अल्प आयु हो तब भी गुरु गंभीर रहना । (२) श्रुत सम्पदा श्रुत ज्ञान रूप शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान । चार भेद -(अ) बहुश्रुत अर्थात् शास्त्र ज्ञानी, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के दृष्टा तथा प्रचार में समर्थ, (ब) परिचित श्रुत अर्थात् शास्त्रों की पूर्ण स्मृति, उच्चारण शुद्धि तथा स्वाध्याय का अभ्यास, (स) विचित्र श्रुत-अपने और दूसरे मतों को जानकर शास्त्रों का तुलनात्मक ज्ञान, सोदाहरण मनोहर व्याख्यान और श्रोताओं पर प्रभाव । व (द) घोषविशुद्धि श्रुत-शास्त्र का उच्चारण करते समय उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, हस्व, दीर्घ आदि स्वर-व्यंजनों पर पूरा ध्यान हो। (३) शरीर सम्पदा-देह का प्रभावशाली एवं सुसंगठित होना। चार भेद—(अ) आरोहपरिणाह सम्पन्न—शरीर की लम्बाई-चौड़ाई-मोटाई सुडौल हो और प्रभाव पूर्ण हो, (ब) विकलांग, अधूरा या बेडौल अंग न हो, (स) स्थिर संहनन—शरीर का संगठन स्थिर हो—ढीलाढाला न हो, एवं (द) प्रतिपूर्णेन्द्रिय—सभी इन्द्रियां पूर्ण हो, सदोष न हो। (४) वचन सम्पदा–मधुर, प्रभावी एवं आदेय वचनों की सम्पन्नता। चार भेद-(अ) आदेय वचन–जनता द्वारा ग्रहण करने योग्य, (ब) मधुर वचन–मीठे वचन हों, कर्णकटु नहीं, (स) अनिश्चित वचन–कषाय के वशीभूत होकर वचन नहीं निकलें, शान्त भाव से बोले । व (द) असंदिग्ध वचन -आशय स्पष्ट हो, श्रोताओं में किसी प्रकार का संदेह उत्त्पन्न न हो। (५) वाचना सम्पदा-शिष्यों को शास्त्र पढ़ाने की योग्यता। चार भेद-(अ) विचयोद्देश—किस शिष्य को कौनसा शास्त्र किस समय पढ़ाना चाहिये इसका ठीक निर्देश कर सके, (ब) विचय वाचना-शिष्य की योग्यता के अनुसार उसे वाचना देना, (स) शिष्य की ग्रहण योग्य बुद्धि देखकर उसे पढ़ाना, तथा (द) अर्थ
४०८