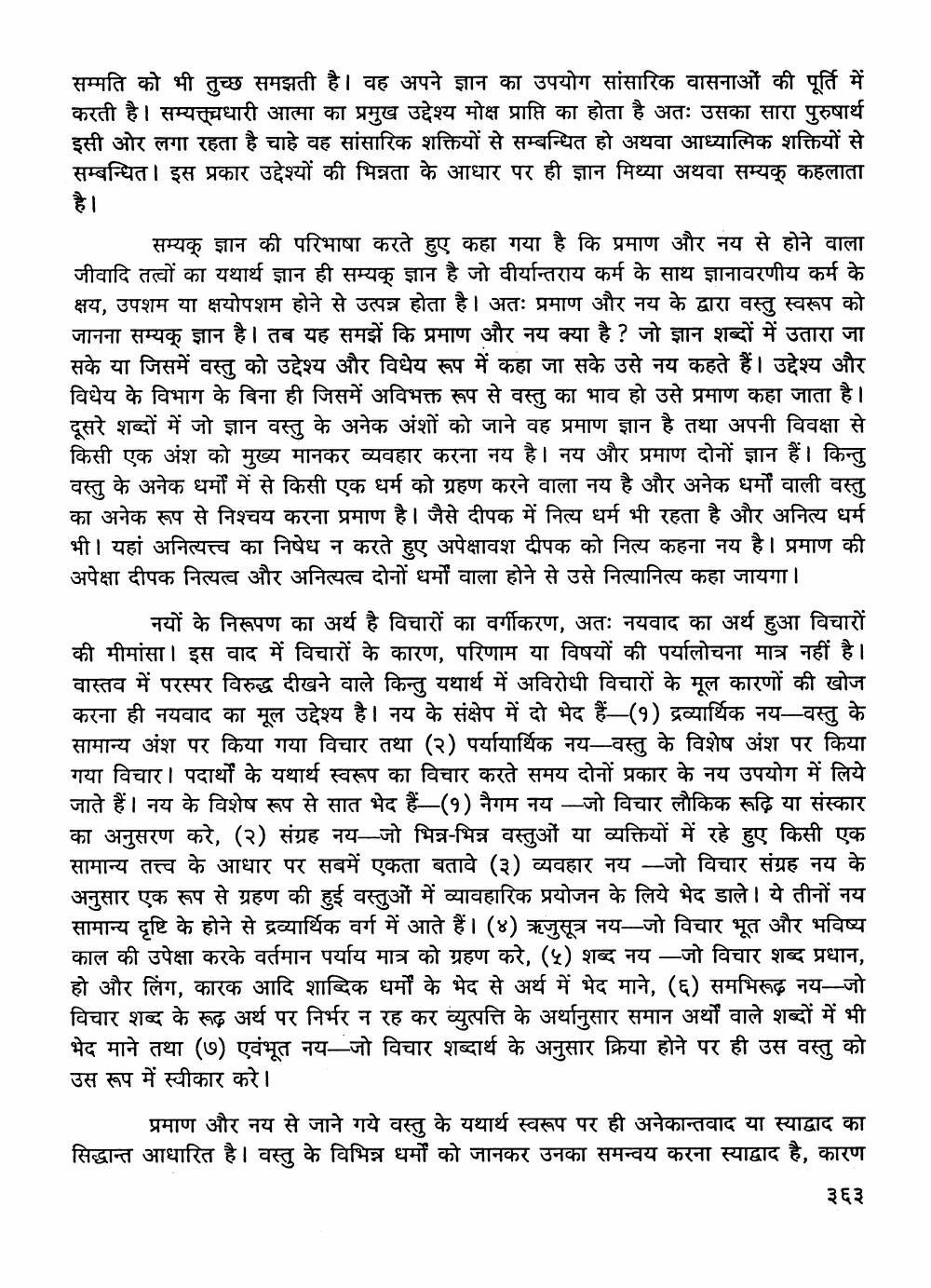________________
सम्मति को भी तुच्छ समझती है। वह अपने ज्ञान का उपयोग सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में करती है। सम्यक्त्वधारी आत्मा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का होता है अतः उसका सारा पुरुषार्थ इसी ओर लगा रहता है चाहे वह सांसारिक शक्तियों से सम्बन्धित हो अथवा आध्यात्मिक शक्तियों से सम्बन्धित। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के आधार पर ही ज्ञान मिथ्या अथवा सम्यक् कहलाता है।
सम्यक् ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि प्रमाण और नय से होने वाला जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है जो वीर्यान्तराय कर्म के साथ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने से उत्पन्न होता है। अतः प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को जानना सम्यक् ज्ञान है। तब यह समझें कि प्रमाण और नय क्या है? जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके या जिसमें वस्त को उद्देश्य और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय के विभाग के बिना ही जिसमें अविभक्त रूप से वस्त का भाव हो उसे प्रमाण का दूसरे शब्दों में जो ज्ञान वस्तु के अनेक अंशों को जाने वह प्रमाण ज्ञान है तथा अपनी विवक्षा से किसी एक अंश को मुख्य मानकर व्यवहार करना नय है। नय और प्रमाण दोनों ज्ञान हैं। किन्तु वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है और अनेक धर्मों वाली वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना प्रमाण है। जैसे दीपक में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्य धर्म भी। यहां अनित्यत्त्व का निषेध न करते हुए अपेक्षावश दीपक को नित्य कहना नय है। प्रमाण की अपेक्षा दीपक नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों धर्मों वाला होने से उसे नित्यानित्य कहा जायगा।
नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण, अतः नयवाद का अर्थ हुआ विचारों की मीमांसा। इस वाद में विचारों के कारण, परिणाम या विषयों की पर्यालोचना मात्र नहीं है। वास्तव में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले किन्तु यथार्थ में अविरोधी विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही नयवाद का मूल उद्देश्य है। नय के संक्षेप में दो भेद हैं—(१) द्रव्यार्थिक नय-वस्तु के सामान्य अंश पर किया गया विचार तथा (२) पर्यायार्थिक नय-वस्तु के विशेष अंश पर किया गया विचार। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का विचार करते समय दोनों प्रकार के नय उपयोग में लिये जाते हैं। नय के विशेष रूप से सात भेद हैं—(१) नैगम नय -जो विचार लौकिक रूढ़ि या संस्कार का अनुसरण करे, (२) संग्रह नय—जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में रहे हुए किसी एक सामान्य तत्त्व के आधार पर सबमें एकता बतावे (३) व्यवहार नय -जो विचार संग्रह नय के अनुसार एक रूप से ग्रहण की हुई वस्तुओं में व्यावहारिक प्रयोजन के लिये भेद डाले। ये तीनों नय सामान्य दृष्टि के होने से द्रव्यार्थिक वर्ग में आते हैं। (४) ऋजुसूत्र नय—जो विचार भूत और भविष्य काल की उपेक्षा करके वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे, (५) शब्द नय -जो विचार शब्द प्रधान, हो और लिंग, कारक आदि शाब्दिक धर्मों के भेद से अर्थ में भेद माने, (६) समभिरूढ़ नय-जो विचार शब्द के रूढ़ अर्थ पर निर्भर न रह कर व्युत्पत्ति के अर्थानुसार समान अर्थों वाले शब्दों में भी भेद माने तथा (७) एवंभूत नय—जो विचार शब्दार्थ के अनुसार क्रिया होने पर ही उस वस्तु को उस रूप में स्वीकार करे।
प्रमाण और नय से जाने गये वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर ही अनेकान्तवाद या स्याद्वाद का सिद्धान्त आधारित है। वस्तु के विभिन्न धर्मों को जानकर उनका समन्वय करना स्याद्वाद है, कारण
३६३