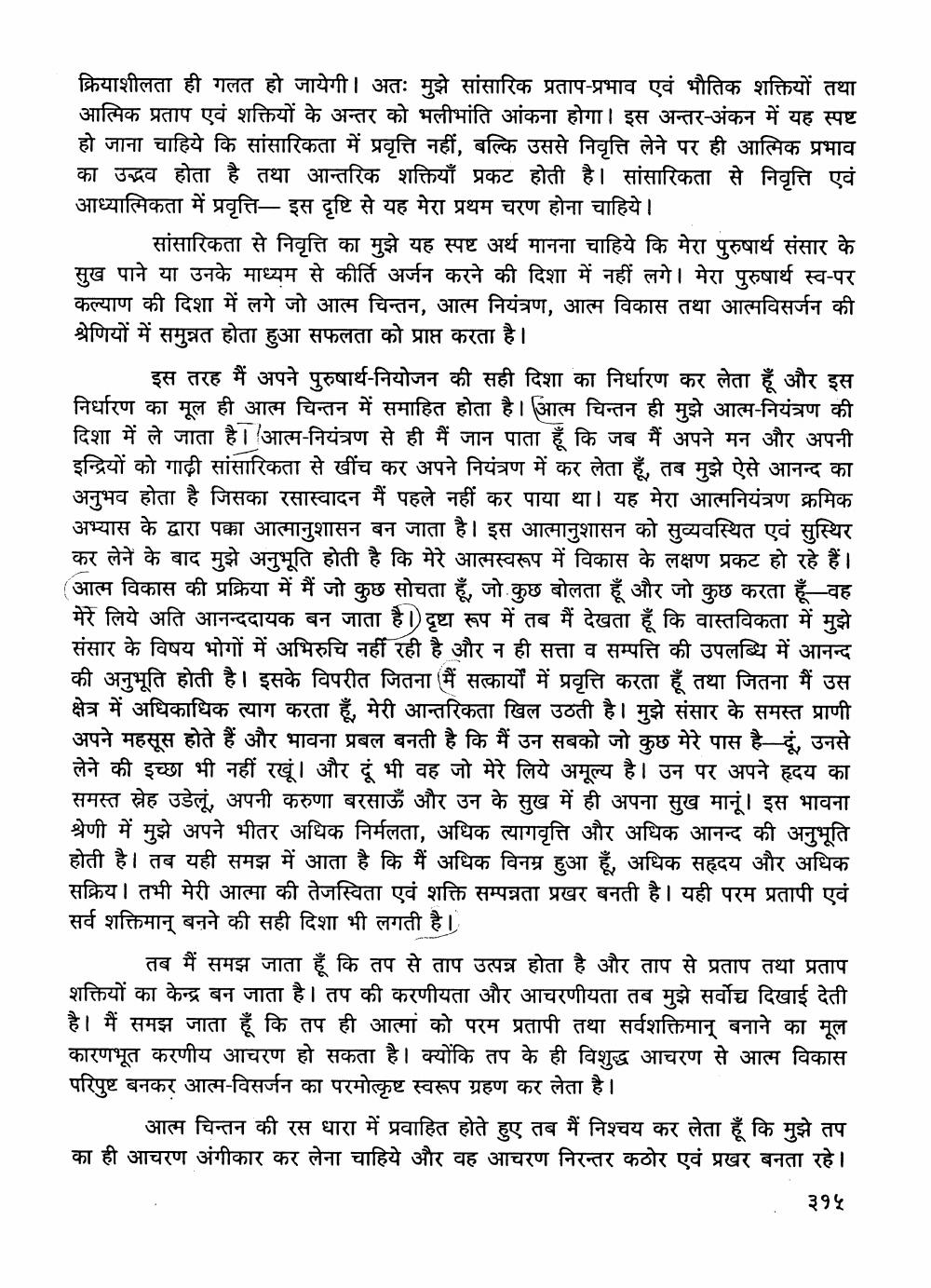________________
क्रियाशीलता ही गलत हो जायेगी। अतः मुझे सांसारिक प्रताप-प्रभाव एवं भौतिक शक्तियों तथा आत्मिक प्रताप एवं शक्तियों के अन्तर को भलीभांति आंकना होगा। इस अन्तर-अंकन में यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि सांसारिकता में प्रवृत्ति नहीं, बल्कि उससे निवृत्ति लेने पर ही आत्मिक प्रभाव का उद्भव होता है तथा आन्तरिक शक्तियाँ प्रकट होती है। सांसारिकता से निवृत्ति एवं आध्यात्मिकता में प्रवृत्ति- इस दृष्टि से यह मेरा प्रथम चरण होना चाहिये।
सांसारिकता से निवृत्ति का मुझे यह स्पष्ट अर्थ मानना चाहिये कि मेरा पुरुषार्थ संसार के सुख पाने या उनके माध्यम से कीर्ति अर्जन करने की दिशा में नहीं लगे। मेरा पुरुषार्थ स्व-पर कल्याण की दिशा में लगे जो आत्म चिन्तन, आत्म नियंत्रण, आत्म विकास तथा आत्मविसर्जन की श्रेणियों में समुन्नत होता हुआ सफलता को प्राप्त करता है।
इस तरह मैं अपने पुरुषार्थ-नियोजन की सही दिशा का निर्धारण कर लेता हूँ और इस निर्धारण का मूल ही आत्म चिन्तन में समाहित होता है। आत्म चिन्तन ही मुझे आत्म-नियंत्रण की दिशा में ले जाता है। आत्म-नियंत्रण से ही मैं जान पाता हूँ कि जब मैं अपने मन और अपनी इन्द्रियों को गाढ़ी सांसारिकता से खींच कर अपने नियंत्रण में कर लेता हूँ, तब मुझे ऐसे आनन्द का अनुभव होता है जिसका रसास्वादन मैं पहले नहीं कर पाया था। यह मेरा आत्मनियंत्रण क्रमिक अभ्यास के द्वारा पक्का आत्मानुशासन बन जाता है। इस आत्मानुशासन को सुव्यवस्थित एवं सुस्थिर र लेने के बाद मुझे अनुभूति होती है कि मेरे आत्मस्वरूप में विकास के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आत्म विकास की प्रक्रिया में मैं जो कुछ सोचता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ और जो कुछ करता हूँ वह मेरे लिये अति आनन्ददायक बन जाता है।) दृष्टा रूप में तब मैं देखता हूँ कि वास्तविकता में मुझे संसार के विषय भोगों में अभिरुचि नहीं रही है और न ही सत्ता व सम्पत्ति की उपलब्धि में आनन्द की अनुभूति होती है। इसके विपरीत जितना (मैं सत्कार्यों में प्रवृत्ति करता हूँ तथा जितना मैं उस क्षेत्र में अधिकाधिक त्याग करता हूँ, मेरी आन्तरिकता खिल उठती है। मुझे संसार के समस्त प्राणी अपने महसूस होते हैं और भावना प्रबल बनती है कि मैं उन सबको जो कुछ मेरे पास है दूं, उनसे लेने की इच्छा भी नहीं रखू। और दूं भी वह जो मेरे लिये अमूल्य है। उन पर अपने हृदय का समस्त स्नेह उडेलूं, अपनी करुणा बरसाऊँ और उन के सुख में ही अपना सुख मानूं। इस भावना श्रेणी में मुझे अपने भीतर अधिक निर्मलता, अधिक त्यागवृत्ति और अधिक आनन्द की अनुभूति होती है। तब यही समझ में आता है कि मैं अधिक विनम्र हुआ हूँ, अधिक सहृदय और अधिक सक्रिय । तभी मेरी आत्मा की तेजस्विता एवं शक्ति सम्पन्नता प्रखर बनती है। यही परम प्रतापी एवं सर्व शक्तिमान् बनने की सही दिशा भी लगती है।
तब मैं समझ जाता हूँ कि तप से ताप उत्पन्न होता है और ताप से प्रताप तथा प्रताप शक्तियों का केन्द्र बन जाता है। तप की करणीयता और आचरणीयता तब मुझे सर्वोच्च दिखाई देती है। मैं समझ जाता हूँ कि तप ही आत्मा को परम प्रतापी तथा सर्वशक्तिमान् बनाने का मूल कारणभूत करणीय आचरण हो सकता है। क्योंकि तप के ही विशुद्ध आचरण से आत्म विकास परिपुष्ट बनकर आत्म-विसर्जन का परमोत्कृष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेता है।
आत्म चिन्तन की रस धारा में प्रवाहित होते हुए तब मैं निश्चय कर लेता हूँ कि मुझे तप का ही आचरण अंगीकार कर लेना चाहिये और वह आचरण निरन्तर कठोर एवं प्रखर बनता रहे।
३१५