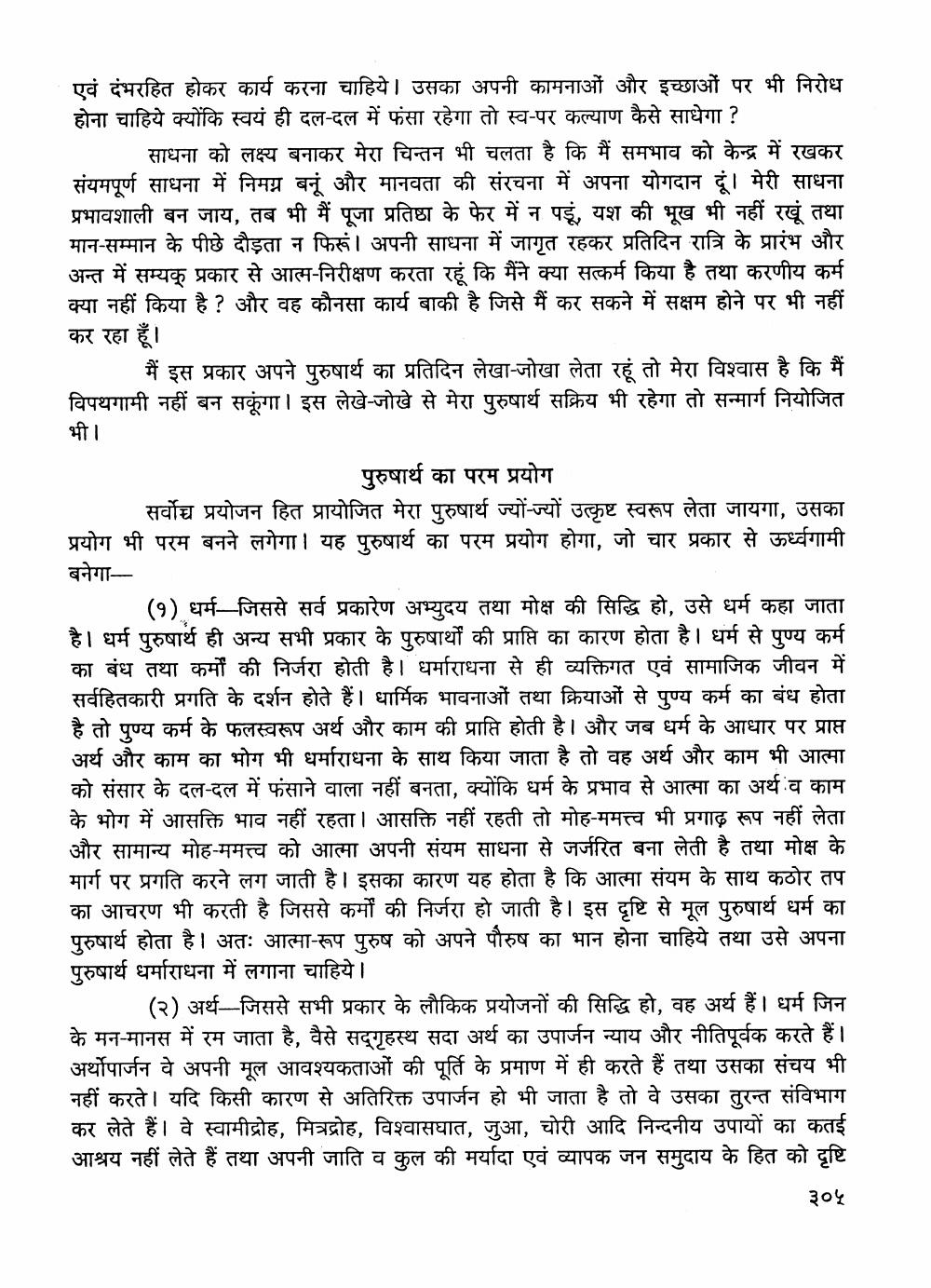________________
एवं दंभरहित होकर कार्य करना चाहिये। उसका अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर भी निरोध होना चाहिये क्योंकि स्वयं ही दल-दल में फंसा रहेगा तो स्व-पर कल्याण कैसे साधेगा?
साधना को लक्ष्य बनाकर मेरा चिन्तन भी चलता है कि मैं समभाव को केन्द्र में रखकर संयमपूर्ण साधना में निमग्न बनूं और मानवता की संरचना में अपना योगदान दूं। मेरी साधना प्रभावशाली बन जाय, तब भी मैं पूजा प्रतिष्ठा के फेर में न पडूं, यश की भूख भी नहीं रखू तथा मान-सम्मान के पीछे दौड़ता न फिरूं। अपनी साधना में जागृत रहकर प्रतिदिन रात्रि के प्रारंभ और अन्त में सम्यक् प्रकार से आत्म-निरीक्षण करता रहूं कि मैंने क्या सत्कर्म किया है तथा करणीय कर्म क्या नहीं किया है ? और वह कौनसा कार्य बाकी है जिसे मैं कर सकने में सक्षम होने पर भी नहीं कर रहा हूँ।
मैं इस प्रकार अपने पुरुषार्थ का प्रतिदिन लेखा-जोखा लेता रहूं तो मेरा विश्वास है कि मैं विपथगामी नहीं बन सकूँगा। इस लेखे-जोखे से मेरा पुरुषार्थ सक्रिय भी रहेगा तो सन्मार्ग नियोजित
भी।
पुरुषार्थ का परम प्रयोग सर्वोच्च प्रयोजन हित प्रायोजित मेरा पुरुषार्थ ज्यों-ज्यों उत्कृष्ट स्वरूप लेता जायगा, उसका प्रयोग भी परम बनने लगेगा। यह पुरुषार्थ का परम प्रयोग होगा, जो चार प्रकार से ऊर्ध्वगामी बनेगा
(१) धर्म—जिससे सर्व प्रकारेण अभ्युदय तथा मोक्ष की सिद्धि हो, उसे धर्म कहा जाता है। धर्म पुरुषार्थ ही अन्य सभी प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण होता है। धर्म से पुण्य कर्म का बंध तथा कर्मों की निर्जरा होती है। धर्माराधना से ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सर्वहितकारी प्रगति के दर्शन होते हैं। धार्मिक भावनाओं तथा क्रियाओं से पुण्य कर्म का बंध होता है तो पुण्य कर्म के फलस्वरूप अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। और जब धर्म के आधार पर प्राप्त अर्थ और काम का भोग भी धर्माराधना के साथ किया जाता है तो वह अर्थ और काम भी आत्मा को संसार के दल-दल में फंसाने वाला नहीं बनता, क्योंकि धर्म के प्रभाव से आत्मा का अर्थ व काम के भोग में आसक्ति भाव नहीं रहता। आसक्ति नहीं रहती तो मोह-ममत्त्व भी प्रगाढ़ रूप नहीं लेता और सामान्य मोह-ममत्त्व को आत्मा अपनी संयम साधना से जर्जरित बना लेती है तथा मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करने लग जाती है। इसका कारण यह होता है कि आत्मा संयम के साथ कठोर तप का आचरण भी करती है जिससे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस दृष्टि से मूल पुरुषार्थ धर्म का पुरुषार्थ होता है। अतः आत्मा-रूप पुरुष को अपने पौरुष का भान होना चाहिये तथा उसे अपना पुरुषार्थ धर्माराधना में लगाना चाहिये।
(२) अर्थ-जिससे सभी प्रकार के लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि हो, वह अर्थ हैं। धर्म जिन के मन-मानस में रम जाता है, वैसे सद्गृहस्थ सदा अर्थ का उपार्जन न्याय और नीतिपूर्वक करते हैं। अर्थोपार्जन वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रमाण में ही करते हैं तथा उसका संचय भी नहीं करते। यदि किसी कारण से अतिरिक्त उपार्जन हो भी जाता है तो वे उसका तुरन्त संविभाग कर लेते हैं। वे स्वामीद्रोह, मित्रद्रोह, विश्वासघात, जुआ, चोरी आदि निन्दनीय उपायों का कतई आश्रय नहीं लेते हैं तथा अपनी जाति व कुल की मर्यादा एवं व्यापक जन समुदाय के हित को दृष्टि
३०५