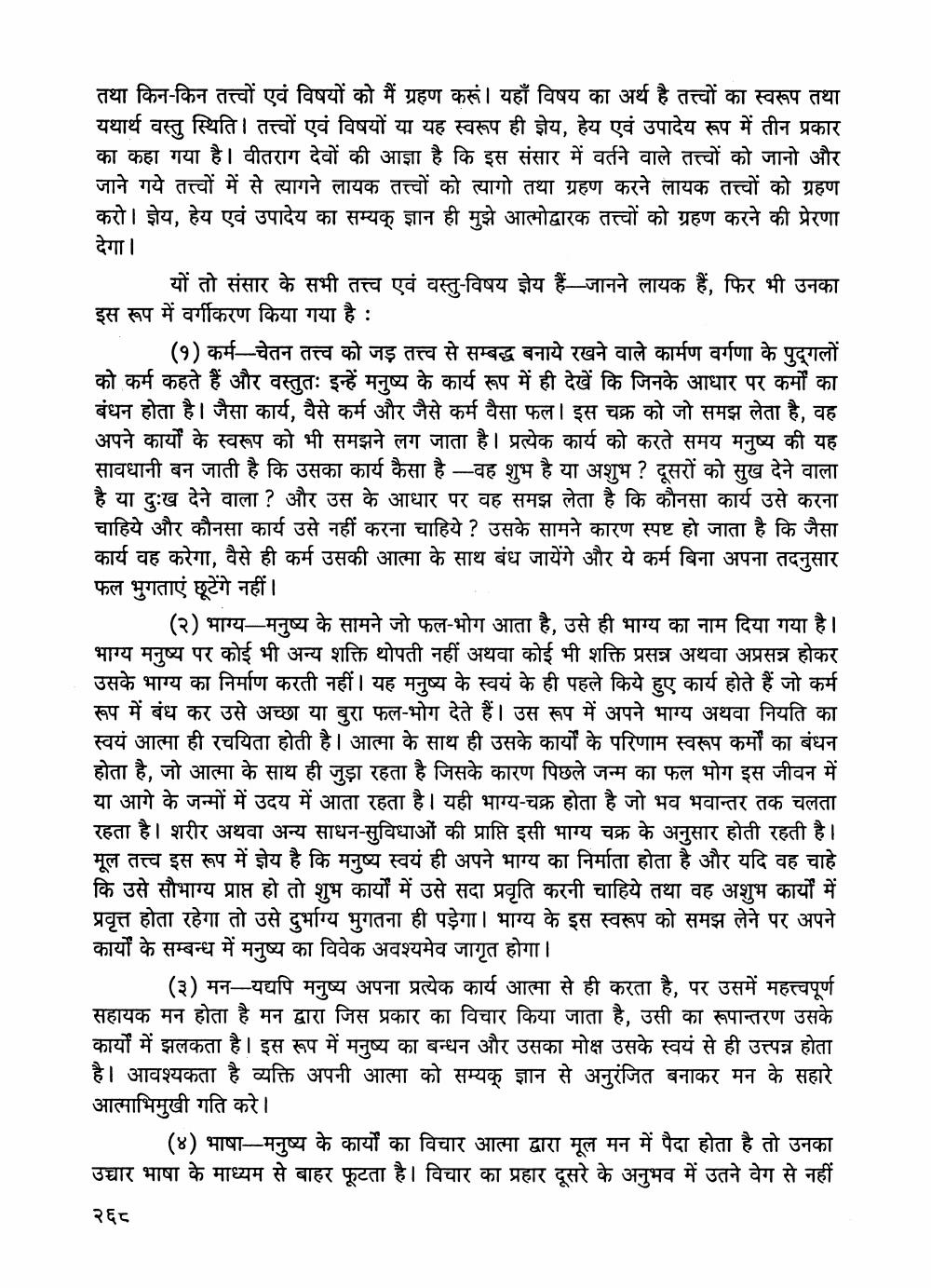________________
तथा किन-किन तत्त्वों एवं विषयों को मैं ग्रहण करूं । यहाँ विषय का अर्थ है तत्त्वों का स्वरूप तथा यथार्थ वस्तु स्थिति। तत्त्वों एवं विषयों या यह स्वरूप ही ज्ञेय, हेय एवं उपादेय रूप में तीन प्रकार का कहा गया है। वीतराग देवों की आज्ञा है कि इस संसार में वर्तने वाले तत्त्वों को जानो और जाने गये तत्त्वों में से त्यागने लायक तत्त्वों को त्यागो तथा ग्रहण करने लायक तत्त्वों को ग्रहण करो। ज्ञेय, हेय एवं उपादेय का सम्यक् ज्ञान ही मुझे आत्मोद्वारक तत्त्वों को ग्रहण करने की प्रेरणा देगा
यों तो संसार के सभी तत्त्व एवं वस्तु-विषय ज्ञेय हैं— जानने लायक हैं, फिर भी उनका इस रूप में वर्गीकरण किया गया है :
(१) कर्म - चेतन तत्त्व को जड़ तत्त्व से सम्बद्ध बनाये रखने वाले कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कर्म कहते हैं और वस्तुतः इन्हें मनुष्य के कार्य रूप में ही देखें कि जिनके आधार पर कर्मों का बंधन होता है। जैसा कार्य, वैसे कर्म और जैसे कर्म वैसा फल । इस चक्र को जो समझ लेता है, वह अपने कार्यों के स्वरूप को भी समझने लग जाता है। प्रत्येक कार्य को करते समय मनुष्य की यह सावधानी बन जाती है कि उसका कार्य कैसा है - वह शुभ है या अशुभ ? दूसरों को सुख देने वाला है या दुःख देने वाला ? और उस के आधार पर वह समझ लेता है कि कौनसा कार्य उसे करना चाहिये और कौनसा कार्य उसे नहीं करना चाहिये ? उसके सामने कारण स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कार्य वह करेगा, वैसे ही कर्म उसकी आत्मा के साथ बंध जायेंगे और ये कर्म बिना अपना तदनुसार फल भुगताएं छूटेंगे नहीं ।
(२) भाग्य - मनुष्य के सामने जो फल भोग आता है, उसे ही भाग्य का नाम दिया गया है। भाग्य मनुष्य पर कोई भी अन्य शक्ति थोपती नहीं अथवा कोई भी शक्ति प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होकर उसके भाग्य का निर्माण करती नहीं । यह मनुष्य के स्वयं के ही पहले किये हुए कार्य होते हैं जो कर्म रूप में बंध कर उसे अच्छा या बुरा फल भोग देते हैं । उस रूप में अपने भाग्य अथवा नियति का स्वयं आत्मा ही रचयिता होती है। आत्मा के साथ ही उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप कर्मों का बंधन होता है, जो आत्मा के साथ ही जुड़ा रहता है जिसके कारण पिछले जन्म का फल भोग इस जीवन में या आगे के जन्मों में उदय में आता रहता है। यही भाग्य-चक्र होता है जो भव भवान्तर तक चलता रहता है। शरीर अथवा अन्य साधन-सुविधाओं की प्राप्ति इसी भाग्य चक्र के अनुसार होती रहती है। मूल तत्त्व इस रूप में ज्ञेय है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है और यदि वह चाहे कि उसे सौभाग्य प्राप्त हो तो शुभ कार्यों में उसे सदा प्रवृति करनी चाहिये तथा वह अशुभ कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा तो उसे दुर्भाग्य भुगतना ही पड़ेगा । भाग्य के इस स्वरूप को समझ लेने पर अपने कार्यों के सम्बन्ध में मनुष्य का विवेक अवश्यमेव जागृत होगा ।
(३) मन - यद्यपि मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य आत्मा से ही करता है, पर उसमें महत्त्वपूर्ण सहायक मन होता है मन द्वारा जिस प्रकार का विचार किया जाता है, उसी का रूपान्तरण उसके कार्यों में झलकता है। इस रूप में मनुष्य का बन्धन और उसका मोक्ष उसके स्वयं से ही उत्त्पन्न होता है । आवश्यकता है व्यक्ति अपनी आत्मा को सम्यक् ज्ञान से अनुरंजित बनाकर मन सहारे आत्माभिमुखी गति करे ।
(४) भाषा - मनुष्य के कार्यों का विचार आत्मा द्वारा मूल मन में पैदा होता है तो उनका उच्चार भाषा के माध्यम से बाहर फूटता है। विचार का प्रहार दूसरे के अनुभव में उतने वेग से नहीं
२६८