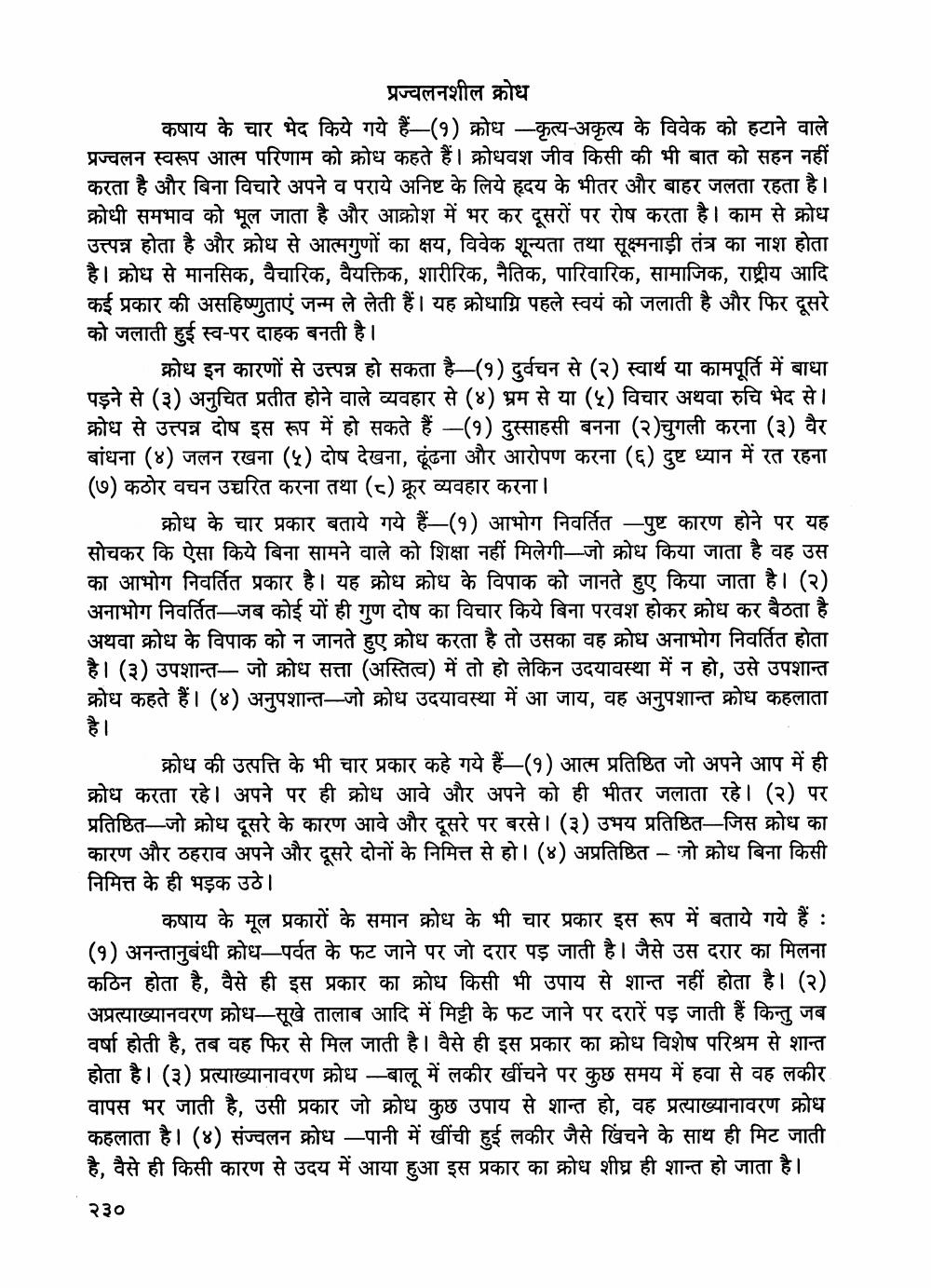________________
प्रज्वलनशील क्रोध
कषाय के चार भेद किये गये हैं— (१) क्रोध – कृत्य अकृत्य के विवेक को हटाने वाले प्रज्वलन स्वरूप आत्म परिणाम को क्रोध कहते हैं । क्रोधवश जीव किसी की भी बात को सहन नहीं करता है और बिना विचारे अपने व पराये अनिष्ट के लिये हृदय के भीतर और बाहर जलता रहता है । क्रोधी समभाव को भूल जाता है और आक्रोश में भर कर दूसरों पर रोष करता है । काम से क्रोध उत्त्पन्न होता है और क्रोध से आत्मगुणों का क्षय, विवेक शून्यता तथा सूक्ष्मनाड़ी तंत्र का नाश होता है। क्रोध से मानसिक, वैचारिक, वैयक्तिक, शारीरिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि कई प्रकार की असहिष्णुताएं जन्म ले लेती हैं। यह क्रोधाग्नि पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरे को जलाती हुई स्व-पर दाहक बनती है।
1
क्रोध इन कारणों से उत्पन्न हो सकता है - ( १ ) दुर्वचन (२) स्वार्थ या कामपूर्ति में बाधा पड़ने से (३) अनुचित प्रतीत होने वाले व्यवहार से (४) भ्रम से या (५) विचार अथवा रुचि भेद से । क्रोध से उत्त्पन्न दोष इस रूप में हो सकते हैं - ( १ ) दुस्साहसी बनना ( २ ) चुगली करना (३) वैर बांधना (४) जलन रखना (५) दोष देखना, ढूंढना और आरोपण करना (६) दुष्ट ध्यान में रत रहना (७) कठोर वचन उच्चरित करना तथा (८) क्रूर व्यवहार करना ।
क्रोध के चार प्रकार बताये गये हैं- ( १ ) आभोग निवर्तित – पुष्ट कारण होने पर यह सोचकर कि ऐसा किये बिना सामने वाले को शिक्षा नहीं मिलेगी – जो क्रोध किया जाता है वह उस का आभोग निवर्तित प्रकार है । यह क्रोध क्रोध के विपाक को जानते हुए किया जाता है। (२) अनाभोग निवर्तित—जब कोई यों ही गुण दोष का विचार किये बिना परवश होकर क्रोध कर बैठता है अथवा क्रोध के विपाक को न जानते हुए क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध अनाभोग निवर्तित होता है । (३) उपशान्त - जो क्रोध सत्ता (अस्तित्व) में तो हो लेकिन उदयावस्था में न हो, उसे उपशान्त क्रोध कहते हैं। (४) अनुपशान्त - जो क्रोध उदयावस्था में आ जाय, वह अनुपशान्त क्रोध कहलाता
है ।
क्रोध की उत्पत्ति के भी चार प्रकार कहे गये हैं— (१) आत्म प्रतिष्ठित जो अपने आप में ही क्रोध करता रहे। अपने पर ही क्रोध आवे और अपने को ही भीतर जलाता रहे। (२) पर प्रतिष्ठित—जो क्रोध दूसरे के कारण आवे और दूसरे पर बरसे। (३) उभय प्रतिष्ठित - जिस क्रोध का कारण और ठहराव अपने और दूसरे दोनों के निमित्त से हो । (४) अप्रतिष्ठित – जो क्रोध बिना किसी निमित्त के ही भड़क उठे ।
1
कषाय के मूल प्रकारों के समान क्रोध के भी चार प्रकार इस रूप में बताये गये हैं : (१) अनन्तानुबंधी क्रोध - पर्वत के फट जाने पर जो दरार पड़ जाती है। जैसे उस दरार का मिलना कठिन होता है, वैसे ही इस प्रकार का क्रोध किसी भी उपाय से शान्त नहीं होता है । (२) अप्रत्याख्यानवरण क्रोध—सूखे तालाब आदि में मिट्टी के फट जाने पर दरारें पड़ जाती हैं किन्तु जब वर्षा होती है, तब वह फिर से मिल जाती है। वैसे ही इस प्रकार का क्रोध विशेष परिश्रम से शान्त होता है। (३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध – बालू में लकीर खींचने पर कुछ समय में हवा से वह लकीर वापस भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध कुछ उपाय से शान्त हो, वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहलाता है । (४) संज्वलन क्रोध – पानी में खींची हुई लकीर जैसे खिंचने के साथ ही मिट जाती है, वैसे ही किसी कारण से उदय में आया हुआ इस प्रकार का क्रोध शीघ्र ही शान्त हो जाता है।
२३०