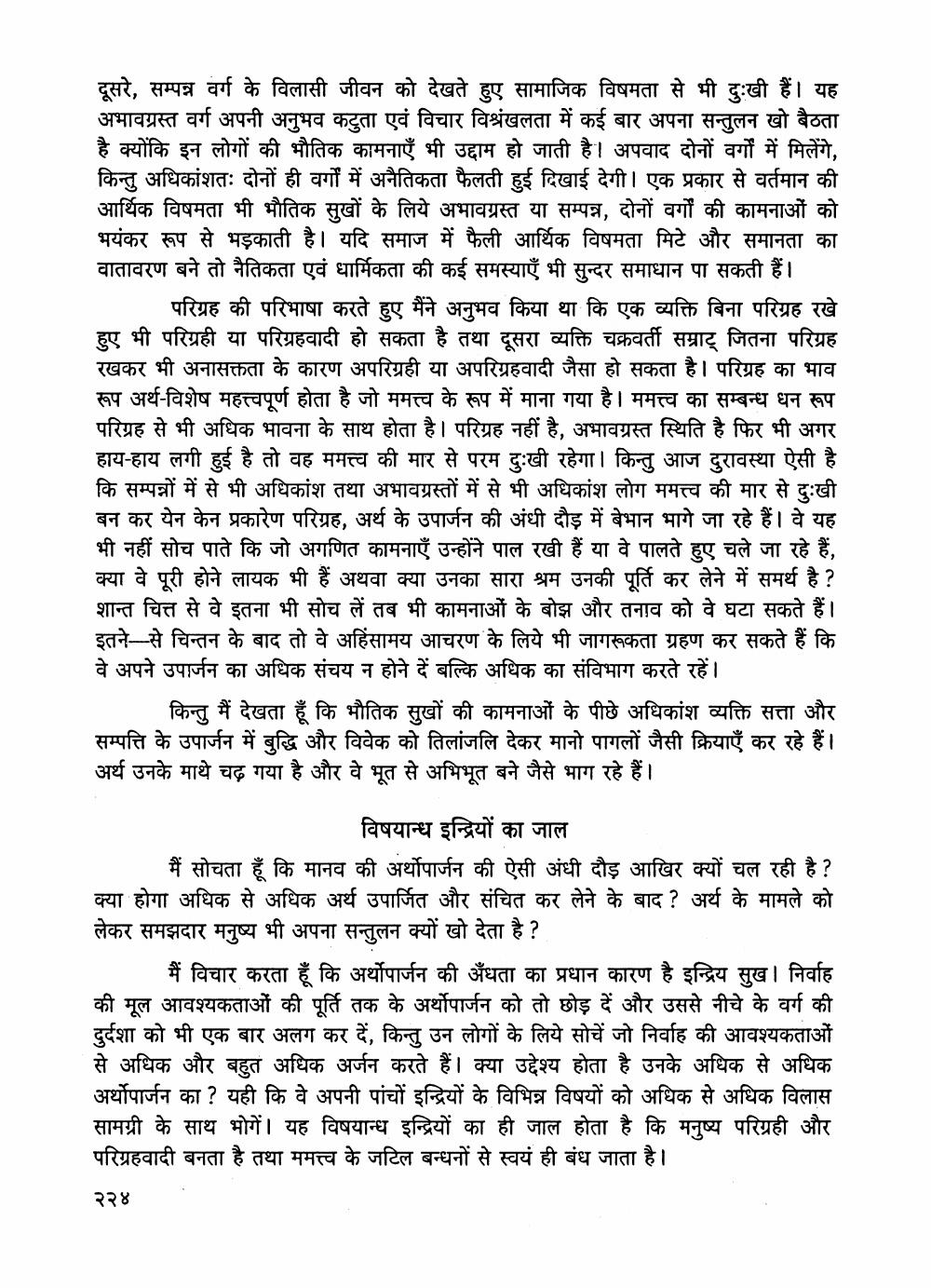________________
दूसरे, सम्पन्न वर्ग के विलासी जीवन को देखते हुए सामाजिक विषमता से भी दुःखी हैं। यह अभावग्रस्त वर्ग अपनी अनुभव कटुता एवं विचार विश्रंखलता में कई बार अपना सन्तुलन खो बैठता है क्योंकि इन लोगों की भौतिक कामनाएँ भी उद्दाम हो जाती है। अपवाद दोनों वर्गों में मिलेंगे, किन्तु अधिकांशतः दोनों ही वर्गों में अनैतिकता फैलती हुई दिखाई देगी। एक प्रकार से वर्तमान की आर्थिक विषमता भी भौतिक सुखों के लिये अभावग्रस्त या सम्पन्न, दोनों वर्गों की कामनाओं को भयंकर रूप से भड़काती है। यदि समाज में फैली आर्थिक विषमता मिटे और समानता का वातावरण बने तो नैतिकता एवं धार्मिकता की कई समस्याएँ भी सुन्दर समाधान पा सकती हैं।
परिग्रह की परिभाषा करते हुए मैंने अनुभव किया था कि एक व्यक्ति बिना परिग्रह रखे हुए भी परिग्रही या परिग्रहवादी हो सकता है तथा दूसरा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट् जितना परिग्रह रखकर भी अनासक्तता के कारण अपरिग्रही या अपरिग्रहवादी जैसा हो सकता है। परिग्रह का भाव रूप अर्थ-विशेष महत्त्वपूर्ण होता है जो ममत्त्व के रूप में माना गया है। ममत्त्व का सम्बन्ध धन रूप परिग्रह से भी अधिक भावना के साथ होता है। परिग्रह नहीं है, अभावग्रस्त स्थिति है फिर भी अगर हाय-हाय लगी हुई है तो वह ममत्त्व की मार से परम दुःखी रहेगा। किन्तु आज दुरावस्था ऐसी है कि सम्पन्नों में से भी अधिकांश तथा अभावग्रस्तों में से भी अधिकांश लोग ममत्त्व की मार से दुःखी बन कर येन केन प्रकारेण परिग्रह, अर्थ के उपार्जन की अंधी दौड़ में बेभान भागे जा रहे हैं। वे यह भी नहीं सोच पाते कि जो अगणित कामनाएँ उन्होंने पाल रखी हैं या वे पालते हुए चले जा रहे हैं, क्या वे पूरी होने लायक भी हैं अथवा क्या उनका सारा श्रम उनकी पूर्ति कर लेने में समर्थ है ? शान्त चित्त से वे इतना भी सोच लें तब भी कामनाओं के बोझ और तनाव को वे घटा सकते हैं। इतने से चिन्तन के बाद तो वे अहिंसामय आचरण के लिये भी जागरूकता ग्रहण कर सकते हैं कि वे अपने उपार्जन का अधिक संचय न होने दें बल्कि अधिक का संविभाग करते रहें।
किन्तु मैं देखता हूँ कि भौतिक सुखों की कामनाओं के पीछे अधिकांश व्यक्ति सत्ता और सम्पत्ति के उपार्जन में बुद्धि और विवेक को तिलांजलि देकर मानो पागलों जैसी क्रियाएँ कर रहे हैं। अर्थ उनके माथे चढ़ गया है और वे भूत से अभिभूत बने जैसे भाग रहे हैं।
विषयान्ध इन्द्रियों का जाल मैं सोचता हूँ कि मानव की अर्थोपार्जन की ऐसी अंधी दौड़ आखिर क्यों चल रही है ? क्या होगा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जित और संचित कर लेने के बाद ? अर्थ के मामले को लेकर समझदार मनुष्य भी अपना सन्तुलन क्यों खो देता है ?
मैं विचार करता हूँ कि अर्थोपार्जन की अँधता का प्रधान कारण है इन्द्रिय सुख । निर्वाह की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तक के अर्थोपार्जन को तो छोड़ दें और उससे नीचे के वर्ग की दुर्दशा को भी एक बार अलग कर दें, किन्तु उन लोगों के लिये सोचें जो निर्वाह की आवश्यकताओं से अधिक और बहुत अधिक अर्जन करते हैं। क्या उद्देश्य होता है उनके अधिक से अधिक अर्थोपार्जन का? यही कि वे अपनी पांचों इन्द्रियों के विभिन्न विषयों को अधिक से अधिक विलास सामग्री के साथ भोगें। यह विषयान्ध इन्द्रियों का ही जाल होता है कि मनुष्य परिग्रही और परिग्रहवादी बनता है तथा ममत्त्व के जटिल बन्धनों से स्वयं ही बंध जाता है।
२२४