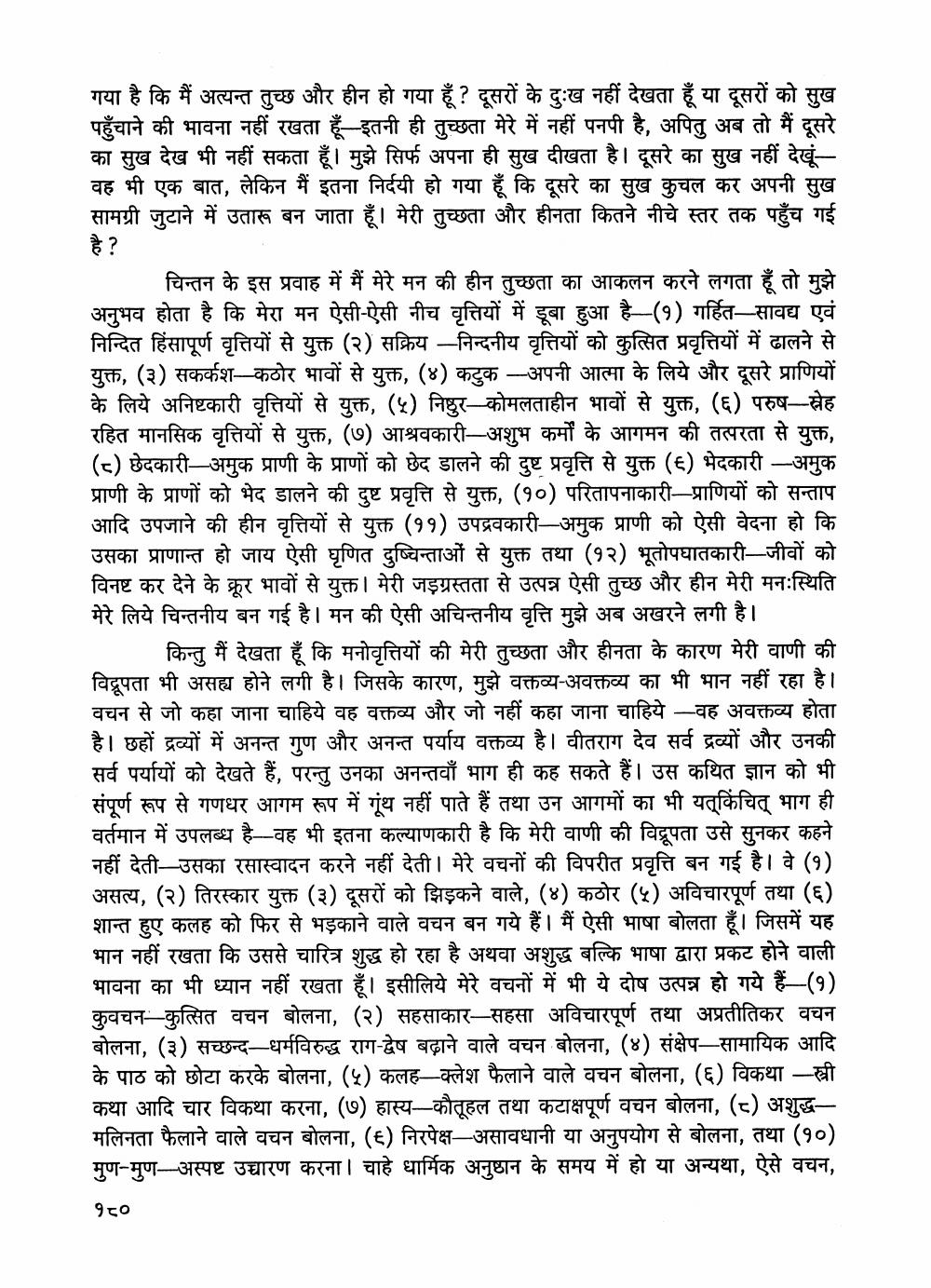________________
गया है कि मैं अत्यन्त तुच्छ और हीन हो गया हूँ ? दूसरों के दुःख नहीं देखता हूँ या दूसरों को सुख पहुँचाने की भावना नहीं रखता हूँ—इतनी ही तुच्छता मेरे में नहीं पनपी है, अपितु अब तो मैं दूसरे का सुख देख भी नहीं सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपना ही सुख दीखता है। दूसरे का सुख नहीं देखूवह भी एक बात, लेकिन मैं इतना निर्दयी हो गया हूँ कि दूसरे का सुख कुचल कर अपनी सुख सामग्री जुटाने में उतारू बन जाता हूँ। मेरी तुच्छता और हीनता कितने नीचे स्तर तक पहुँच गई
___ चिन्तन के इस प्रवाह में मैं मेरे मन की हीन तुच्छता का आकलन करने लगता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि मेरा मन ऐसी-ऐसी नीच वृत्तियों में डूबा हुआ है—(१) गर्हित—सावद्य एवं निन्दित हिंसापूर्ण वृत्तियों से युक्त (२) सक्रिय –निन्दनीय वृत्तियों को कुत्सित प्रवृत्तियों में ढालने से युक्त, (३) सकर्कश कठोर भावों से युक्त, (४) कटुक -अपनी आत्मा के लिये और दूसरे प्राणियों के लिये अनिष्टकारी वृत्तियों से युक्त, (५) निष्ठुर–कोमलताहीन भावों से युक्त, (६) परुष-स्नेह रहित मानसिक वृत्तियों से युक्त, (७) आश्रवकारी–अशुभ कर्मों के आगमन की तत्परता से युक्त, (८) छेदकारी-अमुक प्राणी के प्राणों को छेद डालने की दुष्ट प्रवृत्ति से युक्त (६) भेदकारी -अमुक प्राणी के प्राणों को भेद डालने की दुष्ट प्रवृत्ति से युक्त, (१०) परितापनाकारी प्राणियों को सन्ताप आदि उपजाने की हीन वृत्तियों से युक्त (११) उपद्रवकारी-अमुक प्राणी को ऐसी वेदना हो कि उसका प्राणान्त हो जाय ऐसी घृणित दुष्चिन्ताओं से युक्त तथा (१२) भूतोपघातकारी—जीवों को विनष्ट कर देने के क्रूर भावों से युक्त। मेरी जड़ग्रस्तता से उत्पन्न ऐसी तुच्छ और हीन मेरी मनःस्थिति मेरे लिये चिन्तनीय बन गई है। मन की ऐसी अचिन्तनीय वृत्ति मुझे अब अखरने लगी है।
किन्तु मैं देखता हूँ कि मनोवृत्तियों की मेरी तुच्छता और हीनता के कारण मेरी वाणी की विद्रूपता भी असह्य होने लगी है। जिसके कारण, मुझे वक्तव्य-अवक्तव्य का भी भान नहीं रहा है। वचन से जो कहा जाना चाहिये वह वक्तव्य और जो नहीं कहा जाना चाहिये -वह अवक्तव्य होता है। छहों द्रव्यों में अनन्त गुण और अनन्त पर्याय वक्तव्य है। वीतराग देव सर्व द्रव्यों और उनकी सर्व पर्यायों को देखते हैं, परन्तु उनका अनन्तवाँ भाग ही कह सकते हैं। उस कथित ज्ञान को भी संपूर्ण रूप से गणधर आगम रूप में गूंथ नहीं पाते हैं तथा उन आगमों का भी यत्किंचित् भाग ही वर्तमान में उपलब्ध है—वह भी इतना कल्याणकारी है कि मेरी वाणी की विद्रूपता उसे सुनकर कहने नहीं देती-उसका रसास्वादन करने नहीं देती। मेरे वचनों की विपरीत प्रवृत्ति बन गई है। वे (१) असत्य, (२) तिरस्कार युक्त (३) दूसरों को झिड़कने वाले, (४) कठोर (५) अविचारपूर्ण तथा (६) शान्त हुए कलह को फिर से भड़काने वाले वचन बन गये हैं। मैं ऐसी भाषा बोलता हूँ। जिसमें यह भान नहीं रखता कि उससे चारित्र शुद्ध हो रहा है अथवा अशुद्ध बल्कि भाषा द्वारा प्रकट होने वाली भावना का भी ध्यान नहीं रखता हूँ। इसीलिये मेरे वचनों में भी ये दोष उत्पन्न हो गये हैं—(१) कुवचन-कुत्सित वचन बोलना, (२) सहसाकार-सहसा अविचारपूर्ण तथा अप्रतीतिकर वचन बोलना, (३) सच्छन्द-धर्मविरुद्ध राग-द्वेष बढ़ाने वाले वचन बोलना, (४) संक्षेप–सामायिक आदि के पाठ को छोटा करके बोलना, (५) कलह-क्लेश फैलाने वाले वचन बोलना, (६) विकथा -स्त्री कथा आदि चार विकथा करना, (७) हास्य–कौतूहल तथा कटाक्षपूर्ण वचन बोलना, (८) अशुद्धमलिनता फैलाने वाले वचन बोलना, (६) निरपेक्ष–असावधानी या अनुपयोग से बोलना, तथा (१०) मुण-मुण-अस्पष्ट उच्चारण करना। चाहे धार्मिक अनुष्ठान के समय में हो या अन्यथा, ऐसे वचन, १८०