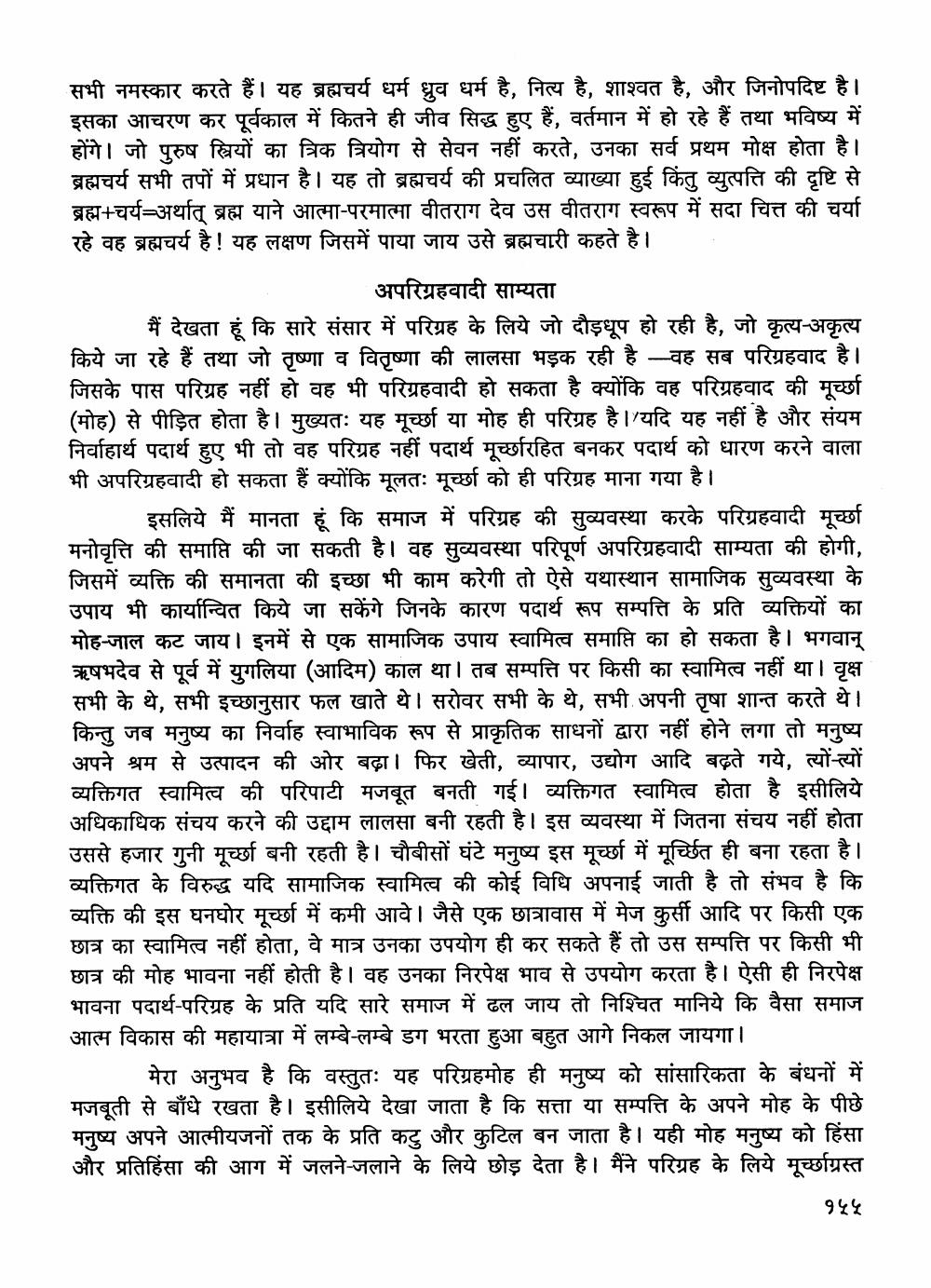________________
सभी नमस्कार करते हैं। यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव धर्म है, नित्य है, शाश्वत है, और जिनोपदिष्ट है। इसका आचरण कर पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं तथा भविष्य में होंगे। जो पुरुष स्त्रियों का त्रिक त्रियोग से सेवन नहीं करते, उनका सर्व प्रथम मोक्ष होता है। ब्रह्मचर्य सभी तपों में प्रधान है। यह तो ब्रह्मचर्य की प्रचलित व्याख्या हुई किंतु व्युत्पत्ति की दृष्टि से ब्रह्मचर्य-अर्थात् ब्रह्म याने आत्मा-परमात्मा वीतराग देव उस वीतराग स्वरूप में सदा चित्त की चर्या रहे वह ब्रह्मचर्य है! यह लक्षण जिसमें पाया जाय उसे ब्रह्मचारी कहते है।
अपरिग्रहवादी साम्यता ___ मैं देखता हूं कि सारे संसार में परिग्रह के लिये जो दौड़धूप हो रही है, जो कृत्य-अकृत्य किये जा रहे हैं तथा जो तृष्णा व वितृष्णा की लालसा भड़क रही है —वह सब परिग्रहवाद है। जिसके पास परिग्रह नहीं हो वह भी परिग्रहवादी हो सकता है क्योंकि वह परिग्रहवाद की मूर्छा (मोह) से पीड़ित होता है। मुख्यतः यह मूर्छा या मोह ही परिग्रह है। यदि यह नहीं है और संयम निर्वाहार्थ पदार्थ हुए भी तो वह परिग्रह नहीं पदार्थ मूरिहित बनकर पदार्थ को धारण करने वाला भी अपरिग्रहवादी हो सकता हैं क्योंकि मूलतः मूर्छा को ही परिग्रह माना गया है।
इसलिये मैं मानता हूं कि समाज में परिग्रह की सुव्यवस्था करके परिग्रहवादी मूर्छा मनोवृत्ति की समाप्ति की जा सकती है। वह सुव्यवस्था परिपूर्ण अपरिग्रहवादी साम्यता की होगी, जिसमें व्यक्ति की समानता की इच्छा भी काम करेगी तो ऐसे यथास्थान सामाजिक सुव्यवस्था के उपाय भी कार्यान्वित किये जा सकेंगे जिनके कारण पदार्थ रूप सम्पत्ति के प्रति व्यक्तियों का मोह-जाल कट जाय। इनमें से एक सामाजिक उपाय स्वामित्व समाप्ति का हो सकता है। भगवान् ऋषभदेव से पूर्व में युगलिया (आदिम) काल था। तब सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्व नहीं था। वृक्ष सभी के थे, सभी इच्छानुसार फल खाते थे। सरोवर सभी के थे, सभी अपनी तृषा शान्त करते थे। किन्तु जब मनुष्य का निर्वाह स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक साधनों द्वारा नहीं होने लगा तो मनुष्य अपने श्रम से उत्पादन की ओर बढ़ा। फिर खेती, व्यापार, उद्योग आदि बढ़ते गये, त्यों-त्यों व्यक्तिगत स्वामित्व की परिपाटी मजबूत बनती गई। व्यक्तिगत स्वामित्व होता है इसीलिये अधिकाधिक संचय करने की उद्दाम लालसा बनी रहती है। इस व्यवस्था में जितना संचय नहीं होता उससे हजार गुनी मूर्छा बनी रहती है। चौबीसों घंटे मनुष्य इस मूर्छा में मूर्छित ही बना रहता है। व्यक्तिगत के विरुद्ध यदि सामाजिक स्वामित्व की कोई विधि अपनाई जाती है तो संभव है कि व्यक्ति की इस घनघोर मूर्छा में कमी आवे। जैसे एक छात्रावास में मेज कुर्सी आदि पर किसी एक छात्र का स्वामित्व नहीं होता, वे मात्र उनका उपयोग ही कर सकते हैं तो उस सम्पत्ति पर किसी भी छात्र की मोह भावना नहीं होती है। वह उनका निरपेक्ष भाव से उपयोग करता है। ऐसी ही निरपेक्ष भावना पदार्थ-परिग्रह के प्रति यदि सारे समाज में ढल जाय तो निश्चित मानिये कि वैसा समाज आत्म विकास की महायात्रा में लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ बहुत आगे निकल जायगा।
मेरा अनुभव है कि वस्तुतः यह परिग्रहमोह ही मनुष्य को सांसारिकता के बंधनों में मजबूती से बाँधे रखता है। इसीलिये देखा जाता है कि सत्ता या सम्पत्ति के अपने मोह के पीछे मनुष्य अपने आत्मीयजनों तक के प्रति कटु और कुटिल बन जाता है। यही मोह मनुष्य को हिंसा और प्रतिहिंसा की आग में जलने जलाने के लिये छोड़ देता है। मैंने परिग्रह के लिये मूर्छाग्रस्त
१५५