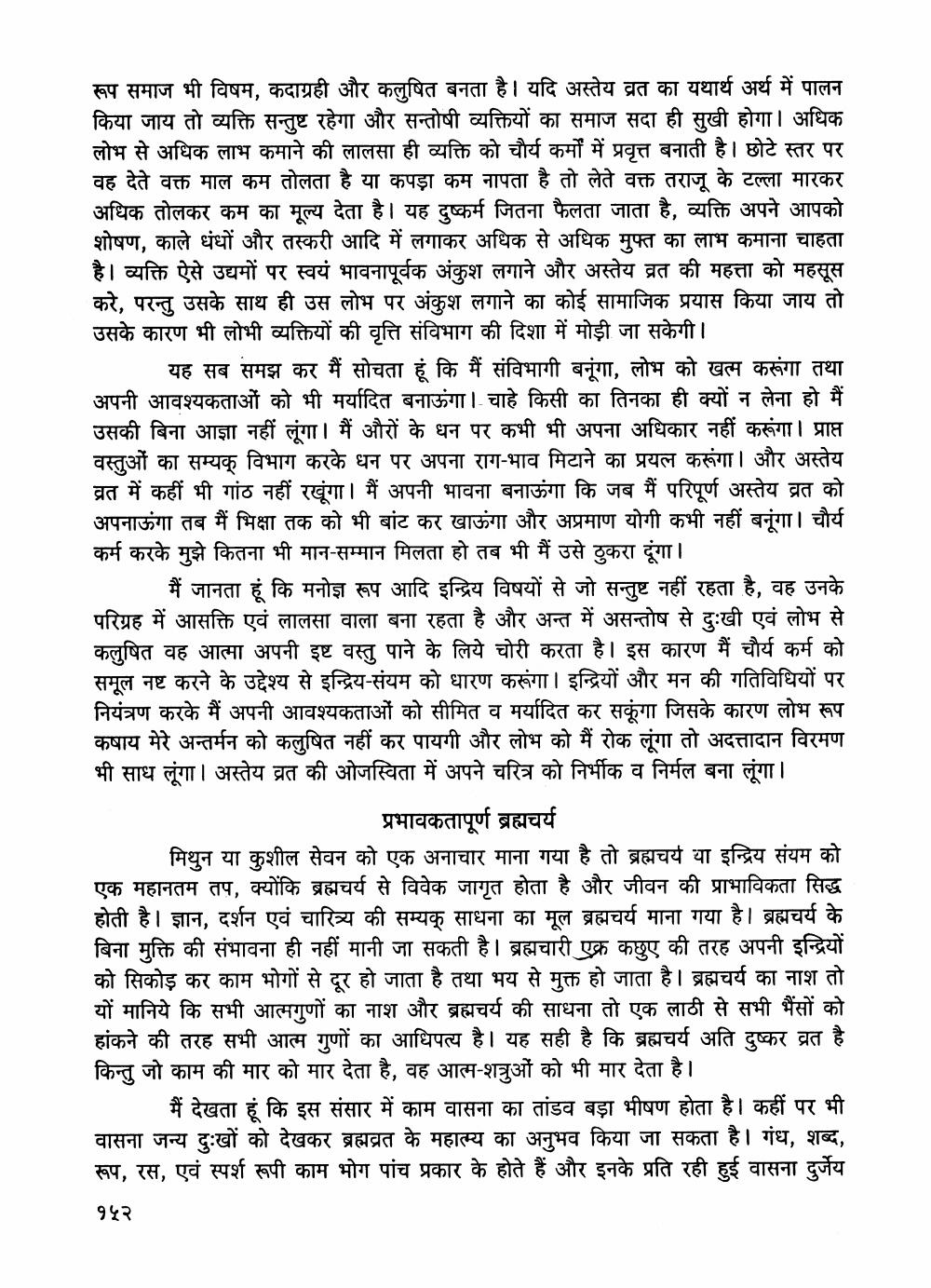________________
रूप समाज भी विषम, कदाग्रही और कलुषित बनता है । यदि अस्तेय व्रत का यथार्थ अर्थ में पालन किया जाय तो व्यक्ति सन्तुष्ट रहेगा और सन्तोषी व्यक्तियों का समाज सदा ही सुखी होगा। अधिक लोभ से अधिक लाभ कमाने की लालसा ही व्यक्ति को चौर्य कर्मों में प्रवृत्त बनाती है। छोटे स्तर पर वह देते वक्त माल कम तोलता है या कपड़ा कम नापता है तो लेते वक्त तराजू के टल्ला मारकर अधिक तोलकर कम का मूल्य देता है । यह दुष्कर्म जितना फैलता जाता है, व्यक्ति अपने आपको शोषण, काले धंधों और तस्करी आदि में लगाकर अधिक से अधिक मुफ्त का लाभ कमाना चाहता है। व्यक्ति ऐसे उद्यमों पर स्वयं भावनापूर्वक अंकुश लगाने और अस्तेय व्रत की महत्ता को महसूस करे, परन्तु उसके साथ ही उस लोभ पर अंकुश लगाने का कोई सामाजिक प्रयास किया जाय तो उसके कारण भी लोभी व्यक्तियों की वृत्ति संविभाग की दिशा में मोड़ी जा सकेगी।
यह सब समझ कर मैं सोचता हूं कि मैं संविभागी बनूंगा, लोभ को खत्म करूंगा तथा अपनी आवश्यकताओं को भी मर्यादित बनाऊंगा। चाहे किसी का तिनका ही क्यों न लेना हो मैं उसकी बिना आज्ञा नहीं लूंगा। मैं औरों के धन पर कभी भी अपना अधिकार नहीं करूंगा । प्राप्त वस्तुओं का सम्यक् विभाग करके धन पर अपना राग भाव मिटाने का प्रयत्न करूंगा । और अस्तेय व्रत में कहीं भी गांठ नहीं रखूंगा। मैं अपनी भावना बनाऊंगा कि जब मैं परिपूर्ण अस्तेय व्रत को अपनाऊंगा तब मैं भिक्षा तक को भी बांट कर खाऊंगा और अप्रमाण योगी कभी नहीं बनूंगा। चौर्य कर्म करके मुझे कितना भी मान-सम्मान मिलता हो तब भी मैं उसे ठुकरा दूंगा ।
मैं जानता हूं कि मनोज्ञ रूप आदि इन्द्रिय विषयों से जो सन्तुष्ट नहीं रहता है, वह उनके परिग्रह में आसक्ति एवं लालसा वाला बना रहता है और अन्त में असन्तोष से दुःखी एवं लोभ से कलुषित वह आत्मा अपनी इष्ट वस्तु पाने के लिये चोरी करता है। इस कारण मैं चौर्य कर्म को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इन्द्रिय-संयम को धारण करूंगा । इन्द्रियों और मन की गतिविधियों पर नियंत्रण करके मैं अपनी आवश्यकताओं को सीमित व मर्यादित कर सकूंगा जिसके कारण लोभ रूप कषाय मेरे अन्तर्मन को कलुषित नहीं कर पायगी और लोभ को मैं रोक लूंगा तो अदत्तादान विरमण भी साध लूंगा । अस्तेय व्रत की ओजस्विता में अपने चरित्र को निर्भीक व निर्मल बना लूंगा ।
प्रभावकतापूर्ण ब्रह्मचर्य
मिथुन या कुशील सेवन को एक अनाचार माना गया है तो ब्रह्मचर्य या इन्द्रिय संयम को एक महानतम तप, क्योंकि ब्रह्मचर्य से विवेक जागृत होता है और जीवन की प्राभाविकता सिद्ध होती है। ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की सम्यक् साधना का मूल ब्रह्मचर्य माना गया है। ब्रह्मचर्य के बिना मुक्ति की संभावना ही नहीं मानी जा सकती है। ब्रह्मचारी एक कछुए की तरह अपनी इन्द्रियों को सिकोड़ कर काम भोगों से दूर हो जाता है तथा भय से मुक्त हो जाता है । ब्रह्मचर्य का नाश तो यों मानिये कि सभी आत्मगुणों का नाश और ब्रह्मचर्य की साधना तो एक लाठी से सभी भैंसों को हांकने की तरह सभी आत्म गुणों का आधिपत्य है । यह सही है कि ब्रह्मचर्य अति दुष्कर व्रत है किन्तु जो काम की मार को मार देता है, वह आत्म-शत्रुओं को भी मार देता है ।
मैं देखता हूं कि इस संसार में काम वासना का तांडव बड़ा भीषण होता है । कहीं पर भी वासना जन्य दुःखों को देखकर ब्रह्मव्रत के महात्म्य का अनुभव किया जा सकता है। गंध, शब्द, रूप, रस, एवं स्पर्श रूपी काम भोग पांच प्रकार के होते हैं और इनके प्रति रही हुई वासना दुर्जेय
१५२