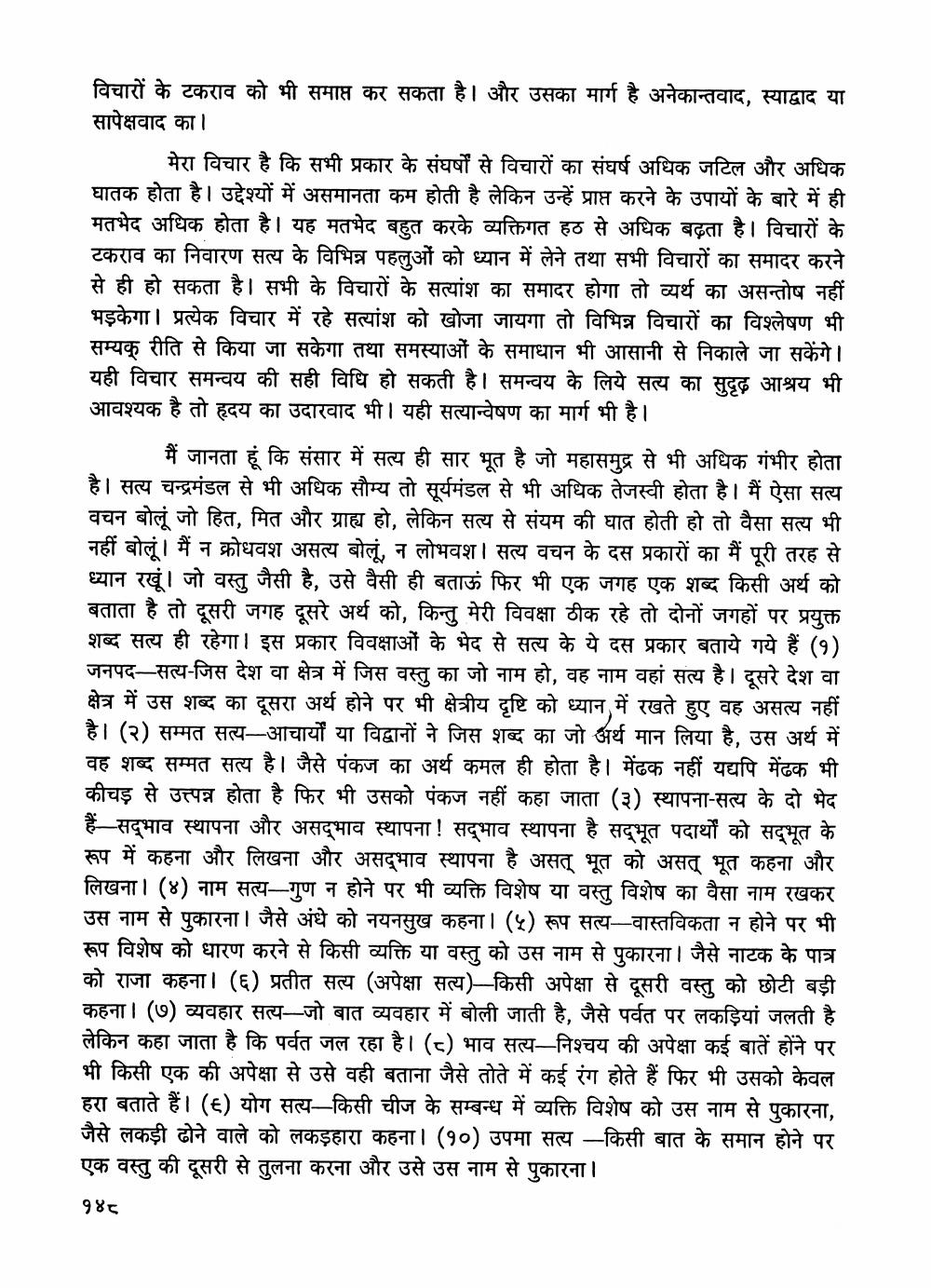________________
विचारों के टकराव को भी समाप्त कर सकता है। और उसका मार्ग है अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या सापेक्षवाद का ।
मेरा विचार है कि सभी प्रकार के संघर्षों से विचारों का संघर्ष अधिक जटिल और अधिक घातक होता है । उद्देश्यों में असमानता कम होती है लेकिन उन्हें प्राप्त करने के उपायों के बारे में ही मतभेद अधिक होता है। यह मतभेद बहुत करके व्यक्तिगत हठ से अधिक बढ़ता है। विचारों के टकराव का निवारण सत्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में लेने तथा सभी विचारों का समादर करने से ही हो सकता है। सभी के विचारों के सत्यांश का समादर होगा तो व्यर्थ का असन्तोष नहीं भड़केगा । प्रत्येक विचार में रहे सत्यांश को खोजा जायगा तो विभिन्न विचारों का विश्लेषण भी सम्यक् रीति से किया जा सकेगा तथा समस्याओं के समाधान भी आसानी से निकाले जा सकेंगे। यही विचार समन्वय की सही विधि हो सकती है। समन्वय के लिये सत्य का सुदृढ़ आश्रय भी आवश्यक है तो हृदय का उदारवाद भी । यही सत्यान्वेषण का मार्ग भी है ।
मैं जानता हूं कि संसार में सत्य ही सार भूत है जो महासमुद्र से भी अधिक गंभीर होता है । सत्य चन्द्रमंडल से भी अधिक सौम्य तो सूर्यमंडल से भी अधिक तेजस्वी होता है। मैं ऐसा सत्य वचन बोलूं जो हित, मित और ग्राह्य हो, लेकिन सत्य से संयम की घात होती हो तो वैसा सत्य भी नहीं बोलूं । मैं न क्रोधवश असत्य बोलूं, न लोभवश । सत्य वचन के दस प्रकारों का मैं पूरी तरह से ध्यान रखूं। जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही बताऊं फिर भी एक जगह एक शब्द किसी अर्थ को बताता है तो दूसरी जगह दूसरे अर्थ को, किन्तु मेरी विवक्षा ठीक रहे तो दोनों जगहों पर प्रयुक्त शब्द सत्य ही रहेगा। इस प्रकार विवक्षाओं के भेद सत्य के ये दस प्रकार बताये गये हैं (१) जनपद - सत्य - जिस देश वा क्षेत्र में जिस वस्तु का जो नाम हो, वह नाम वहां सत्य है। दूसरे देश वा क्षेत्र में उस शब्द का दूसरा अर्थ होने पर भी क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह असत्य नहीं है । ( २ ) सम्मत सत्य - आचार्यों या विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है, उस अर्थ में वह शब्द सम्मत सत्य है। जैसे पंकज का अर्थ कमल ही होता है । मेंढक नहीं यद्यपि मेंढक भी कीचड़ से उत्त्पन्न होता है फिर भी उसको पंकज नहीं कहा जाता (३) स्थापना - सत्य के दो भेद हैं— सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना ! सद्भाव स्थापना है सद्भूत पदार्थों को सद्भूत रूप में कहना और लिखना और असद्भाव स्थापना है असत् भूत को असत् भूत कहना और लिखना । (४) नाम सत्य - गुण न होने पर भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का वैसा नाम रखकर उस नाम पुकारना । जैसे अंधे को नयनसुख कहना । (५) रूप सत्य - वास्तविकता न होने पर भी रूप विशेष को धारण करने से किसी व्यक्ति या वस्तु को उस नाम से पुकारना । जैसे नाटक के पात्र को राजा कहना । (६) प्रतीत सत्य ( अपेक्षा सत्य ) - किसी अपेक्षा से दूसरी वस्तु को छोटी बड़ी कहना । (७) व्यवहार सत्य - जो बात व्यवहार में बोली जाती है, जैसे पर्वत पर लकड़ियां जलती है। लेकिन कहा जाता है कि पर्वत जल रहा है । (८) भाव सत्य - निश्चय अपेक्षा कई बातें होंने पर भी किसी एक की अपेक्षा से उसे वही बताना जैसे तोते में कई रंग होते हैं फिर भी उसको केवल हरा बताते हैं । (६) योग सत्य - किसी चीज के सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष को उस नाम से पुकारना, जैसे लकड़ी ढोने वाले को लकड़हारा कहना । (१०) उपमा सत्य - किसी बात के समान होने पर एक वस्तु की दूसरी से तुलना करना और उसे उस नाम से पुकारना ।
१४८