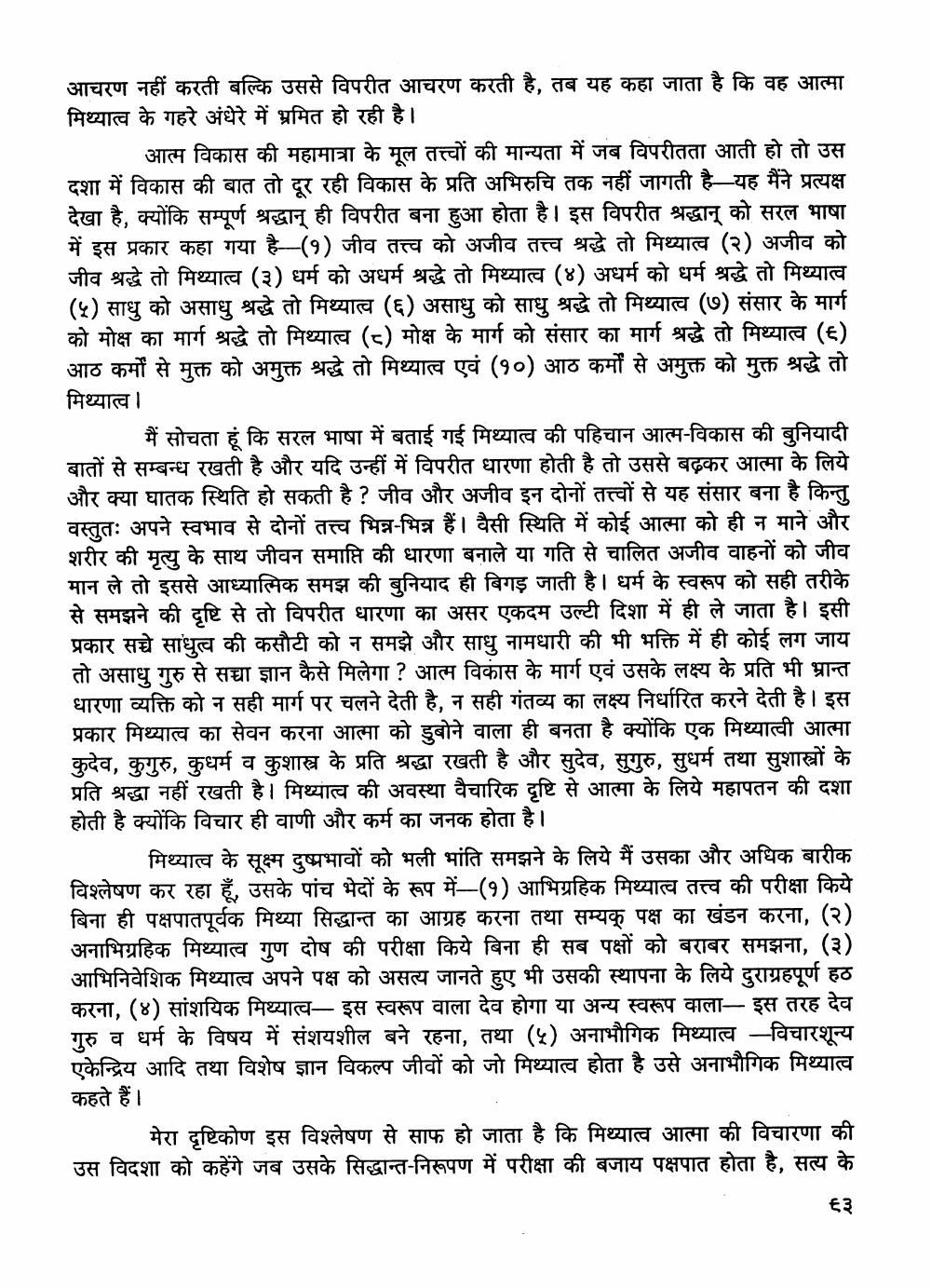________________
आचरण नहीं करती बल्कि उससे विपरीत आचरण करती है, तब यह कहा जाता है कि वह आत्मा मिथ्यात्व के गहरे अंधेरे में भ्रमित हो रही है ।
आत्म विकास की महामात्रा के मूल तत्त्वों की मान्यता में जब विपरीतता आती हो तो उस दशा में विकास की बात तो दूर रही विकास के प्रति अभिरुचि तक नहीं जागती है—यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि सम्पूर्ण श्रद्धान् ही विपरीत बना हुआ होता है। इस विपरीत श्रद्धान् को सरल भाषा में इस प्रकार कहा गया है– (१) जीव तत्त्व को अजीव तत्त्व श्रद्धे तो मिथ्यात्व (२) अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व (३) धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व (४) अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व (५) साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व (६) असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व (७) संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व (८) मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व (६) आठ कर्मों से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व एवं (१०) आठ कर्मों से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व |
मैं सोचता हूं कि सरल भाषा में बताई गई मिथ्यात्व की पहिचान आत्म-विकास की बुनियादी बातों से सम्बन्ध रखती है और यदि उन्हीं में विपरीत धारणा होती है 'उससे बढ़कर आत्मा के लिये और क्या घातक स्थिति हो सकती है ? जीव और अजीव इन दोनों तत्त्वों से यह संसार बना है किन्तु वस्तुतः अपने स्वभाव से दोनों तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं । वैसी स्थिति में कोई आत्मा को ही न माने और शरीर की मृत्यु के साथ जीवन समाप्ति की धारणा बनाले या गति से चालित अजीव वाहनों को जीव मान ले तो इससे आध्यात्मिक समझ की बुनियाद ही बिगड़ जाती है। धर्म के स्वरूप को सही तरीके से समझने की दृष्टि से तो विपरीत धारणा का असर एकदम उल्टी दिशा में ही ले जाता है। इसी प्रकार सच्चे सांधुत्व की कसौटी को न समझे और साधु नामधारी की भी भक्ति में ही कोई लग जाय तो असाधु गुरु से सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा ? आत्म विकास के मार्ग एवं उसके लक्ष्य के प्रति भी धारणा व्यक्ति को न सही मार्ग पर चलने देती है, न सही गंतव्य का लक्ष्य निर्धारित करने देती है । इस प्रकार मिथ्यात्व का सेवन करना आत्मा को डुबोने वाला ही बनता है क्योंकि एक मिथ्यात्वी आत्मा कुदेव, कुगुरु, कुधर्म व कुशास्त्र के प्रति श्रद्धा रखती है और सुदेव, सुगुरु, सुधर्म तथा सुशास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखती है । मिथ्यात्व की अवस्था वैचारिक दृष्टि से आत्मा के लिये महापतन की दशा होती है क्योंकि विचार ही वाणी और कर्म का जनक होता है ।
मिथ्यात्व के सूक्ष्म दुष्प्रभावों को भली भांति समझने के लिये मैं उसका और अधिक बारीक विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके पांच भेदों के रूप में – (१) आभिग्रहिक मिथ्यात्व तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपातपूर्वक मिथ्या सिद्धान्त का आग्रह करना तथा सम्यक् पक्ष का खंडन करना, (२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व गुण दोष की परीक्षा किये बिना ही सब पक्षों को बराबर समझना, (३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी स्थापना के लिये दुराग्रहपूर्ण हठ करना, (४) सांशयिक मिथ्यात्व — इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप वाला—- इस तरह देव गुरु व धर्म के विषय में संशयशील बने रहना, तथा ( ५ ) अनाभौगिक मिथ्यात्व – विचारशून्य एकेन्द्रिय आदि तथा विशेष ज्ञान विकल्प जीवों को जो मिथ्यात्व होता है उसे अनाभौगिक मिथ्यात्व कहते हैं ।
मेरा दृष्टिकोण इस विश्लेषण से साफ हो जाता है कि मिथ्यात्व आत्मा की विचारणा की उस विदशा को कहेंगे जब उसके सिद्धान्त - निरूपण में परीक्षा की बजाय पक्षपात होता है, सत्य के
६३