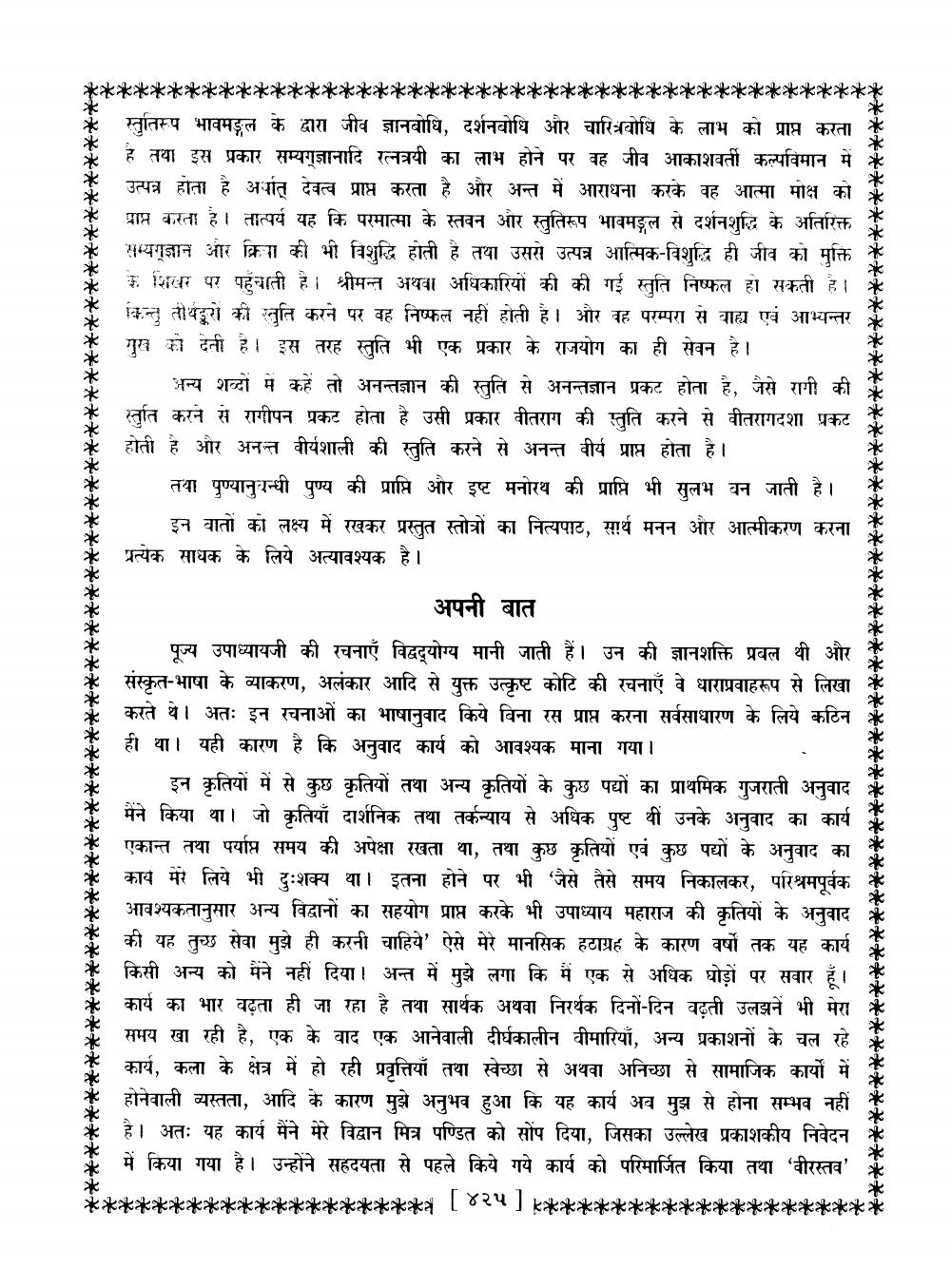________________
*********************************************** * स्तुतिस्प भावमडल के द्वारा जीव ज्ञानबोधि, दर्शनबोधि और चारित्रबोधि के लाभ को प्राप्त करता
है तथा इस प्रकार सम्यगज्ञानादि रत्नत्रयी का लाभ होने पर वह जीव आकाशवर्ती कल्पविमान में उत्पन्न होता है अर्थात् देवत्व प्राप्त करता है और अन्त में आराधना करके वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह कि परमात्मा के स्तवन और स्तुतिरूप भावमङ्गल से दर्शनशुद्धि के अतिरिक्त सम्यगज्ञान और क्रिया की भी विशुद्धि होती है तथा उससे उत्पन्न आत्मिक-विशुद्धि ही जीव को मुक्ति के शिखर पर पहुंचाती है। श्रीमन्त अथवा अधिकारियों की की गई स्तुति निष्फल हो सकती है। किन्तु तीथरों की स्तुति करने पर वह निष्फल नहीं होती है। और वह परम्परा से वाह्य एवं आभ्यन्तर गुख को देती है। इस तरह स्तुति भी एक प्रकार के राजयोग का ही सेवन है।
अन्य शब्दों में कहें तो अनन्तज्ञान की स्तुति से अनन्तज्ञान प्रकट होता है, जैसे रागी की * स्तुति करने से रागीपन प्रकट होता है उसी प्रकार वीतराग की स्तुति करने से वीतरागदशा प्रकट * होती है और अनन्त वीर्यशाली की स्तुति करने से अनन्त वीर्य प्राप्त होता है।
तथा पुण्यानुवन्धी पुण्य की प्राप्ति और इष्ट मनोरथ की प्राप्ति भी सुलभ बन जाती है।
इन बातों को लक्ष्य में रखकर प्रस्तुत स्तोत्रों का नित्यपाट, सार्थ मनन और आत्मीकरण करना प्रत्येक साधक के लिये अत्यावश्यक है।
अपनी बात पूज्य उपाध्यायजी की रचनाएँ विद्वद्योग्य मानी जाती हैं। उन की ज्ञानशक्ति प्रवल थी और * संस्कृत-भाषा के व्याकरण, अलंकार आदि से युक्त उत्कृष्ट कोटि की रचनाएँ वे धाराप्रवाहरूप से लिखा
करते थे। अतः इन रचनाओं का भाषानुवाद किये बिना रस प्राप्त करना सर्वसाधारण के लिये कठिन * * ही था। यही कारण है कि अनुवाद कार्य को आवश्यक माना गया।
इन कृतियों में से कुछ कृतियों तथा अन्य कृतियों के कुछ पद्यों का प्राथमिक गुजराती अनुवाद * * मैंने किया था। जो कृतियाँ दार्शनिक तथा तर्कन्याय से अधिक पुष्ट थीं उनके अनुवाद का कार्य *
एकान्त तथा पर्याप्त समय की अपेक्षा रखता था, तथा कुछ कृतियों एवं कुछ पद्यों के अनुवाद का * * काय मेरे लिये भी दुःशक्य था। इतना होने पर भी 'जैसे तैसे समय निकालकर, परिश्रमपूर्वक * * आवश्यकतानुसार अन्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त करके भी उपाध्याय महाराज की कृतियों के अनुवाद * * की यह तुच्छ सेवा मुझे ही करनी चाहिये' ऐसे मेरे मानसिक हटाग्रह के कारण वर्षों तक यह कार्य * किसी अन्य को मैंने नहीं दिया। अन्त में मुझे लगा कि मैं एक से अधिक घोड़ों पर सवार हूँ। * कार्य का भार बढ़ता ही जा रहा है तथा सार्थक अथवा निरर्थक दिनों-दिन बढ़ती उलझनें भी मेरा * * समय खा रही है, एक के बाद एक आनेवाली दीर्घकालीन वीमारियाँ, अन्य प्रकाशनों के चल रहे * * कार्य, कला के क्षेत्र में हो रही प्रवृत्तियाँ तथा स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से सामाजिक कार्यों में * * होनेवाली व्यस्तता, आदि के कारण मुझे अनुभव हुआ कि यह कार्य अब मुझ से होना सम्भव नहीं *
है। अतः यह कार्य मैंने मेरे विद्वान मित्र पण्डित को सोंप दिया, जिसका उल्लेख प्रकाशकीय निवेदन
में किया गया है। उन्होंने सहृदयता से पहले किये गये कार्य को परिमार्जित किया तथा 'वीरस्तव' * ******************** [४२५] ********************
***************************************************************