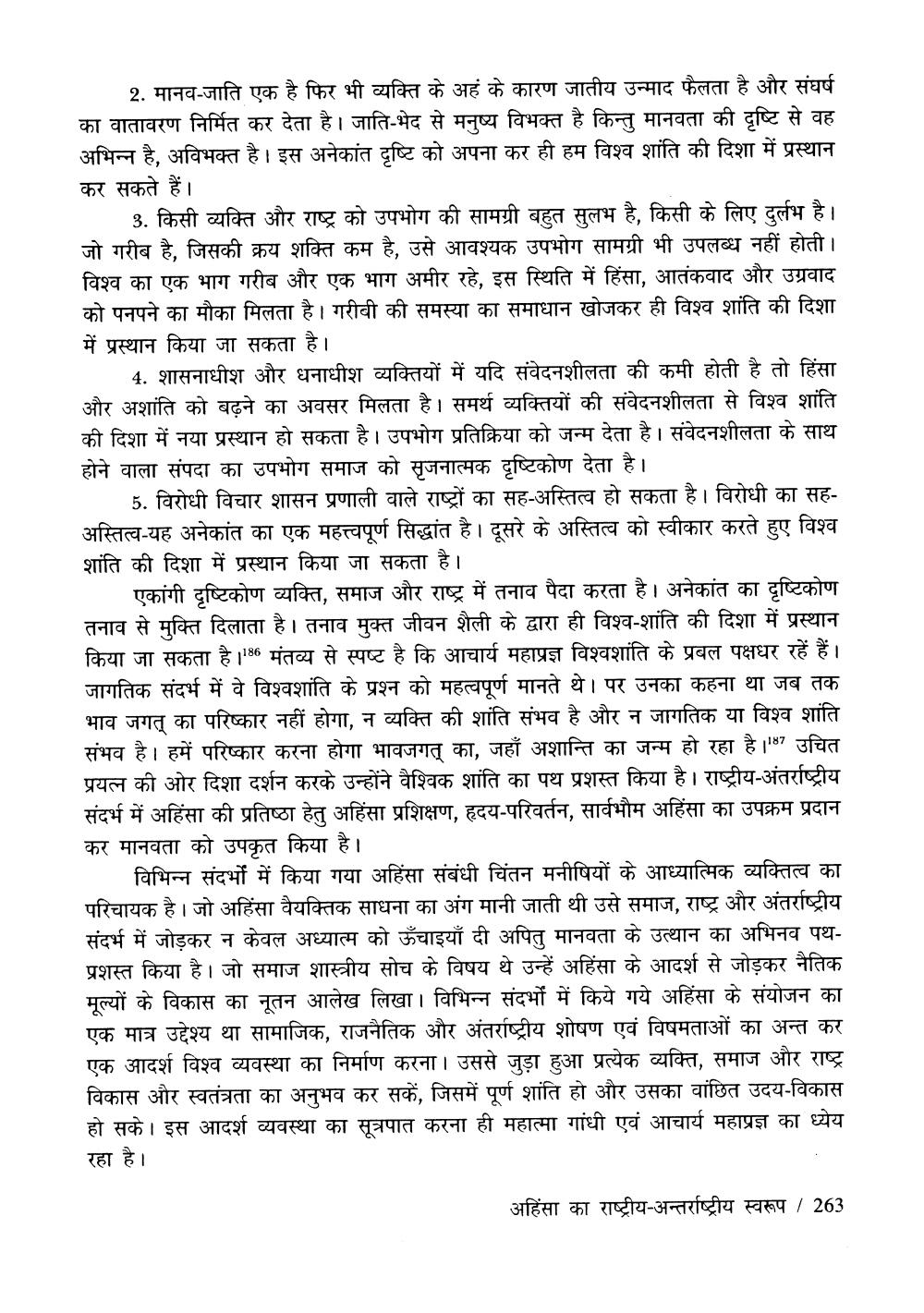________________
2. मानव-जाति एक है फिर भी व्यक्ति के अहं के कारण जातीय उन्माद फैलता है और संघर्ष का वातावरण निर्मित कर देता है। जाति-भेद से मनुष्य विभक्त है किन्तु मानवता की दृष्टि से वह अभिन्न है, अविभक्त है। इस अनेकांत दृष्टि को अपना कर ही हम विश्व शांति की दिशा में प्रस्थान कर सकते हैं। ___3. किसी व्यक्ति और राष्ट्र को उपभोग की सामग्री बहुत सुलभ है, किसी के लिए दुर्लभ है। जो गरीब है, जिसकी क्रय शक्ति कम है, उसे आवश्यक उपभोग सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती। विश्व का एक भाग गरीब और एक भाग अमीर रहे, इस स्थिति में हिंसा, आतंकवाद और उग्रवाद को पनपने का मौका मिलता है। गरीबी की समस्या का समाधान खोजकर ही विश्व शांति की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है।
4. शासनाधीश और धनाधीश व्यक्तियों में यदि संवेदनशीलता की कमी होती है तो हिंसा और अशांति को बढ़ने का अवसर मिलता है। समर्थ व्यक्तियों की संवेदनशीलता से विश्व शांति की दिशा में नया प्रस्थान हो सकता है। उपभोग प्रतिक्रिया को जन्म देता है। संवेदनशीलता के साथ होने वाला संपदा का उपभोग समाज को सृजनात्मक दृष्टिकोण देता है।
5. विरोधी विचार शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों का सह-अस्तित्व हो सकता है। विरोधी का सहअस्तित्व-यह अनेकांत का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए विश्व शांति की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है।
एकांगी दृष्टिकोण व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में तनाव पैदा करता है। अनेकांत का दृष्टिकोण तनाव से मुक्ति दिलाता है। तनाव मुक्त जीवन शैली के द्वारा ही विश्व-शांति की दिशा में प्रस्थान किया जा सकता है।186 मंतव्य से स्पष्ट है कि आचार्य महाप्रज्ञ विश्वशांति के प्रबल पक्षधर रहें हैं। जागतिक संदर्भ में वे विश्वशांति के प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते थे। पर उनका कहना था जब तक भाव जगत् का परिष्कार नहीं होगा, न व्यक्ति की शांति संभव है और न जागतिक या विश्व शांति संभव है। हमें परिष्कार करना होगा भावजगत् का, जहाँ अशान्ति का जन्म हो रहा है। 87 उचित प्रयत्न की ओर दिशा दर्शन करके उन्होंने वैश्विक शांति का पथ प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अहिंसा की प्रतिष्ठा हेतु अहिंसा प्रशिक्षण, हृदय-परिवर्तन, सार्वभौम अहिंसा का उपक्रम प्रदान कर मानवता को उपकृत किया है।
विभिन्न संदर्भो में किया गया अहिंसा संबंधी चिंतन मनीषियों के आध्यात्मिक व्यक्तित्व का परिचायक है। जो अहिंसा वैयक्तिक साधना का अंग मानी जाती थी उसे समाज. राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जोड़कर न केवल अध्यात्म को ऊँचाइयाँ दी अपितु मानवता के उत्थान का अभिनव पथप्रशस्त किया है। जो समाज शास्त्रीय सोच के विषय थे उन्हें अहिंसा के आदर्श से जोड़कर नैतिक मूल्यों के विकास का नूतन आलेख लिखा। विभिन्न संदर्भो में किये गये अहिंसा के संयोजन का एक मात्र उद्देश्य था सामाजिक, राजनैतिक और अंतर्राष्ट्रीय शोषण एवं विषमताओं का अन्त कर एक आदर्श विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र विकास और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, जिसमें पूर्ण शांति हो और उसका वांछित उदय-विकास हो सके। इस आदर्श व्यवस्था का सूत्रपात करना ही महात्मा गांधी एवं आचार्य महाप्रज्ञ का ध्येय रहा है।
अहिंसा का राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप / 263