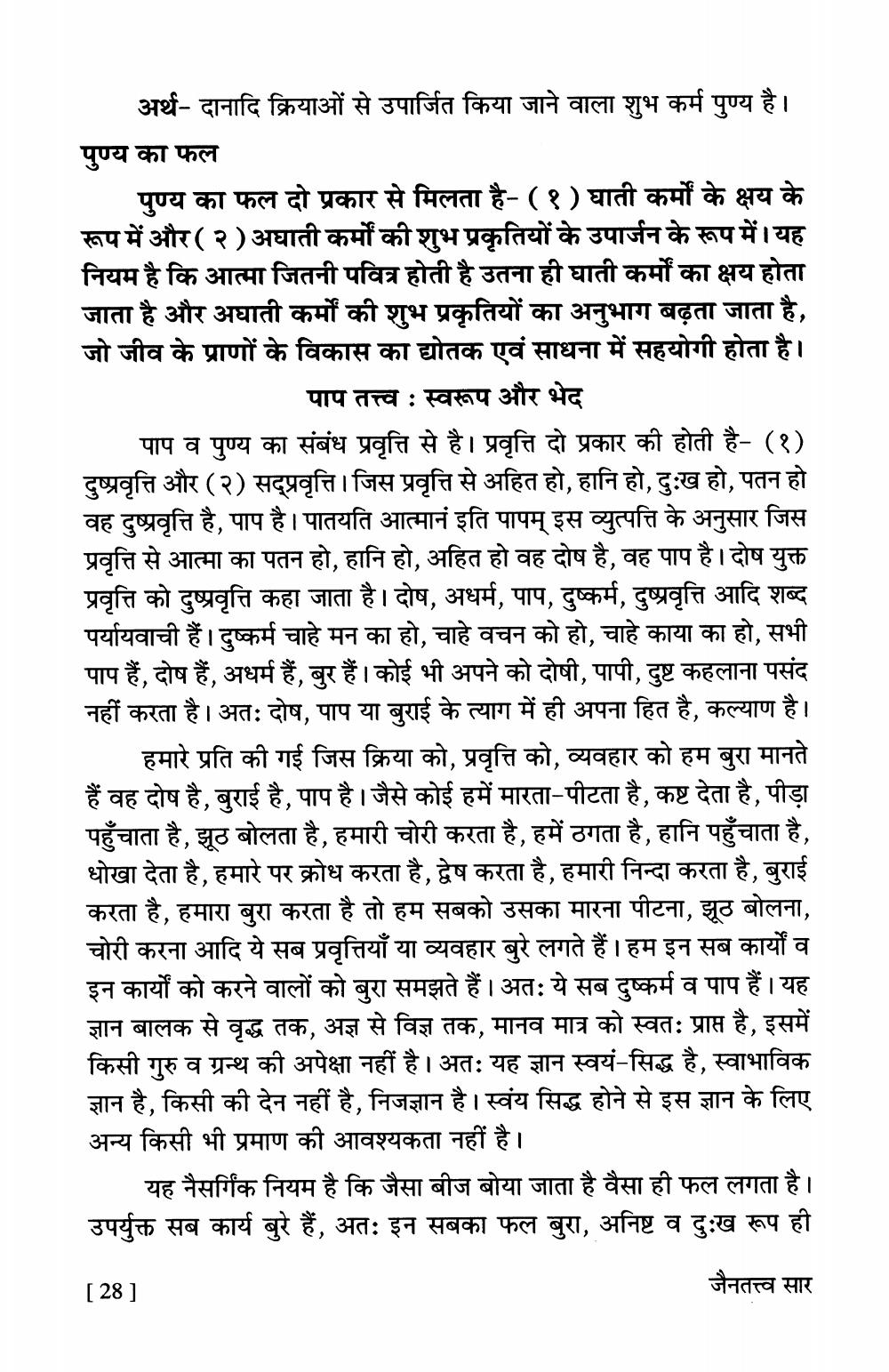________________
अर्थ- दानादि क्रियाओं से उपार्जित किया जाने वाला शुभ कर्म पुण्य है। पुण्य का फल
पुण्य का फल दो प्रकार से मिलता है- (१) घाती कर्मों के क्षय के रूप में और (२) अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों के उपार्जन के रूप में। यह नियम है कि आत्मा जितनी पवित्र होती है उतना ही घाती कर्मों का क्षय होता जाता है और अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है, जो जीव के प्राणों के विकास का द्योतक एवं साधना में सहयोगी होता है।
___ पाप तत्त्व : स्वरूप और भेद पाप व पुण्य का संबंध प्रवृत्ति से है। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है- (१) दुष्प्रवृत्ति और (२) सद्प्रवृत्ति । जिस प्रवृत्ति से अहित हो, हानि हो, दुःख हो, पतन हो वह दुष्प्रवृत्ति है, पाप है। पातयति आत्मानं इति पापम् इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो, हानि हो, अहित हो वह दोष है, वह पाप है। दोष युक्त प्रवृत्ति को दुष्प्रवृत्ति कहा जाता है। दोष, अधर्म, पाप, दुष्कर्म, दुष्प्रवृत्ति आदि शब्द पर्यायवाची हैं। दुष्कर्म चाहे मन का हो, चाहे वचन को हो, चाहे काया का हो, सभी पाप हैं, दोष हैं, अधर्म हैं, बुर हैं। कोई भी अपने को दोषी, पापी, दुष्ट कहलाना पसंद नहीं करता है। अतः दोष, पाप या बुराई के त्याग में ही अपना हित है, कल्याण है।
हमारे प्रति की गई जिस क्रिया को, प्रवृत्ति को, व्यवहार को हम बुरा मानते हैं वह दोष है, बुराई है, पाप है। जैसे कोई हमें मारता-पीटता है, कष्ट देता है, पीड़ा पहुँचाता है, झूठ बोलता है, हमारी चोरी करता है, हमें ठगता है, हानि पहुंचाता है, धोखा देता है, हमारे पर क्रोध करता है, द्वेष करता है, हमारी निन्दा करता है, बुराई करता है, हमारा बुरा करता है तो हम सबको उसका मारना पीटना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि ये सब प्रवृत्तियाँ या व्यवहार बुरे लगते हैं। हम इन सब कार्यों व इन कार्यों को करने वालों को बुरा समझते हैं। अतः ये सब दुष्कर्म व पाप हैं। यह ज्ञान बालक से वृद्ध तक, अज्ञ से विज्ञ तक, मानव मात्र को स्वतः प्राप्त है, इसमें किसी गुरु व ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं है। अतः यह ज्ञान स्वयं-सिद्ध है, स्वाभाविक ज्ञान है, किसी की देन नहीं है, निजज्ञान है। स्वंय सिद्ध होने से इस ज्ञान के लिए अन्य किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
यह नैसर्गिक नियम है कि जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल लगता है। उपर्युक्त सब कार्य बुरे हैं, अतः इन सबका फल बुरा, अनिष्ट व दुःख रूप ही
[28]
जैनतत्त्व सार