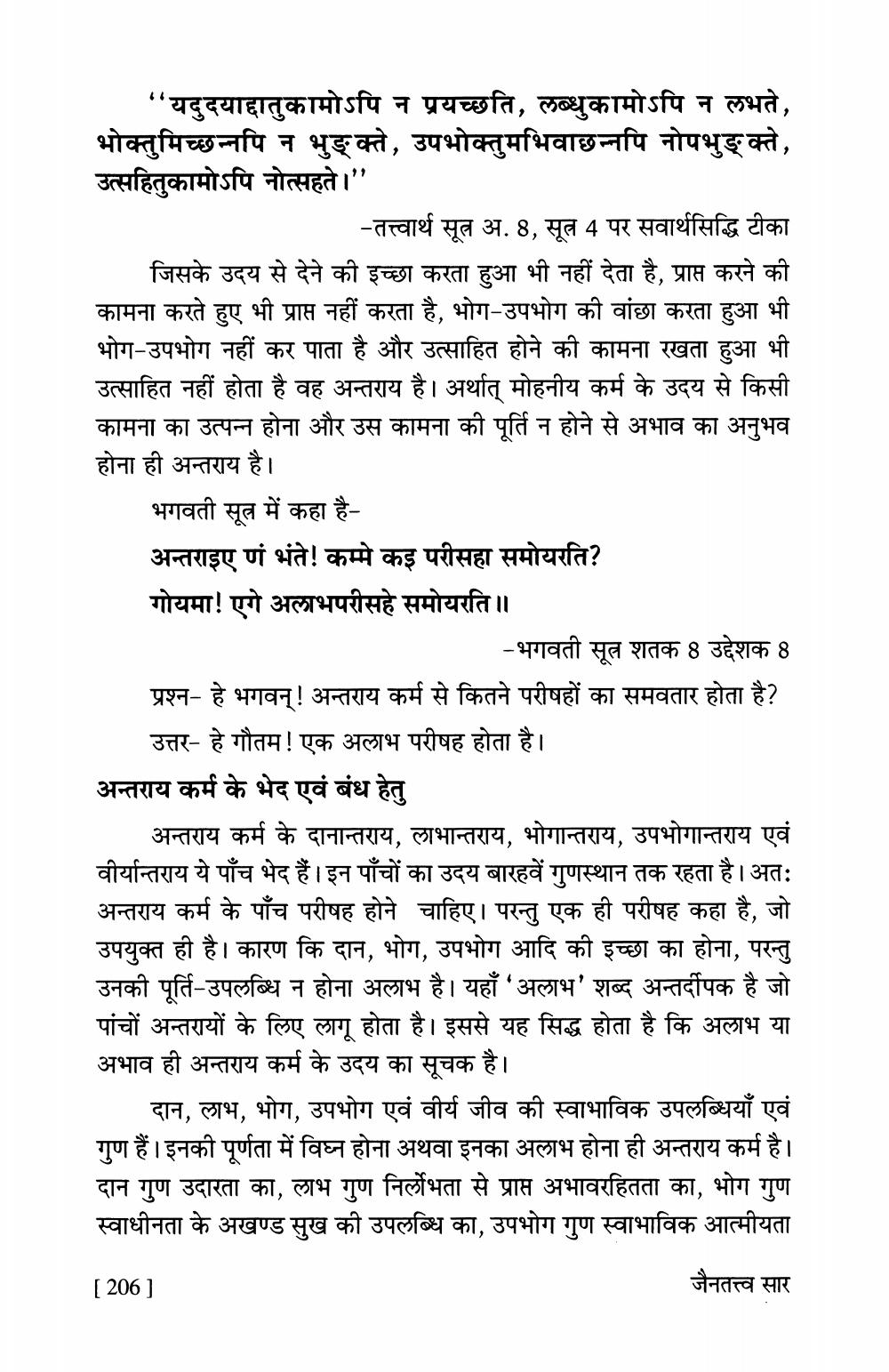________________
"यदुदयादातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि न लभते, भोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते, उपभोक्तुमभिवाछन्नपि नोपभुङ्क्ते, उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते।"
-तत्त्वार्थ सूत्र अ. 8, सूत्र 4 पर सवार्थसिद्धि टीका जिसके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, प्राप्त करने की कामना करते हुए भी प्राप्त नहीं करता है, भोग-उपभोग की वांछा करता हुआ भी भोग-उपभोग नहीं कर पाता है और उत्साहित होने की कामना रखता हुआ भी उत्साहित नहीं होता है वह अन्तराय है। अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय से किसी कामना का उत्पन्न होना और उस कामना की पूर्ति न होने से अभाव का अनुभव होना ही अन्तराय है।
भगवती सूत्र में कहा हैअन्तराइए णं भंते! कम्मे कइ परीसहा समोयरति? गोयमा! एगे अलाभपरीसहे समोयरति॥
--भगवती सूत्र शतक 8 उद्देशक 8 प्रश्न- हे भगवन्! अन्तराय कर्म से कितने परीषहों का समवतार होता है?
उत्तर- हे गौतम! एक अलाभ परीषह होता है। अन्तराय कर्म के भेद एवं बंध हेतु
अन्तराय कर्म के दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय एवं वीर्यान्तराय ये पाँच भेद हैं। इन पाँचों का उदय बारहवें गुणस्थान तक रहता है। अतः अन्तराय कर्म के पाँच परीषह होने चाहिए। परन्तु एक ही परीषह कहा है, जो उपयुक्त ही है। कारण कि दान, भोग, उपभोग आदि की इच्छा का होना, परन्तु उनकी पूर्ति-उपलब्धि न होना अलाभ है। यहाँ 'अलाभ' शब्द अन्तर्दीपक है जो पांचों अन्तरायों के लिए लागू होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अलाभ या अभाव ही अन्तराय कर्म के उदय का सूचक है।
दान, लाभ, भोग, उपभोग एवं वीर्य जीव की स्वाभाविक उपलब्धियाँ एवं गुण हैं। इनकी पूर्णता में विघ्न होना अथवा इनका अलाभ होना ही अन्तराय कर्म है। दान गुण उदारता का, लाभ गुण निर्लोभता से प्राप्त अभावरहितता का, भोग गुण स्वाधीनता के अखण्ड सुख की उपलब्धि का, उपभोग गुण स्वाभाविक आत्मीयता [ 206]
जैनतत्त्व सार