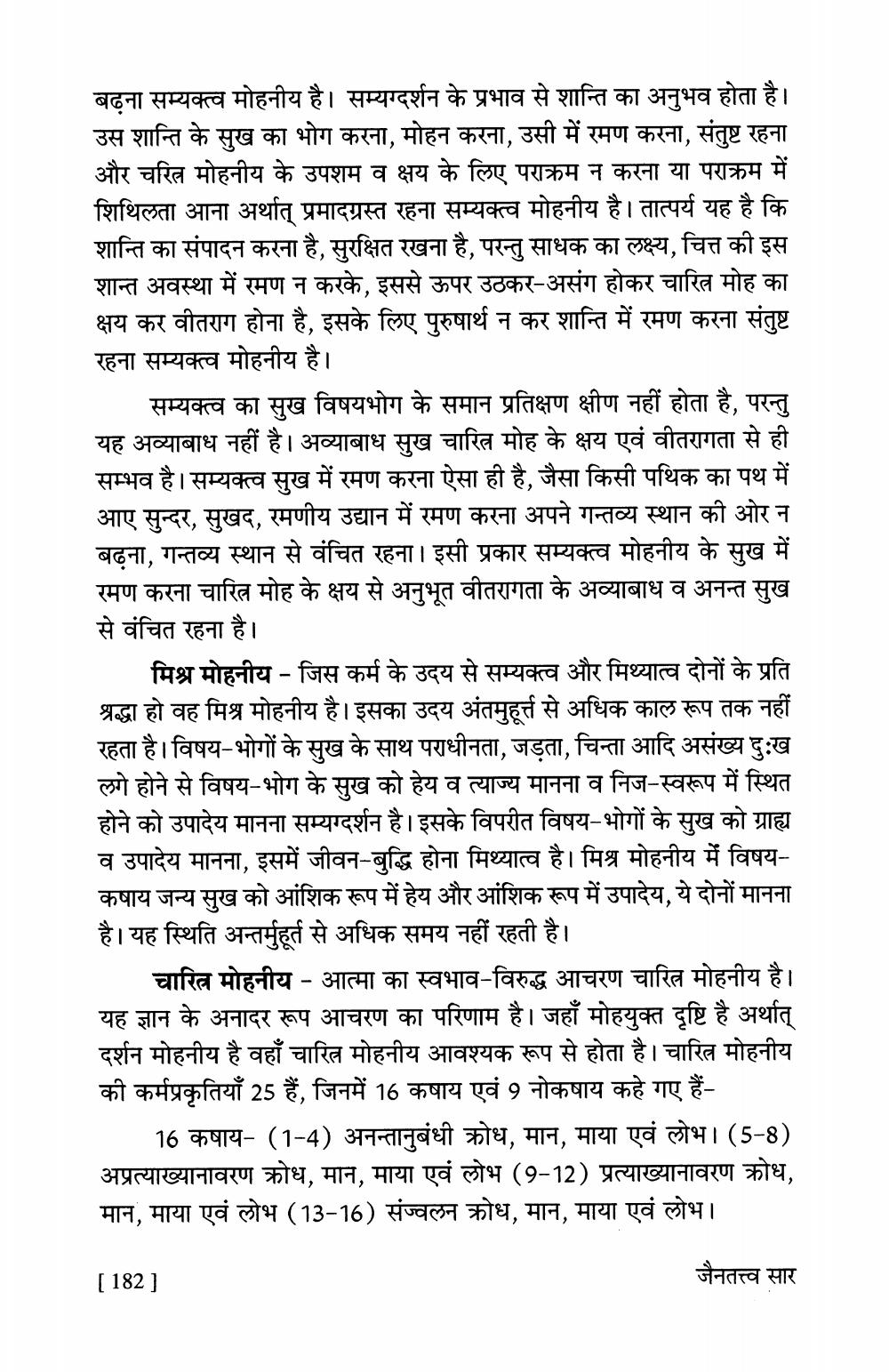________________
बढ़ना सम्यक्त्व मोहनीय है। सम्यग्दर्शन के प्रभाव से शान्ति का अनुभव होता है। उस शान्ति के सुख का भोग करना, मोहन करना, उसी में रमण करना, संतुष्ट रहना
और चरित्र मोहनीय के उपशम व क्षय के लिए पराक्रम न करना या पराक्रम में शिथिलता आना अर्थात् प्रमादग्रस्त रहना सम्यक्त्व मोहनीय है। तात्पर्य यह है कि शान्ति का संपादन करना है, सुरक्षित रखना है, परन्तु साधक का लक्ष्य, चित्त की इस शान्त अवस्था में रमण न करके, इससे ऊपर उठकर-असंग होकर चारित्र मोह का क्षय कर वीतराग होना है, इसके लिए पुरुषार्थ न कर शान्ति में रमण करना संतुष्ट रहना सम्यक्त्व मोहनीय है।
सम्यक्त्व का सुख विषयभोग के समान प्रतिक्षण क्षीण नहीं होता है, परन्तु यह अव्याबाध नहीं है। अव्याबाध सुख चारित्र मोह के क्षय एवं वीतरागता से ही सम्भव है। सम्यक्त्व सुख में रमण करना ऐसा ही है, जैसा किसी पथिक का पथ में आए सुन्दर, सुखद, रमणीय उद्यान में रमण करना अपने गन्तव्य स्थान की ओर न बढ़ना, गन्तव्य स्थान से वंचित रहना। इसी प्रकार सम्यक्त्व मोहनीय के सुख में रमण करना चारित्र मोह के क्षय से अनुभूत वीतरागता के अव्याबाध व अनन्त सुख से वंचित रहना है।
मिश्र मोहनीय - जिस कर्म के उदय से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के प्रति श्रद्धा हो वह मिश्र मोहनीय है। इसका उदय अंतमुहूर्त से अधिक काल रूप तक नहीं रहता है। विषय-भोगों के सुख के साथ पराधीनता, जड़ता, चिन्ता आदि असंख्य दुःख लगे होने से विषय-भोग के सुख को हेय व त्याज्य मानना व निज-स्वरूप में स्थित होने को उपादेय मानना सम्यग्दर्शन है। इसके विपरीत विषय-भोगों के सुख को ग्राह्य व उपादेय मानना, इसमें जीवन-बुद्धि होना मिथ्यात्व है। मिश्र मोहनीय में विषयकषाय जन्य सुख को आंशिक रूप में हेय और आंशिक रूप में उपादेय, ये दोनों मानना है। यह स्थिति अन्तर्मुहूर्त से अधिक समय नहीं रहती है।
चारित्र मोहनीय - आत्मा का स्वभाव-विरुद्ध आचरण चारित्र मोहनीय है। यह ज्ञान के अनादर रूप आचरण का परिणाम है। जहाँ मोहयुक्त दृष्टि है अर्थात् दर्शन मोहनीय है वहाँ चारित्र मोहनीय आवश्यक रूप से होता है। चारित्र मोहनीय की कर्मप्रकृतियाँ 25 हैं, जिनमें 16 कषाय एवं 9 नोकषाय कहे गए हैं
16 कषाय- (1-4) अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया एवं लोभ। (5-8) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया एवं लोभ (9-12) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया एवं लोभ (13-16) संज्वलन क्रोध, मान, माया एवं लोभ।
[182]
जैनतत्त्व सार