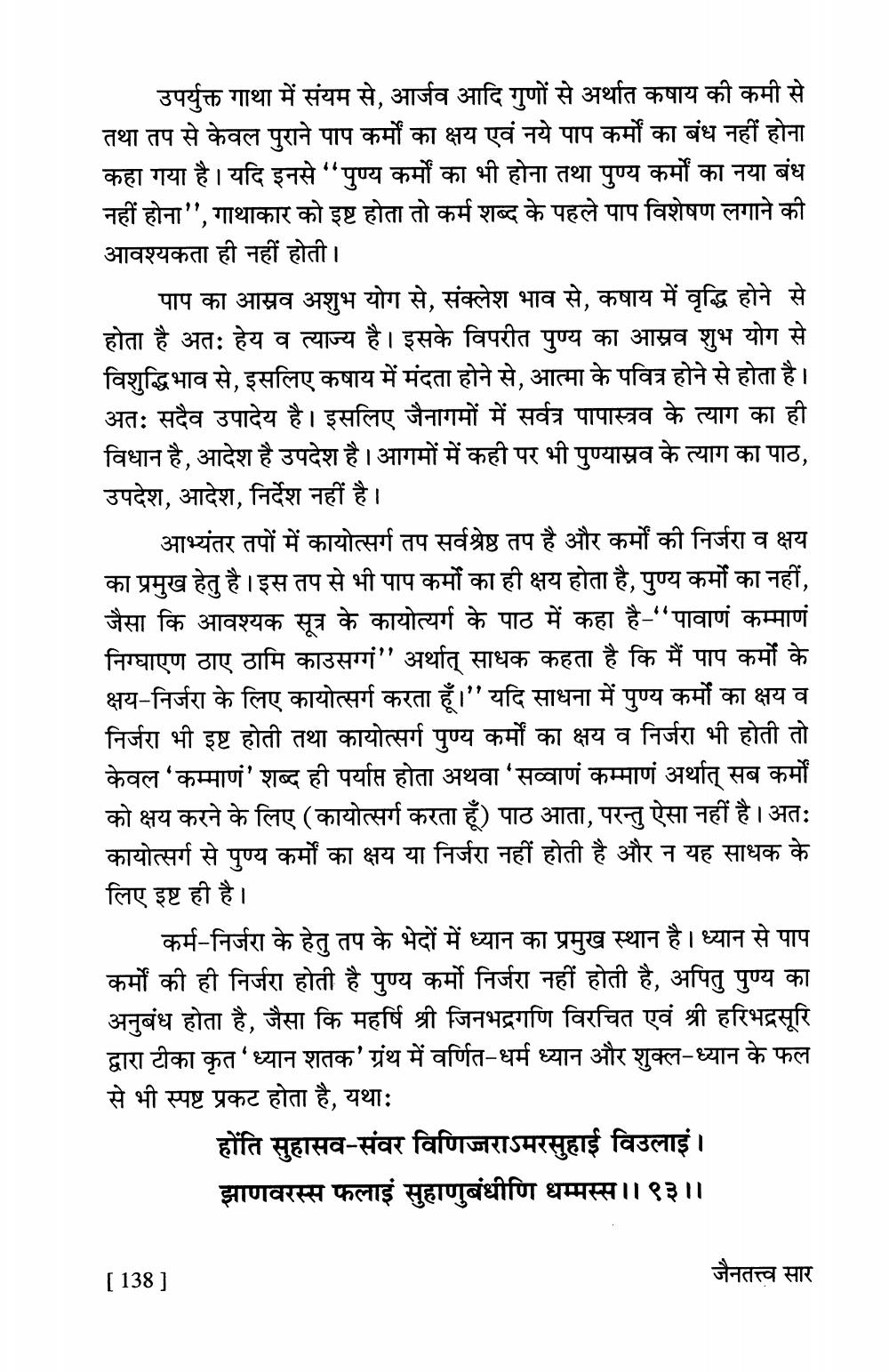________________
उपर्युक्त गाथा में संयम से, आर्जव आदि गुणों से अर्थात कषाय की कमी से तथा तप से केवल पुराने पाप कर्मों का क्षय एवं नये पाप कर्मों का बंध नहीं होना कहा गया है। यदि इनसे "पुण्य कर्मों का भी होना तथा पुण्य कर्मों का नया बंध नहीं होना", गाथाकार को इष्ट होता तो कर्म शब्द के पहले पाप विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती।
पाप का आस्रव अशुभ योग से, संक्लेश भाव से, कषाय में वृद्धि होने से होता है अतः हेय व त्याज्य है। इसके विपरीत पुण्य का आस्रव शुभ योग से विशुद्धिभाव से, इसलिए कषाय में मंदता होने से, आत्मा के पवित्र होने से होता है। अतः सदैव उपादेय है। इसलिए जैनागमों में सर्वत्र पापास्त्रव के त्याग का ही विधान है, आदेश है उपदेश है। आगमों में कही पर भी पुण्यास्रव के त्याग का पाठ, उपदेश, आदेश, निर्देश नहीं है।
आभ्यंतर तपों में कायोत्सर्ग तप सर्वश्रेष्ठ तप है और कर्मों की निर्जरा व क्षय का प्रमुख हेतु है। इस तप से भी पाप कर्मों का ही क्षय होता है, पुण्य कर्मों का नहीं, जैसा कि आवश्यक सूत्र के कायोत्यर्ग के पाठ में कहा है-"पावाणं कम्माणं निग्घाएण ठाए ठामि काउसग्गं" अर्थात् साधक कहता है कि मैं पाप कर्मों के क्षय-निर्जरा के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ।" यदि साधना में पुण्य कर्मों का क्षय व निर्जरा भी इष्ट होती तथा कायोत्सर्ग पुण्य कर्मों का क्षय व निर्जरा भी होती तो केवल 'कम्माणं' शब्द ही पर्याप्त होता अथवा 'सव्वाणं कम्माणं अर्थात् सब कर्मों को क्षय करने के लिए (कायोत्सर्ग करता हूँ) पाठ आता, परन्तु ऐसा नहीं है। अतः कायोत्सर्ग से पुण्य कर्मों का क्षय या निर्जरा नहीं होती है और न यह साधक के लिए इष्ट ही है।
___ कर्म-निर्जरा के हेतु तप के भेदों में ध्यान का प्रमुख स्थान है। ध्यान से पाप कर्मों की ही निर्जरा होती है पुण्य कर्मो निर्जरा नहीं होती है, अपितु पुण्य का अनुबंध होता है, जैसा कि महर्षि श्री जिनभद्रगणि विरचित एवं श्री हरिभद्रसूरि द्वारा टीका कृत 'ध्यान शतक' ग्रंथ में वर्णित-धर्म ध्यान और शुक्ल-ध्यान के फल से भी स्पष्ट प्रकट होता है, यथाः
होंति सुहासव-संवर विणिजराऽमरसुहाई विउलाई। झाणवरस्स फलाइं सुहाणुबंधीणि धम्मस्स।। ९३॥
[138]
जैनतत्त्व सार