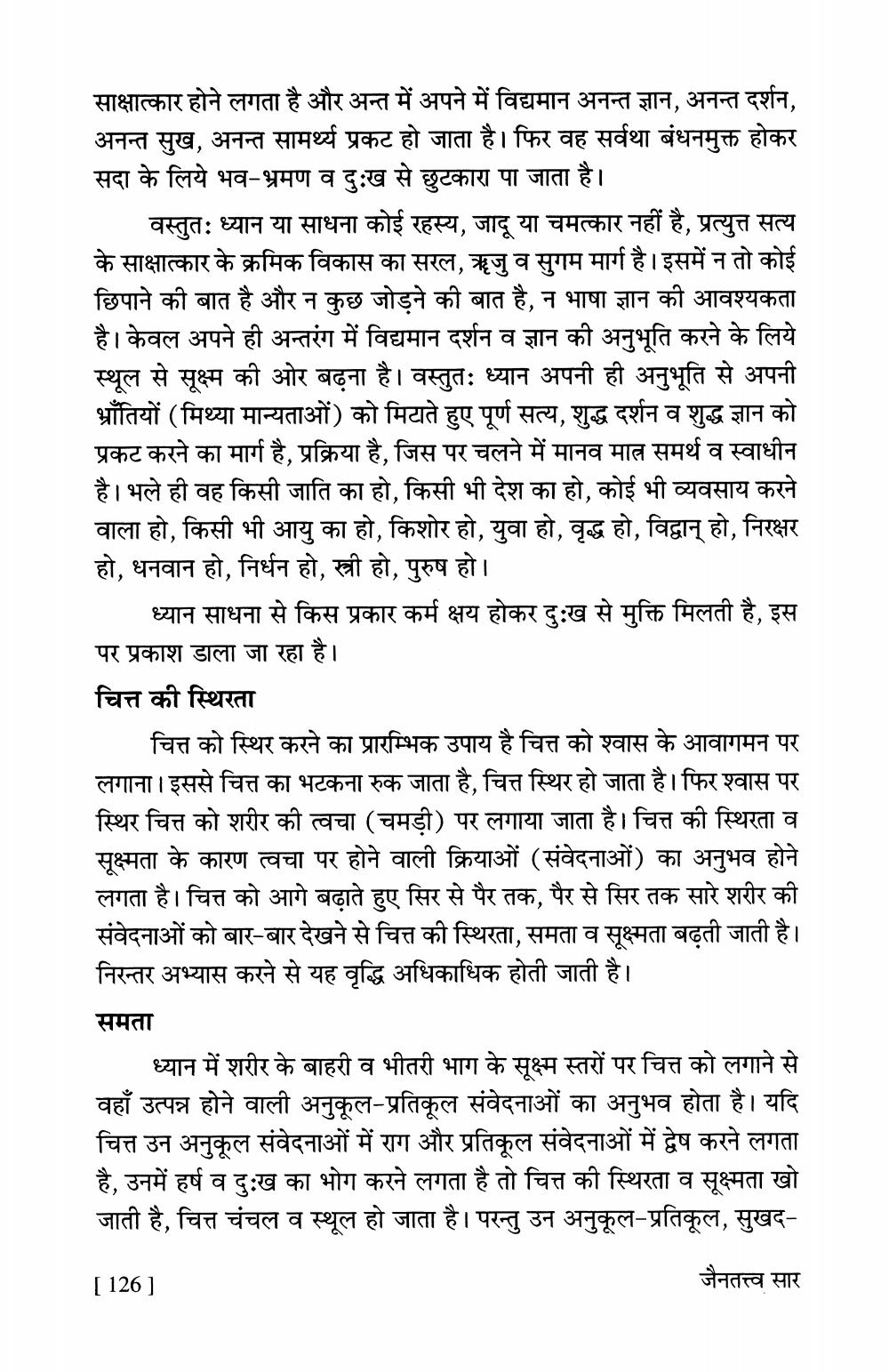________________
साक्षात्कार होने लगता है और अन्त में अपने में विद्यमान अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त सामर्थ्य प्रकट हो जाता है। फिर वह सर्वथा बंधनमुक्त होकर सदा के लिये भव-भ्रमण व दु:ख से छुटकारा पा जाता है।
वस्तुतः ध्यान या साधना कोई रहस्य, जादू या चमत्कार नहीं है, प्रत्युत्त सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक विकास का सरल, ऋजु व सुगम मार्ग है। इसमें न तो कोई छिपाने की बात है और न कुछ जोड़ने की बात है, न भाषा ज्ञान की आवश्यकता है। केवल अपने ही अन्तरंग में विद्यमान दर्शन व ज्ञान की अनुभूति करने के लिये स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना है। वस्तुतः ध्यान अपनी ही अनुभूति से अपनी भ्राँतियों (मिथ्या मान्यताओं) को मिटाते हुए पूर्ण सत्य, शुद्ध दर्शन व शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने का मार्ग है, प्रक्रिया है, जिस पर चलने में मानव मात्र समर्थ व स्वाधीन है। भले ही वह किसी जाति का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी व्यवसाय करने वाला हो, किसी भी आयु का हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, विद्वान् हो, निरक्षर हो, धनवान हो, निर्धन हो, स्त्री हो, पुरुष हो।
ध्यान साधना से किस प्रकार कर्म क्षय होकर दुःख से मुक्ति मिलती है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। चित्त की स्थिरता
चित्त को स्थिर करने का प्रारम्भिक उपाय है चित्त को श्वास के आवागमन पर लगाना। इससे चित्त का भटकना रुक जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। फिर श्वास पर स्थिर चित्त को शरीर की त्वचा (चमड़ी) पर लगाया जाता है। चित्त की स्थिरता व सूक्ष्मता के कारण त्वचा पर होने वाली क्रियाओं (संवेदनाओं) का अनुभव होने लगता है। चित्त को आगे बढ़ाते हुए सिर से पैर तक, पैर से सिर तक सारे शरीर की संवेदनाओं को बार-बार देखने से चित्त की स्थिरता, समता व सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। निरन्तर अभ्यास करने से यह वृद्धि अधिकाधिक होती जाती है। समता
ध्यान में शरीर के बाहरी व भीतरी भाग के सूक्ष्म स्तरों पर चित्त को लगाने से वहाँ उत्पन्न होने वाली अनुकूल-प्रतिकूल संवेदनाओं का अनुभव होता है। यदि चित्त उन अनुकूल संवेदनाओं में राग और प्रतिकूल संवेदनाओं में द्वेष करने लगता है, उनमें हर्ष व दुःख का भोग करने लगता है तो चित्त की स्थिरता व सूक्ष्मता खो जाती है, चित्त चंचल व स्थूल हो जाता है। परन्तु उन अनुकूल-प्रतिकूल, सुखद
[126]
जैनतत्त्व सार