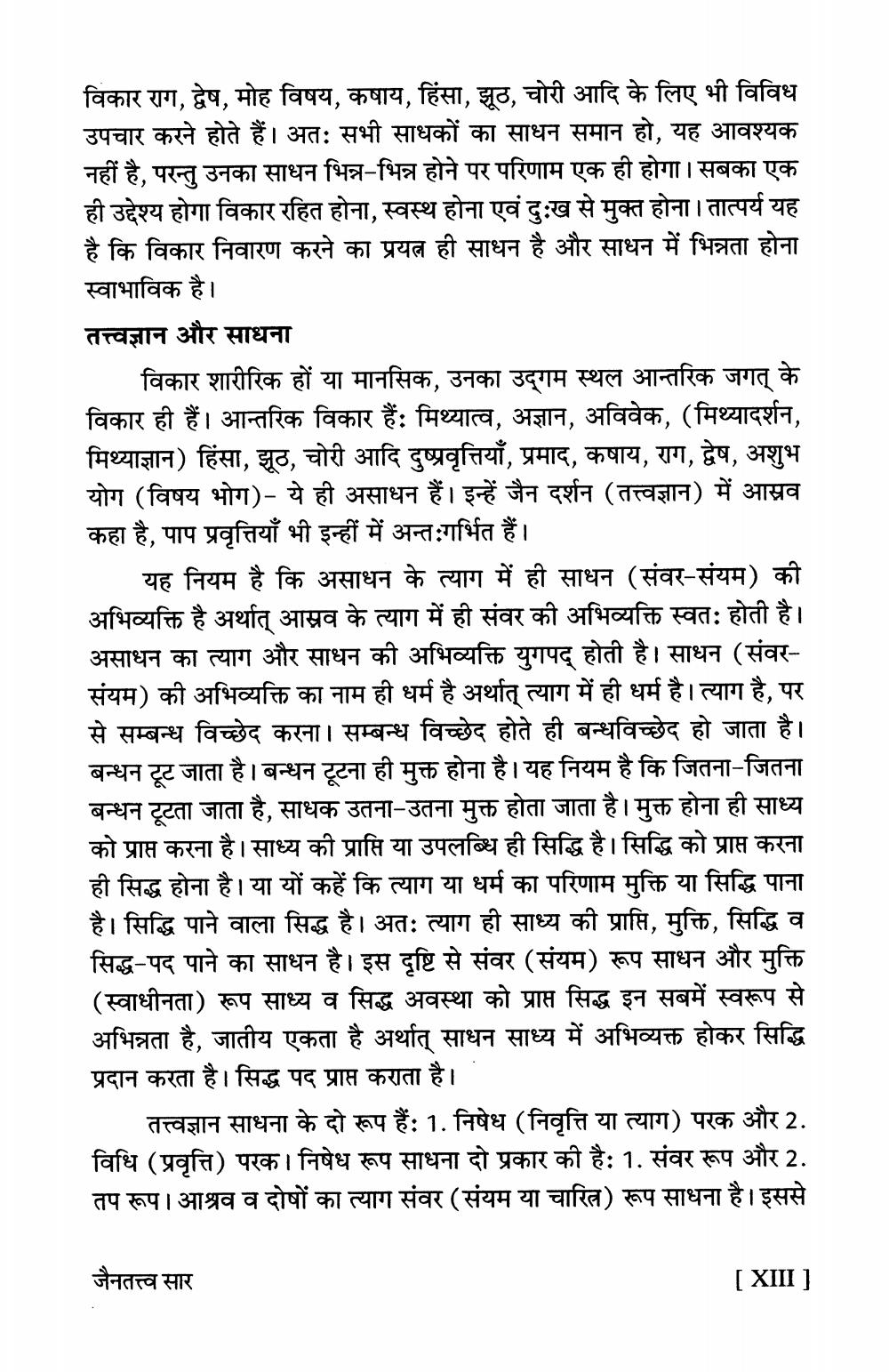________________
विकार राग, द्वेष, मोह विषय, कषाय, हिंसा, झूठ, चोरी आदि के लिए भी विविध उपचार करने होते हैं। अतः सभी साधकों का साधन समान हो, यह आवश्यक नहीं है, परन्तु उनका साधन भिन्न-भिन्न होने पर परिणाम एक ही होगा। सबका एक ही उद्देश्य होगा विकार रहित होना, स्वस्थ होना एवं दुःख से मुक्त होना। तात्पर्य यह है कि विकार निवारण करने का प्रयत्न ही साधन है और साधन में भिन्नता होना स्वाभाविक है। तत्त्वज्ञान और साधना
विकार शारीरिक हों या मानसिक, उनका उद्गम स्थल आन्तरिक जगत् के विकार ही हैं। आन्तरिक विकार हैं: मिथ्यात्व, अज्ञान, अविवेक, (मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान) हिंसा, झूठ, चोरी आदि दुष्प्रवृत्तियाँ, प्रमाद, कषाय, राग, द्वेष, अशुभ योग (विषय भोग)- ये ही असाधन हैं। इन्हें जैन दर्शन (तत्त्वज्ञान) में आस्रव कहा है, पाप प्रवृत्तियाँ भी इन्हीं में अन्तःगर्भित हैं। ___ यह नियम है कि असाधन के त्याग में ही साधन (संवर-संयम) की अभिव्यक्ति है अर्थात् आस्रव के त्याग में ही संवर की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। असाधन का त्याग और साधन की अभिव्यक्ति युगपद् होती है। साधन (संवरसंयम) की अभिव्यक्ति का नाम ही धर्म है अर्थात् त्याग में ही धर्म है। त्याग है, पर से सम्बन्ध विच्छेद करना। सम्बन्ध विच्छेद होते ही बन्धविच्छेद हो जाता है। बन्धन टूट जाता है। बन्धन टूटना ही मुक्त होना है। यह नियम है कि जितना-जितना बन्धन टूटता जाता है, साधक उतना-उतना मुक्त होता जाता है। मुक्त होना ही साध्य को प्राप्त करना है। साध्य की प्राप्ति या उपलब्धि ही सिद्धि है। सिद्धि को प्राप्त करना ही सिद्ध होना है। या यों कहें कि त्याग या धर्म का परिणाम मुक्ति या सिद्धि पाना है। सिद्धि पाने वाला सिद्ध है। अतः त्याग ही साध्य की प्राप्ति, मुक्ति, सिद्धि व सिद्ध-पद पाने का साधन है। इस दृष्टि से संवर (संयम) रूप साधन और मुक्ति (स्वाधीनता) रूप साध्य व सिद्ध अवस्था को प्राप्त सिद्ध इन सबमें स्वरूप से अभिन्नता है, जातीय एकता है अर्थात् साधन साध्य में अभिव्यक्त होकर सिद्धि प्रदान करता है। सिद्ध पद प्राप्त कराता है।
तत्त्वज्ञान साधना के दो रूप हैं: 1. निषेध (निवृत्ति या त्याग) परक और 2. विधि (प्रवृत्ति) परक। निषेध रूप साधना दो प्रकार की है: 1. संवर रूप और 2. तप रूप। आश्रव व दोषों का त्याग संवर (संयम या चारित्र) रूप साधना है। इससे
जैनतत्त्व सार
[XIII]