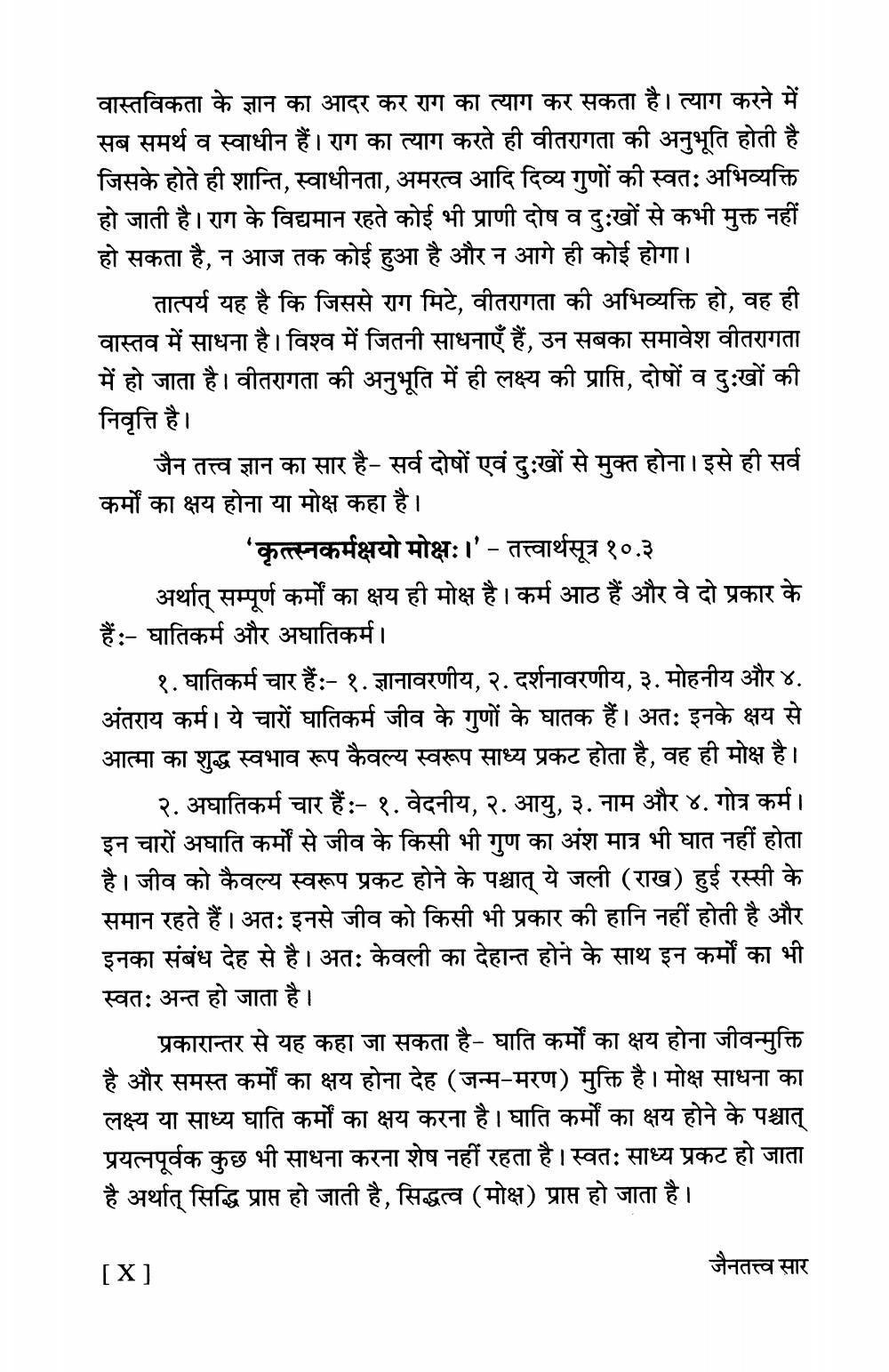________________
वास्तविकता के ज्ञान का आदर कर राग का त्याग कर सकता है। त्याग करने में सब समर्थ व स्वाधीन हैं। राग का त्याग करते ही वीतरागता की अनुभूति होती है जिसके होते ही शान्ति, स्वाधीनता, अमरत्व आदि दिव्य गुणों की स्वत: अभिव्यक्ति हो जाती है। राग के विद्यमान रहते कोई भी प्राणी दोष व दुःखों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, न आज तक कोई हुआ है और न आगे ही कोई होगा ।
तात्पर्य यह है कि जिससे राग मिटे, वीतरागता की अभिव्यक्ति हो, वह ही वास्तव में साधना है। विश्व में जितनी साधनाएँ हैं, उन सबका समावेश वीतरागता में हो जाता है। वीतरागता की अनुभूति में ही लक्ष्य की प्राप्ति, दोषों व दुःखों की निवृत्ति है ।
जैन तत्त्वज्ञान का सार है- सर्व दोषों एवं दुःखों से मुक्त होना । इसे ही सर्व कर्मों का क्षय होना या मोक्ष कहा है ।
'कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः । ' - तत्त्वार्थसूत्र १०.३
अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है। कर्म आठ हैं और वे दो प्रकार के हैं :- घातिकर्म और अघातिकर्म ।
१. घातिकर्म चार हैं:- १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. मोहनीय और ४. अंतराय कर्म। ये चारों घातिकर्म जीव के गुणों के घातक हैं । अतः इनके क्षय से आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप कैवल्य स्वरूप साध्य प्रकट होता है, वह ही मोक्ष है।
२. अघातिकर्म चार हैं :- १. वेदनीय, २. आयु, ३. नाम और ४. गोत्र कर्म । इन चारों अघाति कर्मों से जीव के किसी भी गुण का अंश मात्र भी घात नहीं होता है । जीव को कैवल्य स्वरूप प्रकट होने के पश्चात् ये जली (राख) हुई रस्सी के समान रहते हैं । अतः इनसे जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और इनका संबंध देह से है । अतः केवली का देहान्त होने के साथ इन कर्मों का भी स्वतः अन्त हो जाता है ।
प्रकारान्तर से यह कहा जा सकता है- घाति कर्मों का क्षय होना जीवन्मुक्ति है और समस्त कर्मों का क्षय होना देह (जन्म-मरण) मुक्ति है । मोक्ष साधना का लक्ष्य या साध्य घाति कर्मों का क्षय करना है। घाति कर्मों का क्षय होने के पश्चात् प्रयत्नपूर्वक कुछ भी साधना करना शेष नहीं रहता है । स्वतः साध्य प्रकट हो जाता अर्थात् सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धत्व (मोक्ष) प्राप्त हो जाता है I
[X]
जैतत्त्व सा