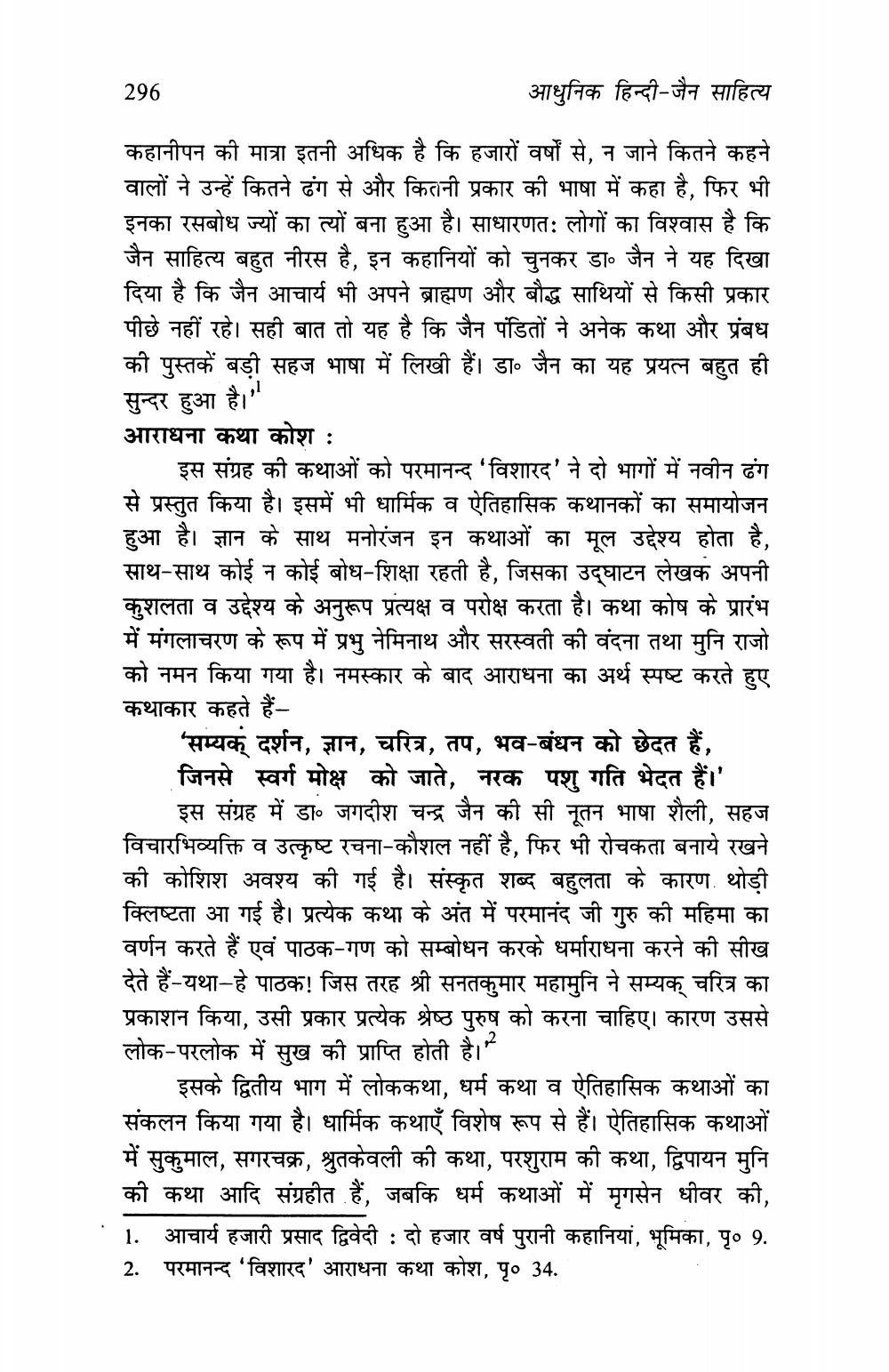________________
296
आधुनिक हिन्दी-जैन साहित्य
कहानीपन की मात्रा इतनी अधिक है कि हजारों वर्षों से, न जाने कितने कहने वालों ने उन्हें कितने ढंग से और कितनी प्रकार की भाषा में कहा है, फिर भी इनका रसबोध ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि जैन साहित्य बहुत नीरस है, इन कहानियों को चुनकर डा. जैन ने यह दिखा दिया है कि जैन आचार्य भी अपने ब्राह्मण और बौद्ध साथियों से किसी प्रकार पीछे नहीं रहे। सही बात तो यह है कि जैन पंडितों ने अनेक कथा और प्रबंध की पुस्तकें बड़ी सहज भाषा में लिखी हैं। डा. जैन का यह प्रयत्न बहुत ही सुन्दर हुआ है।" आराधना कथा कोश :
इस संग्रह की कथाओं को परमानन्द 'विशारद' ने दो भागों में नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें भी धार्मिक व ऐतिहासिक कथानकों का समायोजन हुआ है। ज्ञान के साथ मनोरंजन इन कथाओं का मूल उद्देश्य होता है, साथ-साथ कोई न कोई बोध-शिक्षा रहती है, जिसका उद्घाटन लेखक अपनी कुशलता व उद्देश्य के अनुरूप प्रत्यक्ष व परोक्ष करता है। कथा कोष के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में प्रभु नेमिनाथ और सरस्वती की वंदना तथा मुनि राजो को नमन किया गया है। नमस्कार के बाद आराधना का अर्थ स्पष्ट करते हुए कथाकार कहते हैं
'सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, भव-बंधन को छेदत हैं, जिनसे स्वर्ग मोक्ष को जाते, नरक पशु गति भेदत हैं।'
इस संग्रह में डा. जगदीश चन्द्र जैन की सी नूतन भाषा शैली, सहज विचारभिव्यक्ति व उत्कृष्ट रचना-कौशल नहीं है, फिर भी रोचकता बनाये रखने की कोशिश अवश्य की गई है। संस्कृत शब्द बहुलता के कारण. थोड़ी क्लिष्टता आ गई है। प्रत्येक कथा के अंत में परमानंद जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं एवं पाठक-गण को सम्बोधन करके धर्माराधना करने की सीख देते हैं-यथा-हे पाठक! जिस तरह श्री सनतकुमार महामुनि ने सम्यक् चरित्र का प्रकाशन किया, उसी प्रकार प्रत्येक श्रेष्ठ पुरुष को करना चाहिए। कारण उससे लोक-परलोक में सुख की प्राप्ति होती है।'
इसके द्वितीय भाग में लोककथा, धर्म कथा व ऐतिहासिक कथाओं का संकलन किया गया है। धार्मिक कथाएँ विशेष रूप से हैं। ऐतिहासिक कथाओं में सुकुमाल, सगरचक्र, श्रुतकेवली की कथा, परशुराम की कथा, द्विपायन मुनि
की कथा आदि संग्रहीत हैं, जबकि धर्म कथाओं में मृगसेन धीवर की, - 1. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : दो हजार वर्ष पुरानी कहानियां, भूमिका, पृ० 9.
2. परमानन्द 'विशारद' आराधना कथा कोश, पृ० 34.