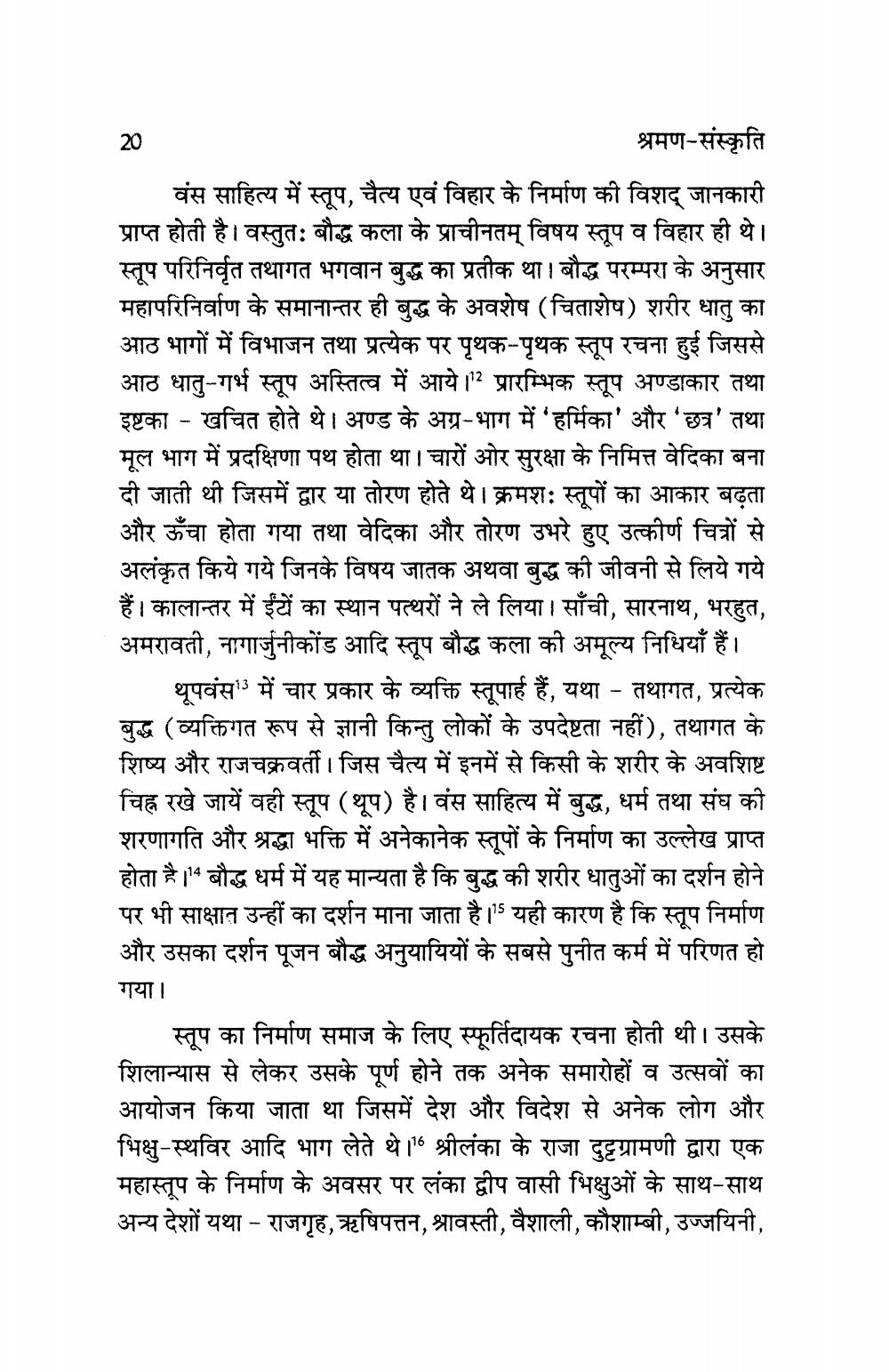________________
20
श्रमण-संस्कृति वंस साहित्य में स्तूप, चैत्य एवं विहार के निर्माण की विशद् जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः बौद्ध कला के प्राचीनतम् विषय स्तूप व विहार ही थे। स्तूप परिनिर्वृत तथागत भगवान बुद्ध का प्रतीक था। बौद्ध परम्परा के अनुसार महापरिनिर्वाण के समानान्तर ही बुद्ध के अवशेष (चिताशेष) शरीर धातु का आठ भागों में विभाजन तथा प्रत्येक पर पृथक-पृथक स्तूप रचना हुई जिससे आठ धातु-गर्भ स्तूप अस्तित्व में आये। प्रारम्भिक स्तूप अण्डाकार तथा इष्टका - खचित होते थे। अण्ड के अग्र-भाग में 'हर्मिका' और 'छत्र' तथा मूल भाग में प्रदक्षिणा पथ होता था। चारों ओर सुरक्षा के निमित्त वेदिका बना दी जाती थी जिसमें द्वार या तोरण होते थे। क्रमशः स्तूपों का आकार बढ़ता और ऊँचा होता गया तथा वेदिका और तोरण उभरे हुए उत्कीर्ण चित्रों से अलंकृत किये गये जिनके विषय जातक अथवा बुद्ध की जीवनी से लिये गये हैं। कालान्तर में ईंटों का स्थान पत्थरों ने ले लिया। साँची, सारनाथ, भरहुत, अमरावती, नागार्जुनीकोंड आदि स्तूप बौद्ध कला की अमूल्य निधियाँ हैं।
थूपवंस' में चार प्रकार के व्यक्ति स्तूपार्ह हैं, यथा - तथागत, प्रत्येक बुद्ध (व्यक्तिगत रूप से ज्ञानी किन्तु लोकों के उपदेष्टता नहीं), तथागत के शिष्य और राजचक्रवर्ती। जिस चैत्य में इनमें से किसी के शरीर के अवशिष्ट चिह्न रखे जायें वही स्तूप (थूप) है। वंस साहित्य में बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरणागति और श्रद्धा भक्ति में अनेकानेक स्तूपों के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। 4 बौद्ध धर्म में यह मान्यता है कि बुद्ध की शरीर धातुओं का दर्शन होने पर भी साक्षात उन्हीं का दर्शन माना जाता है। यही कारण है कि स्तूप निर्माण और उसका दर्शन पूजन बौद्ध अनुयायियों के सबसे पुनीत कर्म में परिणत हो
गया।
स्तूप का निर्माण समाज के लिए स्फूर्तिदायक रचना होती थी। उसके शिलान्यास से लेकर उसके पूर्ण होने तक अनेक समारोहों व उत्सवों का आयोजन किया जाता था जिसमें देश और विदेश से अनेक लोग और भिक्षु-स्थविर आदि भाग लेते थे। श्रीलंका के राजा दुट्टग्रामणी द्वारा एक महास्तूप के निर्माण के अवसर पर लंका द्वीप वासी भिक्षुओं के साथ-साथ अन्य देशों यथा - राजगृह, ऋषिपत्तन, श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जयिनी.