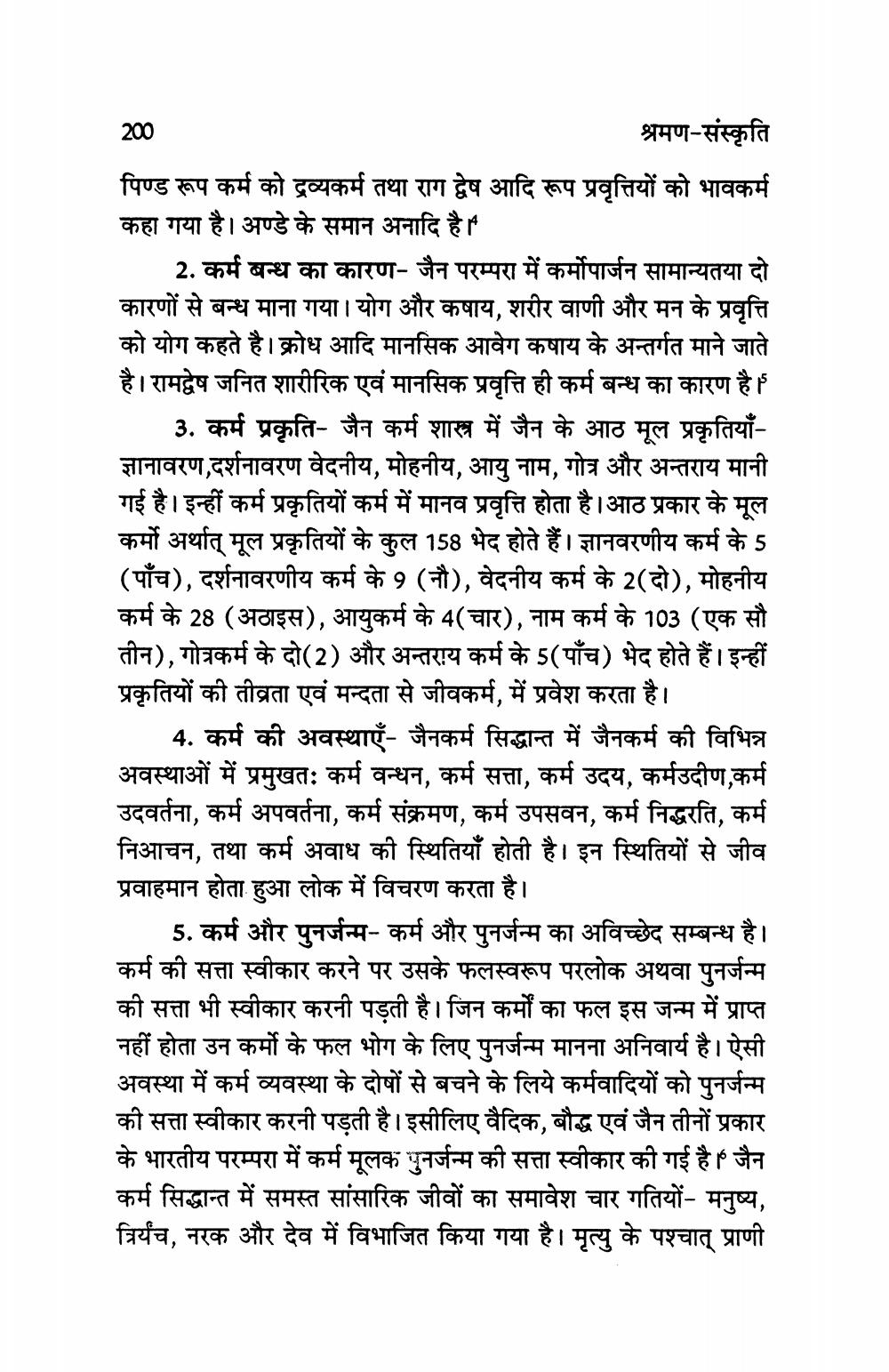________________
200
श्रमण-संस्कृति पिण्ड रूप कर्म को द्रव्यकर्म तथा राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्तियों को भावकर्म कहा गया है। अण्डे के समान अनादि है।
2. कर्म बन्ध का कारण- जैन परम्परा में कर्मोपार्जन सामान्यतया दो कारणों से बन्ध माना गया। योग और कषाय, शरीर वाणी और मन के प्रवृत्ति को योग कहते है। क्रोध आदि मानसिक आवेग कषाय के अन्तर्गत माने जाते है। रामद्वेष जनित शारीरिक एवं मानसिक प्रवृत्ति ही कर्म बन्ध का कारण है। ___3. कर्म प्रकृति- जैन कर्म शास्त्र में जैन के आठ मूल प्रकृतियाँज्ञानावरण,दर्शनावरण वेदनीय, मोहनीय, आयु नाम, गोत्र और अन्तराय मानी गई है। इन्हीं कर्म प्रकृतियों कर्म में मानव प्रवृत्ति होता है। आठ प्रकार के मूल कर्मो अर्थात् मूल प्रकृतियों के कुल 158 भेद होते हैं। ज्ञानवरणीय कर्म के 5 (पाँच), दर्शनावरणीय कर्म के 9 (नौ), वेदनीय कर्म के 2(दो), मोहनीय कर्म के 28 (अठाइस), आयुकर्म के 4(चार), नाम कर्म के 103 (एक सौ तीन), गोत्रकर्म के दो(2) और अन्तराय कर्म के 5(पाँच) भेद होते हैं। इन्हीं प्रकृतियों की तीव्रता एवं मन्दता से जीवकर्म, में प्रवेश करता है।
4. कर्म की अवस्थाएँ- जैनकर्म सिद्धान्त में जैनकर्म की विभिन्न अवस्थाओं में प्रमुखतः कर्म वन्धन, कर्म सत्ता, कर्म उदय, कर्मउदीण,कर्म उदवर्तना, कर्म अपवर्तना, कर्म संक्रमण, कर्म उपसवन, कर्म निद्धरति, कर्म निआचन, तथा कर्म अवाध की स्थितियाँ होती है। इन स्थितियों से जीव प्रवाहमान होता हुआ लोक में विचरण करता है।
5. कर्म और पुनर्जन्म- कर्म और पुनर्जन्म का अविच्छेद सम्बन्ध है। कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर उसके फलस्वरूप परलोक अथवा पुनर्जन्म की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त नहीं होता उन कर्मो के फल भोग के लिए पुनर्जन्म मानना अनिवार्य है। ऐसी अवस्था में कर्म व्यवस्था के दोषों से बचने के लिये कर्मवादियों को पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। इसीलिए वैदिक, बौद्ध एवं जैन तीनों प्रकार के भारतीय परम्परा में कर्म मूलक पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार की गई है। जैन कर्म सिद्धान्त में समस्त सांसारिक जीवों का समावेश चार गतियों- मनुष्य, त्रिर्यंच, नरक और देव में विभाजित किया गया है। मृत्यु के पश्चात् प्राणी