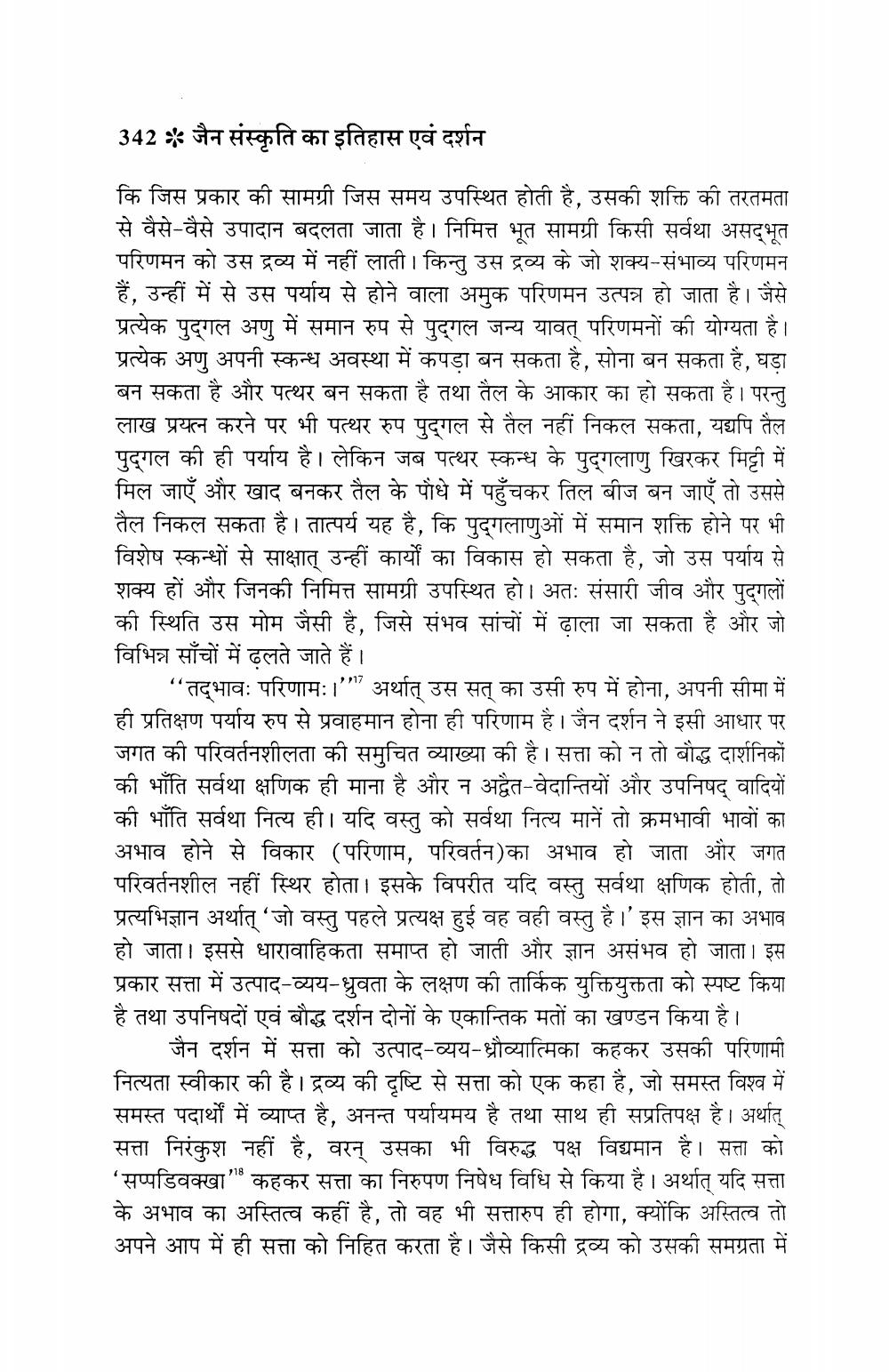________________
342 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
कि जिस प्रकार की सामग्री जिस समय उपस्थित होती है, उसकी शक्ति की तरतमता से वैसे-वैसे उपादान बदलता जाता है। निमित्त भूत सामग्री किसी सर्वथा असद्भूत परिणमन को उस द्रव्य में नहीं लाती। किन्तु उस द्रव्य के जो शक्य-संभाव्य परिणमन हैं, उन्हीं में से उस पर्याय से होने वाला अमुक परिणमन उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रत्येक पुद्गल अणु में समान रुप से पुद्गल जन्य यावत् परिणमनों की योग्यता है। प्रत्येक अणु अपनी स्कन्ध अवस्था में कपड़ा बन सकता है, सोना बन सकता है, घड़ा बन सकता है और पत्थर बन सकता है तथा तैल के आकार का हो सकता है। परन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी पत्थर रुप पुद्गल से तैल नहीं निकल सकता, यद्यपि तैल पुद्गल की ही पर्याय है। लेकिन जब पत्थर स्कन्ध के पुद्गलाणु खिरकर मिट्टी में मिल जाएँ और खाद बनकर तैल के पौधे में पहुँचकर तिल बीज बन जाएँ तो उससे तैल निकल सकता है। तात्पर्य यह है, कि पुद्गलाणुओं में समान शक्ति होने पर भी विशेष स्कन्धों से साक्षात् उन्हीं कार्यों का विकास हो सकता है, जो उस पर्याय से शक्य हों और जिनकी निमित्त सामग्री उपस्थित हो। अतः संसारी जीव और पुद्गलों की स्थिति उस मोम जैसी है, जिसे संभव सांचों में ढाला जा सकता है और जो विभिन्न साँचों में ढलते जाते हैं।
"तभावः परिणामः। अर्थात् उस सत् का उसी रुप में होना, अपनी सीमा में ही प्रतिक्षण पर्याय रुप से प्रवाहमान होना ही परिणाम है। जैन दर्शन ने इसी आधार पर जगत की परिवर्तनशीलता की समुचित व्याख्या की है। सत्ता को न तो बौद्ध दार्शनिकों की भाँति सर्वथा क्षणिक ही माना है और न अद्वैत-वेदान्तियों और उपनिषद् वादियों की भाँति सर्वथा नित्य ही। यदि वस्तु को सर्वथा नित्य मानें तो क्रमभावी भावों का अभाव होने से विकार (परिणाम, परिवर्तन)का अभाव हो जाता और जगत परिवर्तनशील नहीं स्थिर होता। इसके विपरीत यदि वस्तु सर्वथा क्षणिक होती, तो प्रत्यभिज्ञान अर्थात् ‘जो वस्तु पहले प्रत्यक्ष हुई वह वही वस्तु है।' इस ज्ञान का अभाव हो जाता। इससे धारावाहिकता समाप्त हो जाती और ज्ञान असंभव हो जाता। इस प्रकार सत्ता में उत्पाद-व्यय-ध्रुवता के लक्षण की तार्किक युक्तियुक्तता को स्पष्ट किया है तथा उपनिषदों एवं बौद्ध दर्शन दोनों के एकान्तिक मतों का खण्डन किया है।
जैन दर्शन में सत्ता को उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मिका कहकर उसकी परिणामी नित्यता स्वीकार की है। द्रव्य की दृष्टि से सत्ता को एक कहा है, जो समस्त विश्व में समस्त पदार्थों में व्याप्त है, अनन्त पर्यायमय है तथा साथ ही सप्रतिपक्ष है। अर्थात् सत्ता निरंकुश नहीं है, वरन् उसका भी विरुद्ध पक्ष विद्यमान है। सत्ता को "सप्पडिवक्खा" कहकर सत्ता का निरुपण निषेध विधि से किया है। अर्थात् यदि सत्ता के अभाव का अस्तित्व कहीं है, तो वह भी सत्तारुप ही होगा, क्योंकि अस्तित्व तो अपने आप में ही सत्ता को निहित करता है। जैसे किसी द्रव्य को उसकी समग्रता में