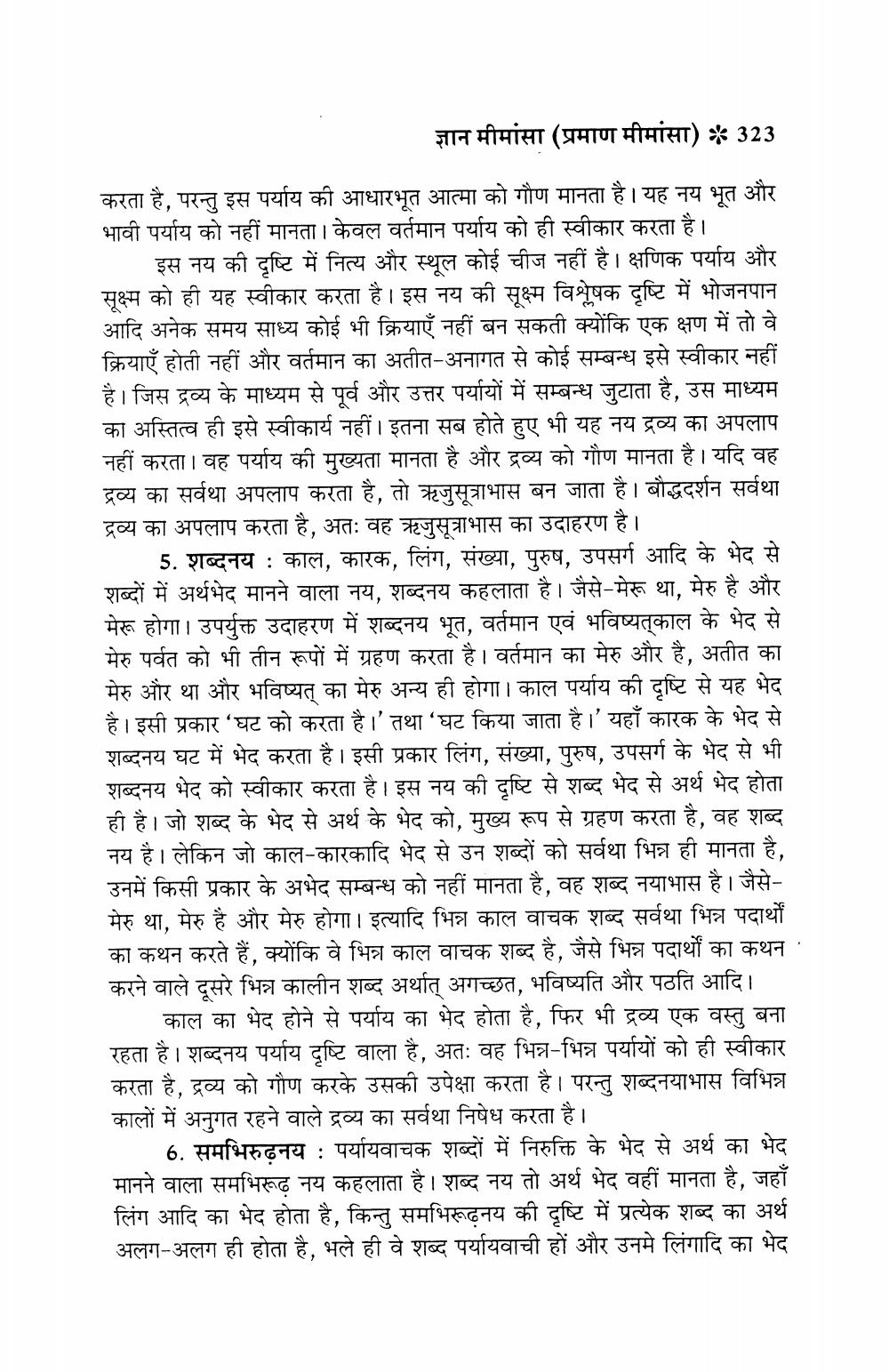________________
ज्ञान मीमांसा (प्रमाण मीमांसा) * 323
करता है, परन्तु इस पर्याय की आधारभूत आत्मा को गौण मानता है। यह नय भूत और भावी पर्याय को नहीं मानता। केवल वर्तमान पर्याय को ही स्वीकार करता है।
इस नय की दृष्टि में नित्य और स्थूल कोई चीज नहीं है। क्षणिक पर्याय और सूक्ष्म को ही यह स्वीकार करता है। इस नय की सूक्ष्म विशेषक दृष्टि में भोजनपान आदि अनेक समय साध्य कोई भी क्रियाएँ नहीं बन सकती क्योंकि एक क्षण में तो वे क्रियाएँ होती नहीं और वर्तमान का अतीत-अनागत से कोई सम्बन्ध इसे स्वीकार नहीं है। जिस द्रव्य के माध्यम से पूर्व और उत्तर पर्यायों में सम्बन्ध जुटाता है, उस माध्यम का अस्तित्व ही इसे स्वीकार्य नहीं। इतना सब होते हुए भी यह नय द्रव्य का अपलाप नहीं करता। वह पर्याय की मुख्यता मानता है और द्रव्य को गौण मानता है। यदि वह द्रव्य का सर्वथा अपलाप करता है, तो ऋजुसूत्राभास बन जाता है। बौद्धदर्शन सर्वथा द्रव्य का अपलाप करता है, अतः वह ऋजुसूत्राभास का उदाहरण है।
5. शब्दनय : काल, कारक, लिंग, संख्या, पुरुष, उपसर्ग आदि के भेद से शब्दों में अर्थभेद मानने वाला नय, शब्दनय कहलाता है। जैसे-मेरू था, मेरु है और मेरू होगा। उपर्युक्त उदाहरण में शब्दनय भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्काल के भेद से मेरु पर्वत को भी तीन रूपों में ग्रहण करता है। वर्तमान का मेरु और है, अतीत का मेरु और था और भविष्यत् का मेरु अन्य ही होगा। काल पर्याय की दृष्टि से यह भेद है। इसी प्रकार ‘घट को करता है।' तथा 'घट किया जाता है।' यहाँ कारक के भेद से शब्दनय घट में भेद करता है। इसी प्रकार लिंग, संख्या, पुरुष, उपसर्ग के भेद से भी शब्दनय भेद को स्वीकार करता है। इस नय की दृष्टि से शब्द भेद से अर्थ भेद होता ही है। जो शब्द के भेद से अर्थ के भेद को, मुख्य रूप से ग्रहण करता है, वह शब्द नय है। लेकिन जो काल-कारकादि भेद से उन शब्दों को सर्वथा भिन्न ही मानता है, उनमें किसी प्रकार के अभेद सम्बन्ध को नहीं मानता है, वह शब्द नयाभास है। जैसेमेरु था. मेरु है और मेरु होगा। इत्यादि भिन्न काल वाचक शब्द सर्वथा भिन्न पदार्थों का कथन करते हैं, क्योंकि वे भिन्न काल वाचक शब्द है, जैसे भिन्न पदार्थों का कथन करने वाले दूसरे भिन्न कालीन शब्द अर्थात् अगच्छत, भविष्यति और पठति आदि।
काल का भेद होने से पर्याय का भेद होता है, फिर भी द्रव्य एक वस्तु बना रहता है। शब्दनय पर्याय दृष्टि वाला है, अतः वह भिन्न-भिन्न पर्यायों को ही स्वीकार करता है, द्रव्य को गौण करके उसकी उपेक्षा करता है। परन्तु शब्दनयाभास विभिन्न कालों में अनुगत रहने वाले द्रव्य का सर्वथा निषेध करता है।
6. समभिरुढ़नय : पर्यायवाचक शब्दों में निरुक्ति के भेद से अर्थ का भेद मानने वाला समभिरूढ़ नय कहलाता है। शब्द नय तो अर्थ भेद वहीं मानता है, जहाँ लिंग आदि का भेद होता है, किन्तु समभिरूढनय की दृष्टि में प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग-अलग ही होता है, भले ही वे शब्द पर्यायवाची हों और उनमे लिंगादि का भेद