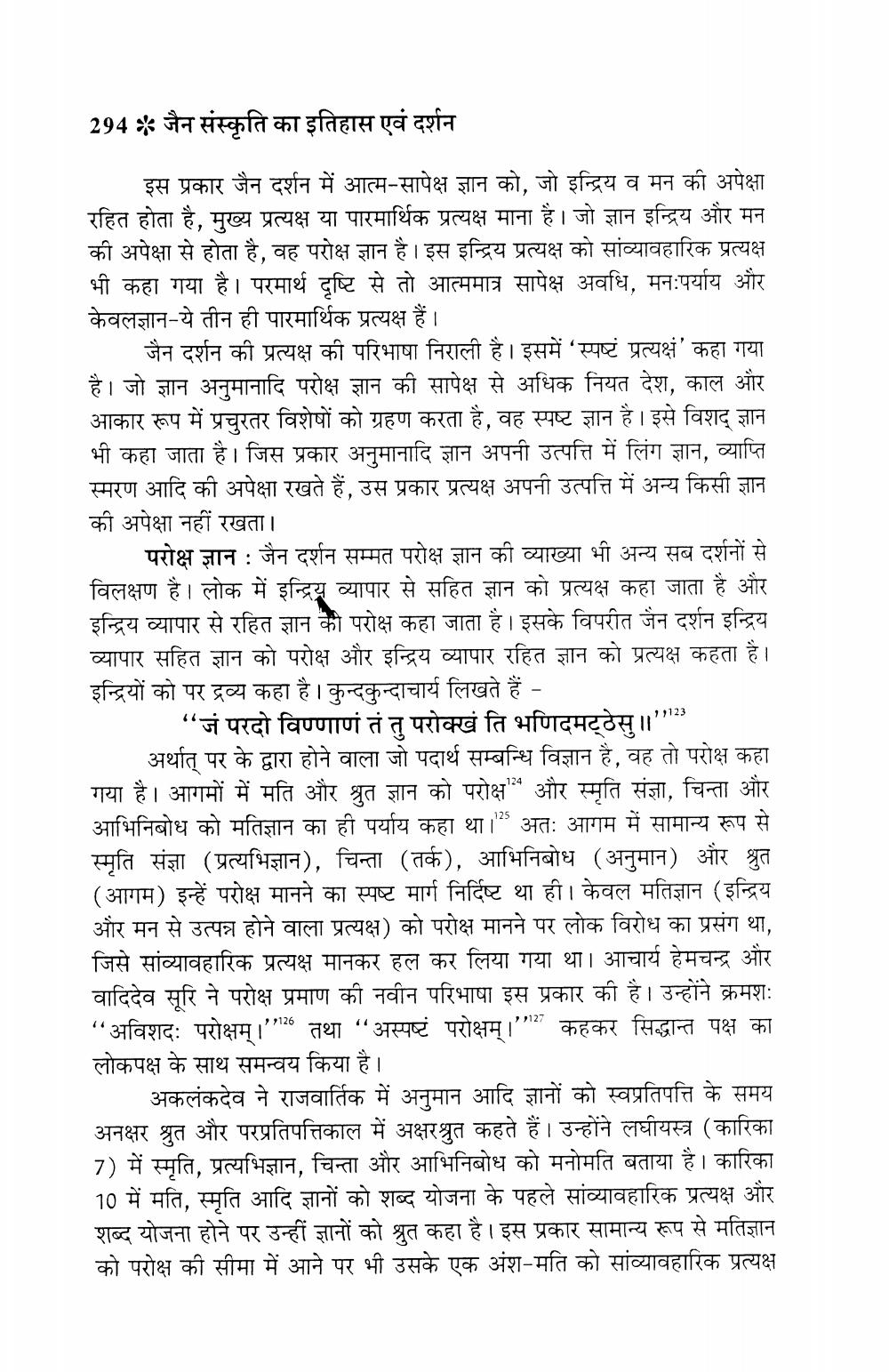________________
294 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
इस प्रकार जैन दर्शन में आत्म-सापेक्ष ज्ञान को, जो इन्द्रिय व मन की अपेक्षा रहित होता है, मुख्य प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना है। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा से होता है, वह परोक्ष ज्ञान है। इस इन्द्रिय प्रत्यक्ष को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। परमार्थ दृष्टि से तो आत्ममात्र सापेक्ष अवधि, मनःपर्याय और केवलज्ञान-ये तीन ही पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं।
जैन दर्शन की प्रत्यक्ष की परिभाषा निराली है। इसमें स्पष्टं प्रत्यक्षं' कहा गया है। जो ज्ञान अनुमानादि परोक्ष ज्ञान की सापेक्ष से अधिक नियत देश, काल और आकार रूप में प्रचुरतर विशेषों को ग्रहण करता है, वह स्पष्ट ज्ञान है। इसे विशद् ज्ञान भी कहा जाता है। जिस प्रकार अनुमानादि ज्ञान अपनी उत्पत्ति में लिंग ज्ञान, व्याप्ति स्मरण आदि की अपेक्षा रखते हैं, उस प्रकार प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति में अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता।
परोक्ष ज्ञान : जैन दर्शन सम्मत परोक्ष ज्ञान की व्याख्या भी अन्य सब दर्शनों से विलक्षण है। लोक में इन्द्रिय व्यापार से सहित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है और इन्द्रिय व्यापार से रहित ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। इसके विपरीत जैन दर्शन इन्द्रिय व्यापार सहित ज्ञान को परोक्ष और इन्द्रिय व्यापार रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहता है। इन्द्रियों को पर द्रव्य कहा है । कुन्दकुन्दाचार्य लिखते हैं -
"जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमठेसु॥"123 अर्थात् पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ सम्बन्धि विज्ञान है, वह तो परोक्ष कहा गया है। आगमों में मति और श्रुत ज्ञान को परोक्ष और स्मृति संज्ञा, चिन्ता और आभिनिबोध को मतिज्ञान का ही पर्याय कहा था। अतः आगम में सामान्य रूप से स्मृति संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क), आभिनिबोध (अनुमान) और श्रुत (आगम) इन्हें परोक्ष मानने का स्पष्ट मार्ग निर्दिष्ट था ही। केवल मतिज्ञान (इन्द्रिय
और मन से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष) को परोक्ष मानने पर लोक विरोध का प्रसंग था, जिसे सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष मानकर हल कर लिया गया था। आचार्य हेमचन्द्र और वादिदेव सूरि ने परोक्ष प्रमाण की नवीन परिभाषा इस प्रकार की है। उन्होंने क्रमशः “अविशदः परोक्षम्।"३० तथा “अस्पष्टं परोक्षम्।” कहकर सिद्धान्त पक्ष का लोकपक्ष के साथ समन्वय किया है।
अकलंकदेव ने राजवार्तिक में अनुमान आदि ज्ञानों को स्वप्रतिपत्ति के समय अनक्षर श्रुत और परप्रतिपत्तिकाल में अक्षरश्रुत कहते हैं। उन्होंने लघीयस्त्र (कारिका 7) में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, चिन्ता और आभिनिबोध को मनोमति बताया है। कारिका 10 में मति, स्मृति आदि ज्ञानों को शब्द योजना के पहले सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और शब्द योजना होने पर उन्हीं ज्ञानों को श्रुत कहा है। इस प्रकार सामान्य रूप से मतिज्ञान को परोक्ष की सीमा में आने पर भी उसके एक अंश-मति को सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष