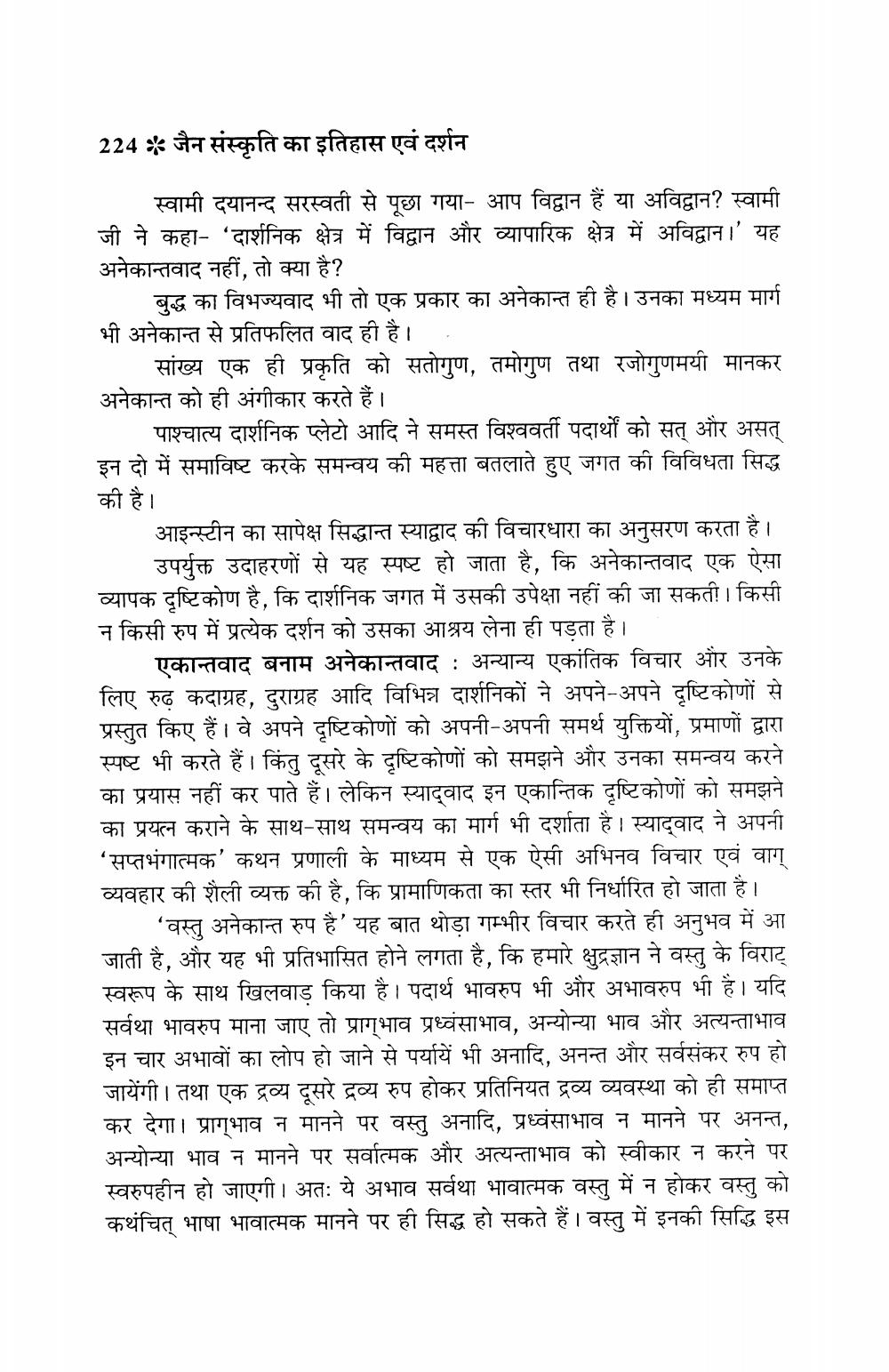________________
224 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
स्वामी दयानन्द सरस्वती से पूछा गया- आप विद्वान हैं या अविद्वान? स्वामी जी ने कहा- 'दार्शनिक क्षेत्र में विद्वान और व्यापारिक क्षेत्र में अविद्वान।' यह अनेकान्तवाद नहीं, तो क्या है?
बुद्ध का विभज्यवाद भी तो एक प्रकार का अनेकान्त ही है। उनका मध्यम मार्ग भी अनेकान्त से प्रतिफलित वाद ही है।
सांख्य एक ही प्रकृति को सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुणमयी मानकर अनेकान्त को ही अंगीकार करते हैं।
पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो आदि ने समस्त विश्ववर्ती पदार्थों को सत् और असत् इन दो में समाविष्ट करके समन्वय की महत्ता बतलाते हुए जगत की विविधता सिद्ध की है।
आइन्स्टीन का सापेक्ष सिद्धान्त स्याद्वाद की विचारधारा का अनुसरण करता है।
उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि अनेकान्तवाद एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है, कि दार्शनिक जगत में उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी न किसी रूप में प्रत्येक दर्शन को उसका आश्रय लेना ही पड़ता है।
एकान्तवाद बनाम अनेकान्तवाद : अन्यान्य एकांतिक विचार और उनके लिए रुढ़ कदाग्रह, दुराग्रह आदि विभिन्न दार्शनिकों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किए हैं। वे अपने दृष्टिकोणों को अपनी-अपनी समर्थ युक्तियों, प्रमाणों द्वारा स्पष्ट भी करते हैं। किंतु दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने और उनका समन्वय करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्यावाद इन एकान्तिक दृष्टिकोणों को समझने का प्रयत्न कराने के साथ-साथ समन्वय का मार्ग भी दर्शाता है। स्याद्वाद ने अपनी 'सप्तभंगात्मक' कथन प्रणाली के माध्यम से एक ऐसी अभिनव विचार एवं वाग् व्यवहार की शैली व्यक्त की है, कि प्रामाणिकता का स्तर भी निर्धारित हो जाता है।
'वस्तु अनेकान्त रुप है' यह बात थोड़ा गम्भीर विचार करते ही अनुभव में आ जाती है, और यह भी प्रतिभासित होने लगता है, कि हमारे क्षुद्रज्ञान ने वस्तु के विराट स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया है। पदार्थ भावरुप भी और अभावरुप भी है। यदि सर्वथा भावरुप माना जाए तो प्राग्भाव प्रध्वंसाभाव, अन्योन्या भाव और अत्यन्ताभाव इन चार अभावों का लोप हो जाने से पर्यायें भी अनादि, अनन्त और सर्वसंकर रुप हो जायेंगी। तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रुप होकर प्रतिनियत द्रव्य व्यवस्था को ही समाप्त कर देगा। प्राग्भाव न मानने पर वस्तु अनादि, प्रध्वंसाभाव न मानने पर अनन्त, अन्योन्या भाव न मानने पर सर्वात्मक और अत्यन्ताभाव को स्वीकार न करने पर स्वरुपहीन हो जाएगी। अतः ये अभाव सर्वथा भावात्मक वस्तु में न होकर वस्तु को कथंचित् भाषा भावात्मक मानने पर ही सिद्ध हो सकते हैं। वस्तु में इनकी सिद्धि इस