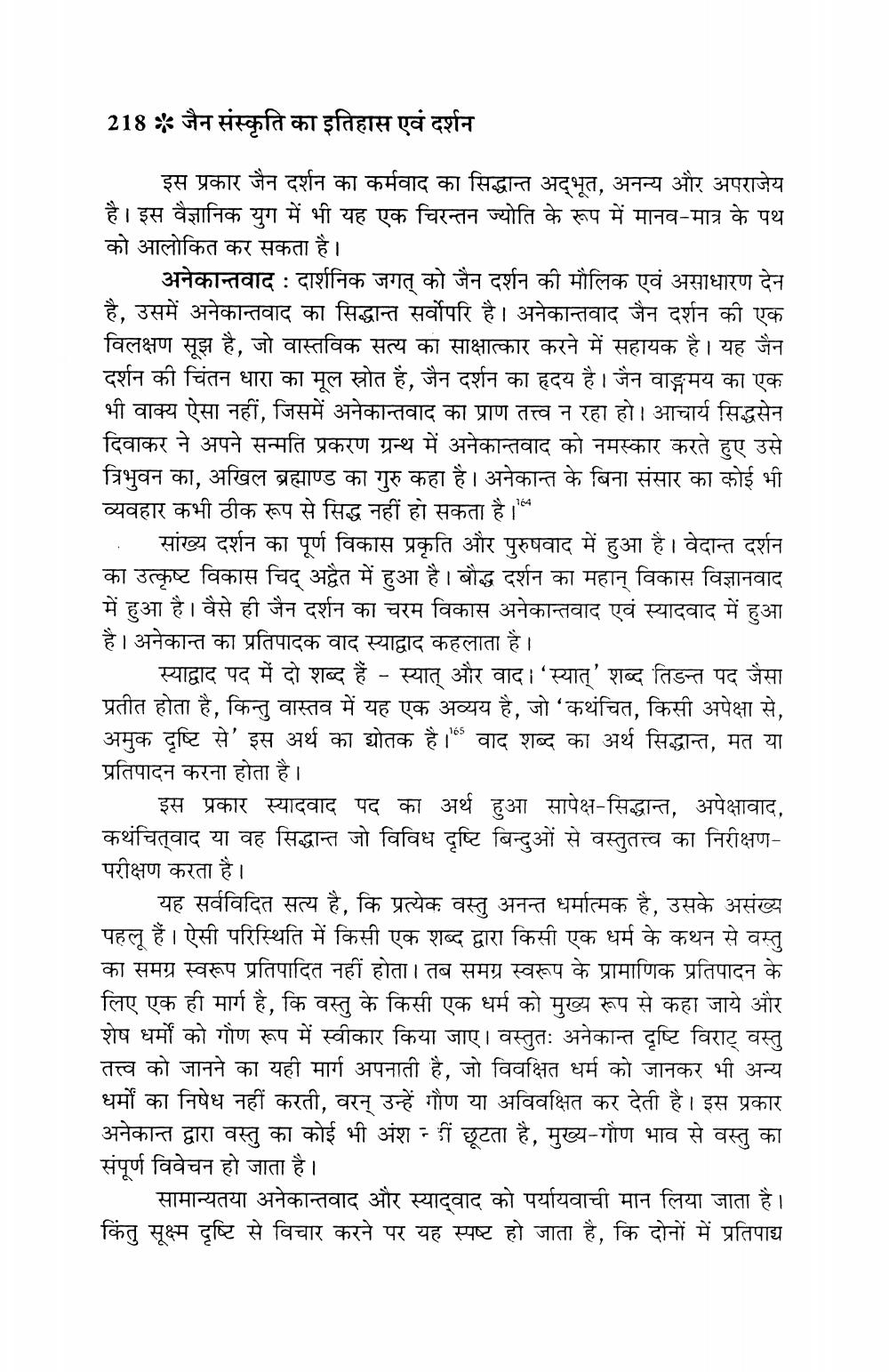________________
218* जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
इस प्रकार जैन दर्शन का कर्मवाद का सिद्धान्त अद्भूत, अनन्य और अपराजेय है। इस वैज्ञानिक युग में भी यह एक चिरन्तन ज्योति के रूप में मानव-मात्र के पथ को आलोकित कर सकता है।
अनेकान्तवाद : दार्शनिक जगत् को जैन दर्शन की मौलिक एवं असाधारण देन है, उसमें अनेकान्तवाद का सिद्धान्त सर्वोपरि है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की एक विलक्षण सूझ है, जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार करने में सहायक है। यह जैन दर्शन की चिंतन धारा का मूल स्रोत है, जैन दर्शन का हृदय है। जैन वाङ्गमय का एक भी वाक्य ऐसा नहीं, जिसमें अनेकान्तवाद का प्राण तत्त्व न रहा हो। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने सन्मति प्रकरण ग्रन्थ में अनेकान्तवाद को नमस्कार करते हुए उसे त्रिभुवन का, अखिल ब्रह्माण्ड का गुरु कहा है। अनेकान्त के बिना संसार का कोई भी व्यवहार कभी ठीक रूप से सिद्ध नहीं हो सकता है। .. सांख्य दर्शन का पूर्ण विकास प्रकृति और पुरुषवाद में हुआ है। वेदान्त दर्शन का उत्कृष्ट विकास चिद् अद्वैत में हुआ है। बौद्ध दर्शन का महान् विकास विज्ञानवाद में हुआ है। वैसे ही जैन दर्शन का चरम विकास अनेकान्तवाद एवं स्यादवाद में हुआ है। अनेकान्त का प्रतिपादक वाद स्याद्वाद कहलाता है।
स्याद्वाद पद में दो शब्द हैं - स्यात् और वाद। ‘स्यात्' शब्द तिङन्त पद जैसा प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में यह एक अव्यय है, जो 'कथंचित, किसी अपेक्षा से, अमुक दृष्टि से' इस अर्थ का द्योतक है। वाद शब्द का अर्थ सिद्धान्त, मत या प्रतिपादन करना होता है।
इस प्रकार स्यादवाद पद का अर्थ हुआ सापेक्ष-सिद्धान्त, अपेक्षावाद, कथंचित्वाद या वह सिद्धान्त जो विविध दृष्टि बिन्दुओं से वस्तुतत्त्व का निरीक्षणपरीक्षण करता है।
यह सर्वविदित सत्य है, कि प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है, उसके असंख्य पहलू हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी एक शब्द द्वारा किसी एक धर्म के कथन से वस्तु का समग्र स्वरूप प्रतिपादित नहीं होता। तब समग्र स्वरूप के प्रामाणिक प्रतिपादन के लिए एक ही मार्ग है, कि वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य रूप से कहा जाये और शेष धर्मों को गौण रूप में स्वीकार किया जाए। वस्तुतः अनेकान्त दृष्टि विराट् वस्तु तत्त्व को जानने का यही मार्ग अपनाती है, जो विवक्षित धर्म को जानकर भी अन्य धर्मों का निषेध नहीं करती, वरन् उन्हें गौण या अविवक्षित कर देती है। इस प्रकार अनेकान्त द्वारा वस्तु का कोई भी अंश - ही छूटता है, मुख्य-गौण भाव से वस्तु का संपूर्ण विवेचन हो जाता है।
सामान्यतया अनेकान्तवाद और स्याद्वाद को पर्यायवाची मान लिया जाता है। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि दोनों में प्रतिपाद्य