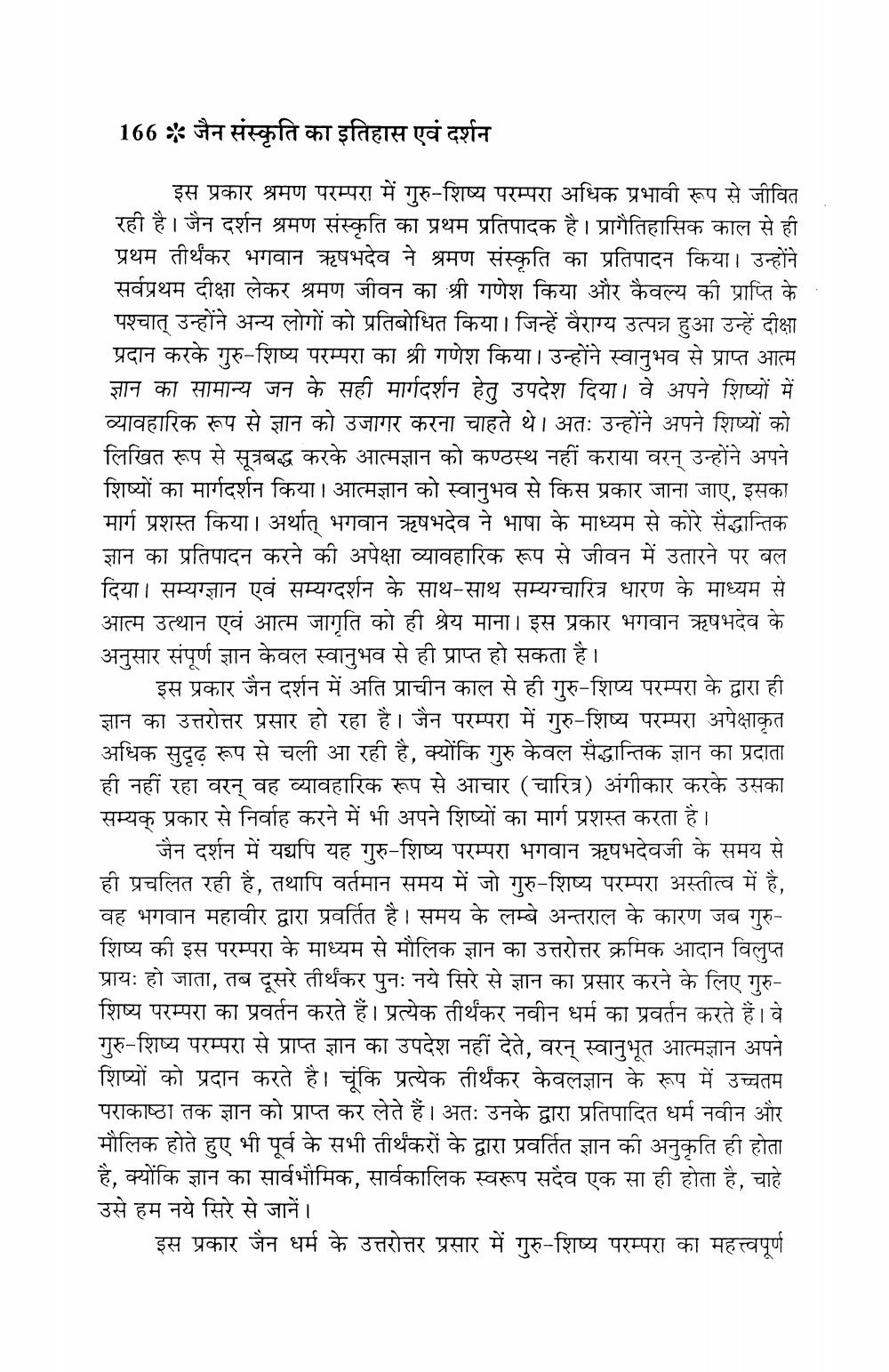________________
166 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
इस प्रकार श्रमण परम्परा में गुरु-शिष्य परम्परा अधिक प्रभावी रूप से जीवित रही है। जैन दर्शन श्रमण संस्कृति का प्रथम प्रतिपादक है। प्रागैतिहासिक काल से ही प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने श्रमण संस्कृति का प्रतिपादन किया। उन्होंने सर्वप्रथम दीक्षा लेकर श्रमण जीवन का श्री गणेश किया और कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने अन्य लोगों को प्रतिबोधित किया। जिन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ उन्हें दीक्षा प्रदान करके गुरु-शिष्य परम्परा का श्री गणेश किया। उन्होंने स्वानुभव से प्राप्त आत्म ज्ञान का सामान्य जन के सही मार्गदर्शन हेतु उपदेश दिया। वे अपने शिष्यों में व्यावहारिक रूप से ज्ञान को उजागर करना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने शिष्यों को लिखित रूप से सूत्रबद्ध करके आत्मज्ञान को कण्ठस्थ नहीं कराया वरन् उन्होंने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया। आत्मज्ञान को स्वानुभव से किस प्रकार जाना जाए, इसका मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात् भगवान ऋषभदेव ने भाषा के माध्यम से कोरे सैद्धान्तिक ज्ञान का प्रतिपादन करने की अपेक्षा व्यावहारिक रूप से जीवन में उतारने पर बल दिया। सम्यग्ज्ञान एवं सम्यग्दर्शन के साथ-साथ सम्यग्चारित्र धारण के माध्यम से आत्म उत्थान एवं आत्म जागृति को ही श्रेय माना। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के अनुसार संपूर्ण ज्ञान केवल स्वानुभव से ही प्राप्त हो सकता है।
__इस प्रकार जैन दर्शन में अति प्राचीन काल से ही गुरु-शिष्य परम्परा के द्वारा ही ज्ञान का उत्तरोत्तर प्रसार हो रहा है। जैन परम्परा में गुरु-शिष्य परम्परा अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ रूप से चली आ रही है, क्योंकि गुरु केवल सैद्धान्तिक ज्ञान का प्रदाता ही नहीं रहा वरन् वह व्यावहारिक रूप से आचार (चारित्र) अंगीकार करके उसका सम्यक् प्रकार से निर्वाह करने में भी अपने शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करता है।
जैन दर्शन में यद्यपि यह गुरु-शिष्य परम्परा भगवान ऋषभदेवजी के समय से ही प्रचलित रही है, तथापि वर्तमान समय में जो गुरु-शिष्य परम्परा अस्तीत्व में है, वह भगवान महावीर द्वारा प्रवर्तित है। समय के लम्बे अन्तराल के कारण जब गुरुशिष्य की इस परम्परा के माध्यम से मौलिक ज्ञान का उत्तरोत्तर क्रमिक आदान विलुप्त प्रायः हो जाता, तब दूसरे तीर्थंकर पुनः नये सिरे से ज्ञान का प्रसार करने के लिए गुरुशिष्य परम्परा का प्रवर्तन करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर नवीन धर्म का प्रवर्तन करते हैं। वे गुरु-शिष्य परम्परा से प्राप्त ज्ञान का उपदेश नहीं देते, वरन् स्वानुभूत आत्मज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान करते है। चूंकि प्रत्येक तीर्थंकर केवलज्ञान के रूप में उच्चतम पराकाष्ठा तक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अतः उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म नवीन और मौलिक होते हुए भी पूर्व के सभी तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित ज्ञान की अनुकृति ही होता है, क्योंकि ज्ञान का सार्वभौमिक, सार्वकालिक स्वरूप सदैव एक सा ही होता है, चाहे उसे हम नये सिरे से जानें।
इस प्रकार जैन धर्म के उत्तरोत्तर प्रसार में गुरु-शिष्य परम्परा का महत्त्वपूर्ण