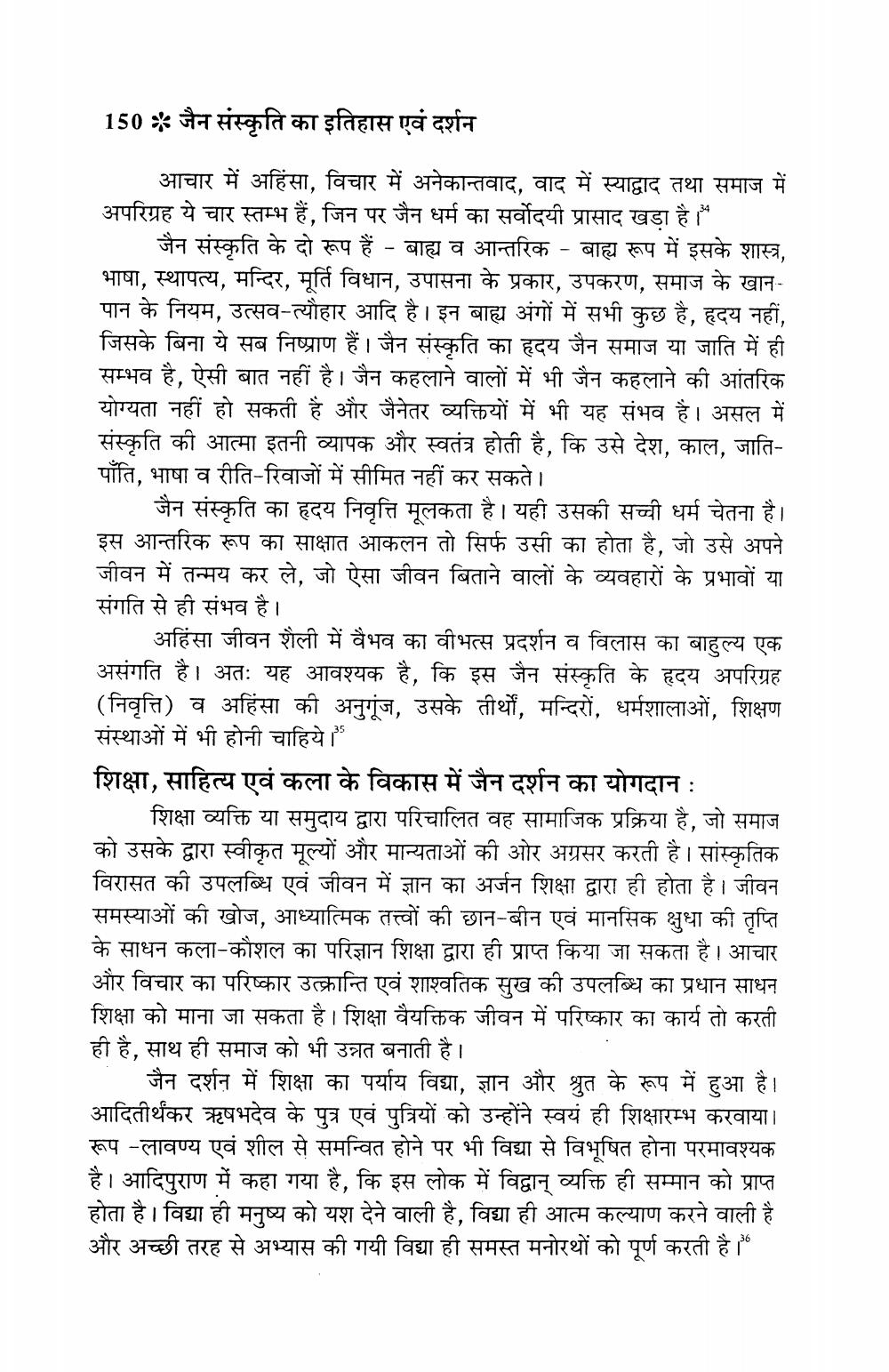________________
150 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
आचार में अहिंसा, विचार में अनेकान्तवाद, वाद में स्याद्वाद तथा समाज में अपरिग्रह ये चार स्तम्भ हैं, जिन पर जैन धर्म का सर्वोदयी प्रासाद खड़ा है।
जैन संस्कृति के दो रूप हैं - बाह्य व आन्तरिक - बाह्य रूप में इसके शास्त्र, भाषा, स्थापत्य, मन्दिर, मूर्ति विधान, उपासना के प्रकार, उपकरण, समाज के खानपान के नियम, उत्सव-त्यौहार आदि है। इन बाह्य अंगों में सभी कुछ है, हृदय नहीं, जिसके बिना ये सब निष्प्राण हैं। जैन संस्कृति का हृदय जैन समाज या जाति में ही सम्भव है, ऐसी बात नहीं है। जैन कहलाने वालों में भी जैन कहलाने की आंतरिक योग्यता नहीं हो सकती है और जैनेतर व्यक्तियों में भी यह संभव है। असल में संस्कृति की आत्मा इतनी व्यापक और स्वतंत्र होती है, कि उसे देश, काल, जातिपाँति, भाषा व रीति-रिवाजों में सीमित नहीं कर सकते।
जैन संस्कृति का हृदय निवृत्ति मूलकता है। यही उसकी सच्ची धर्म चेतना है। इस आन्तरिक रूप का साक्षात आकलन तो सिर्फ उसी का होता है, जो उसे अपने जीवन में तन्मय कर ले, जो ऐसा जीवन बिताने वालों के व्यवहारों के प्रभावों या संगति से ही संभव है।
अहिंसा जीवन शैली में वैभव का वीभत्स प्रदर्शन व विलास का बाहुल्य एक असंगति है। अतः यह आवश्यक है, कि इस जैन संस्कृति के हृदय अपरिग्रह (निवृत्ति) व अहिंसा की अनुगूंज, उसके तीर्थों, मन्दिरों, धर्मशालाओं, शिक्षण संस्थाओं में भी होनी चाहिये। शिक्षा, साहित्य एवं कला के विकास में जैन दर्शन का योगदान :
शिक्षा व्यक्ति या समुदाय द्वारा परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज को उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और मान्यताओं की ओर अग्रसर करती है। सांस्कृतिक विरासत की उपलब्धि एवं जीवन में ज्ञान का अर्जन शिक्षा द्वारा ही होता है। जीवन समस्याओं की खोज, आध्यात्मिक तत्त्वों की छान-बीन एवं मानसिक क्षुधा की तृप्ति के साधन कला-कौशल का परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आचार
और विचार का परिष्कार उत्क्रान्ति एवं शाश्वतिक सुख की उपलब्धि का प्रधान साधन शिक्षा को माना जा सकता है। शिक्षा वैयक्तिक जीवन में परिष्कार का कार्य तो करती ही है, साथ ही समाज को भी उन्नत बनाती है।
जैन दर्शन में शिक्षा का पर्याय विद्या, ज्ञान और श्रुत के रूप में हुआ है। आदितीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र एवं पुत्रियों को उन्होंने स्वयं ही शिक्षारम्भ करवाया। रूप -लावण्य एवं शील से समन्वित होने पर भी विद्या से विभूषित होना परमावश्यक है। आदिपुराण में कहा गया है, कि इस लोक में विद्वान् व्यक्ति ही सम्मान को प्राप्त होता है। विद्या ही मनुष्य को यश देने वाली है, विद्या ही आत्म कल्याण करने वाली है और अच्छी तरह से अभ्यास की गयी विद्या ही समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है।"