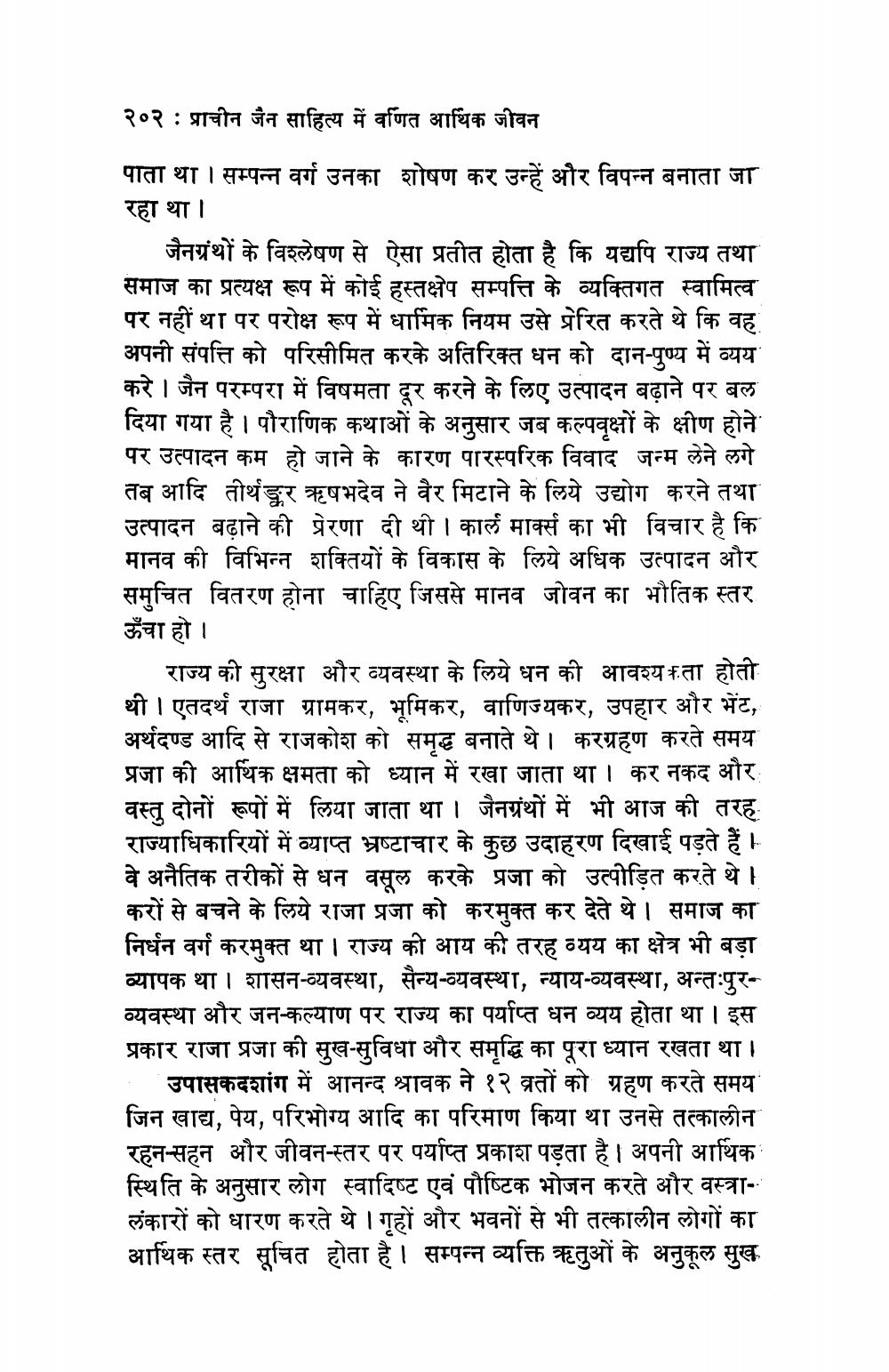________________
२०२ : प्राचीन जैन साहित्य में वर्णित आर्थिक जीवन पाता था । सम्पन्न वर्ग उनका शोषण कर उन्हें और विपन्न बनाता जा रहा था।
जैनग्रंथों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि राज्य तथा समाज का प्रत्यक्ष रूप में कोई हस्तक्षेप सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व पर नहीं था पर परोक्ष रूप में धार्मिक नियम उसे प्रेरित करते थे कि वह अपनी संपत्ति को परिसीमित करके अतिरिक्त धन को दान-पुण्य में व्यय करे । जैन परम्परा में विषमता दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है । पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कल्पवृक्षों के क्षीण होने पर उत्पादन कम हो जाने के कारण पारस्परिक विवाद जन्म लेने लगे तब आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव ने वैर मिटाने के लिये उद्योग करने तथा उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी थी। कार्ल मार्क्स का भी विचार है कि मानव की विभिन्न शक्तियों के विकास के लिये अधिक उत्पादन और समुचित वितरण होना चाहिए जिससे मानव जीवन का भौतिक स्तर ऊँचा हो।
राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिये धन की आवश्यकता होती थी। एतदर्थ राजा ग्रामकर, भूमिकर, वाणिज्यकर, उपहार और भेंट, अर्थदण्ड आदि से राजकोश को समृद्ध बनाते थे। करग्रहण करते समय प्रजा की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता था। कर नकद और वस्तु दोनों रूपों में लिया जाता था। जैनग्रंथों में भी आज की तरह राज्याधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। वे अनैतिक तरीकों से धन वसूल करके प्रजा को उत्पीड़ित करते थे। करों से बचने के लिये राजा प्रजा को करमुक्त कर देते थे। समाज का निर्धन वर्ग करमुक्त था। राज्य की आय की तरह व्यय का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक था। शासन-व्यवस्था, सैन्य-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था, अन्तःपुरव्यवस्था और जन-कल्याण पर राज्य का पर्याप्त धन व्यय होता था। इस प्रकार राजा प्रजा की सुख-सुविधा और समृद्धि का पूरा ध्यान रखता था।
उपासकदशांग में आनन्द श्रावक ने १२ व्रतों को ग्रहण करते समय जिन खाद्य, पेय, परिभोग्य आदि का परिमाण किया था उनसे तत्कालीन रहन-सहन और जीवन-स्तर पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार लोग स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन करते और वस्त्रालंकारों को धारण करते थे । गृहों और भवनों से भी तत्कालीन लोगों का आर्थिक स्तर सूचित होता है । सम्पन्न व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल सुख