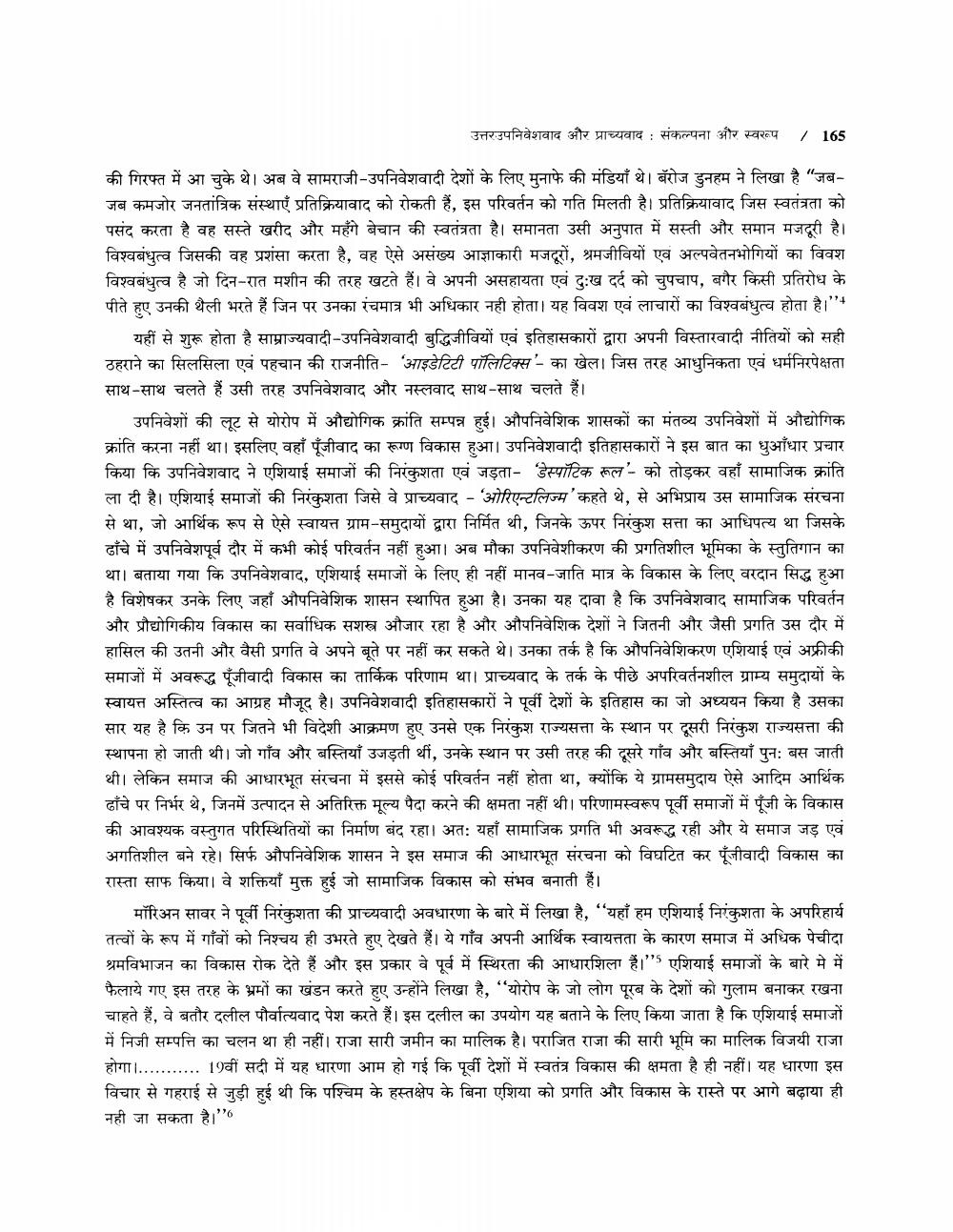________________
उत्तरउपनिवेशवाद और प्राच्यवाद : संकल्पना और स्वरूप / 165
की गिरफ्त में आ चुके थे। अब वे सामराजी-उपनिवेशवादी देशों के लिए मुनाफे की मंडियाँ थे। बॅरोज डुनहम ने लिखा है "जबजब कमजोर जनतांत्रिक संस्थाएँ प्रतिक्रियावाद को रोकती हैं, इस परिवर्तन को गति मिलती है। प्रतिक्रियावाद जिस स्वतंत्रता को पसंद करता है वह सस्ते खरीद और महँगे बेचान की स्वतंत्रता है। समानता उसी अनुपात में सस्ती और समान मजदूरी है। विश्वबंधुत्व जिसकी वह प्रशंसा करता है, वह ऐसे असंख्य आज्ञाकारी मजदूरों, श्रमजीवियों एवं अल्पवेतनभोगियों का विवश विश्वबंधुत्व है जो दिन-रात मशीन की तरह खटते हैं। वे अपनी असहायता एवं दुःख दर्द को चुपचाप, बगैर किसी प्रतिरोध के पीते हुए उनकी थैली भरते हैं जिन पर उनका रंचमात्र भी अधिकार नही होता। यह विवश एवं लाचारों का विश्वबंधुत्व होता है।''
से शुरू होता है साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी बुद्धिजीवियों एवं इतिहासकारों द्वारा अपनी विस्तारवादी नीतियों को सही ठहराने का सिलसिला एवं पहचान की राजनीति- 'आइडेटिटी पॉलिटिक्स'- का खेल। जिस तरह आधुनिकता एवं धर्मनिरपेक्षता साथ-साथ चलते हैं उसी तरह उपनिवेशवाद और नस्लवाद साथ-साथ चलते हैं।
उपनिवेशों की लूट से योरोप में औद्योगिक क्रांति सम्पन्न हुई। औपनिवेशिक शासकों का मंतव्य उपनिवेशों में औद्योगिक क्रांति करना नहीं था। इसलिए वहाँ पूँजीवाद का रूग्ण विकास हुआ। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने इस बात का धुआँधार प्रचार किया कि उपनिवेशवाद ने एशियाई समाजों की निरंकुशता एवं जड़ता- 'डेस्पॉटिक रूल'- को तोड़कर वहाँ सामाजिक क्रांति ला दी है। एशियाई समाजों की निरंकुशता जिसे वे प्राच्यवाद - 'ओरिएन्टलिज्म' कहते थे, से अभिप्राय उस सामाजिक संरचना से था, जो आर्थिक रूप से ऐसे स्वायत्त ग्राम-समुदायों द्वारा निर्मित थी, जिनके ऊपर निरंकुश सत्ता का आधिपत्य था जिसके ढाँचे में उपनिवेशपूर्व दौर में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मौका उपनिवेशीकरण की प्रगतिशील भूमिका के स्तुतिगान का था। बताया गया कि उपनिवेशवाद, एशियाई समाजों के लिए ही नहीं मानव-जाति मात्र के विकास के लिए वरदान सिद्ध हुआ है विशेषकर उनके लिए जहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है। उनका यह दावा है कि उपनिवेशवाद सामाजिक परिवर्तन
और प्रौद्योगिकीय विकास का सर्वाधिक सशस्त्र औजार रहा है और औपनिवेशिक देशों ने जितनी और जैसी प्रगति उस दौर में हासिल की उतनी और वैसी प्रगति वे अपने बूते पर नहीं कर सकते थे। उनका तर्क है कि औपनिवेशिकरण एशियाई एवं अफ्रीकी समाजों में अवरूद्ध पूँजीवादी विकास का तार्किक परिणाम था। प्राच्यवाद के तर्क के पीछे अपरिवर्तनशील ग्राम्य समुदायों के स्वायत्त अस्तित्व का आग्रह मौजूद है। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने पूर्वी देशों के इतिहास का जो अध्ययन किया है उसका सार यह है कि उन पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उनसे एक निरंकुश राज्यसत्ता के स्थान पर दूसरी निरंकुश राज्यसत्ता की स्थापना हो जाती थी। जो गाँव और बस्तियाँ उजड़ती थीं, उनके स्थान पर उसी तरह की दूसरे गाँव और बस्तियाँ पुनः बस जाती थी। लेकिन समाज की आधारभूत संरचना में इससे कोई परिवर्तन नहीं होता था, क्योंकि ये ग्रामसमुदाय ऐसे आदिम आर्थिक ढाँचे पर निर्भर थे, जिनमें उत्पादन से अतिरिक्त मूल्य पैदा करने की क्षमता नहीं थी। परिणामस्वरूप पूर्वी समाजों में पूँजी के विकास की आवश्यक वस्तुगत परिस्थितियों का निर्माण बंद रहा। अतः यहाँ सामाजिक प्रगति भी अवरूद्ध रही और ये समाज जड़ एवं अगतिशील बने रहे। सिर्फ औपनिवेशिक शासन ने इस समाज की आधारभूत संरचना को विघटित कर पूँजीवादी विकास का रास्ता साफ किया। वे शक्तियाँ मुक्त हुई जो सामाजिक विकास को संभव बनाती हैं।
मॉरिअन सावर ने पूर्वी निरंकुशता की प्राच्यवादी अवधारणा के बारे में लिखा है, “यहाँ हम एशियाई निरंकुशता के अपरिहार्य तत्वों के रूप में गाँवों को निश्चय ही उभरते हुए देखते हैं। ये गाँव अपनी आर्थिक स्वायत्तता के कारण समाज में अधिक पेचीदा श्रमविभाजन का विकास रोक देते हैं और इस प्रकार वे पूर्व में स्थिरता की आधारशिला हैं।'' एशियाई समाजों के बारे मे में फैलाये गए इस तरह के भ्रमों का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा है, “योरोप के जो लोग पूरब के देशों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वे बतौर दलील पौर्वात्यवाद पेश करते हैं। इस दलील का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि एशियाई समाजों में निजी सम्पत्ति का चलन था ही नहीं। राजा सारी जमीन का मालिक है। पराजित राजा की सारी भूमि का मालिक विजयी राजा होगा।........... 19वीं सदी में यह धारणा आम हो गई कि पूर्वी देशों में स्वतंत्र विकास की क्षमता है ही नहीं। यह धारणा इस विचार से गहराई से जुड़ी हुई थी कि पश्चिम के हस्तक्षेप के बिना एशिया को प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया ही नही जा सकता है।"