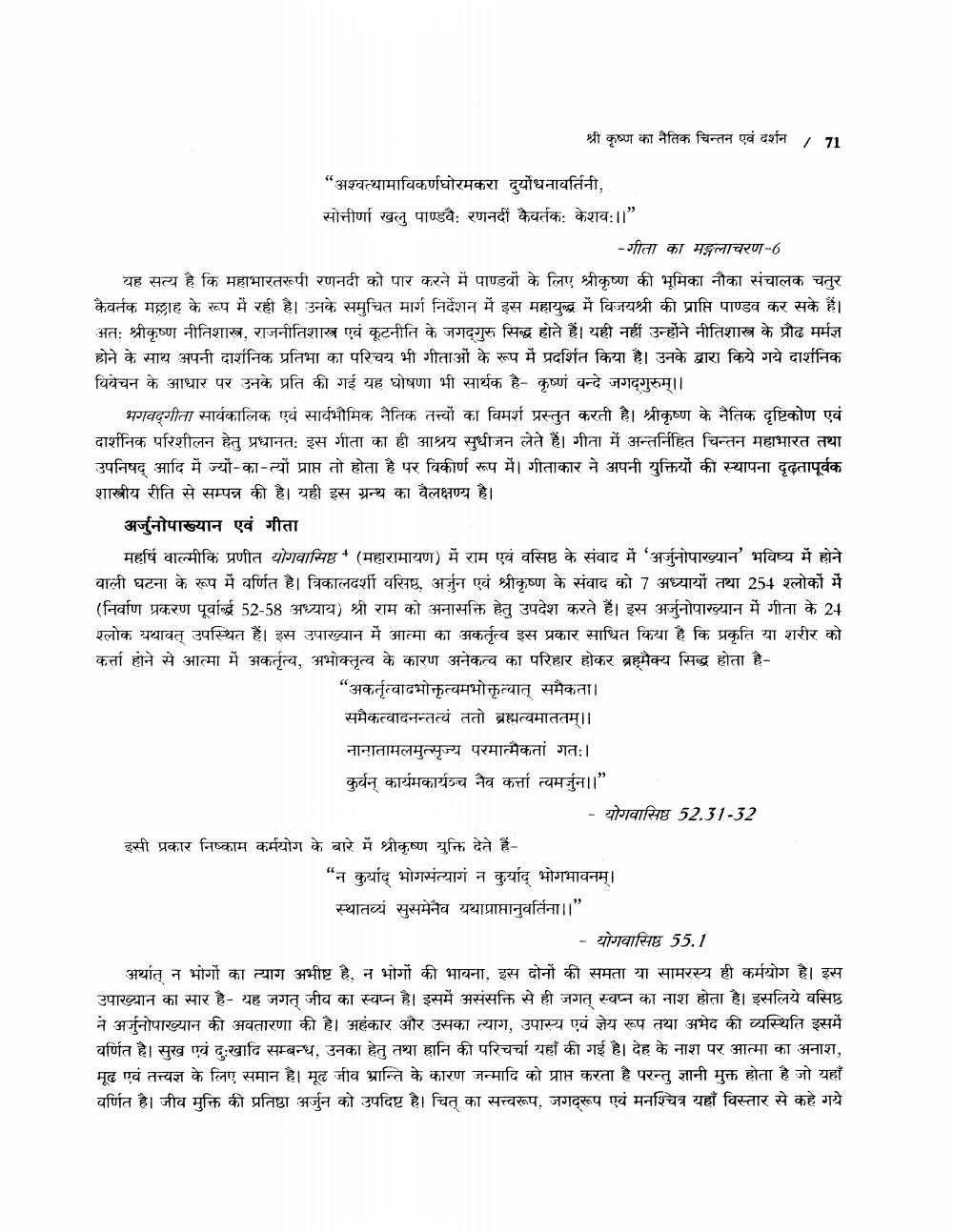________________
श्री कृष्ण का नैतिक चिन्तन एवं दर्शन / 71
"अश्वत्थामाविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी कैवर्तक: केशवः।।"
-गीता का मङ्गलाचरण-6 यह सत्य है कि महाभारतरूपी रणनदी को पार करने में पाण्डवों के लिए श्रीकृष्ण की भूमिका नौका संचालक चतुर कैवर्तक मल्लाह के रूप में रही है। उनके समुचित मार्ग निर्देशन में इस महायुद्ध में विजयश्री की प्राप्ति पाण्डव कर सके हैं। अत: श्रीकृष्ण नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं कूटनीति के जगद्गुरु सिद्ध होते हैं। यही नहीं उन्होंने नीतिशास्त्र के प्रौढ मर्मज्ञ होने के साथ अपनी दार्शनिक प्रतिभा का परिचय भी गीताओं के रूप में प्रदर्शित किया है। उनके द्वारा किये गये दार्शनिक विवेचन के आधार पर उनके प्रति की गई यह घोषणा भी सार्थक है- कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।।
भगवद्गीता सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक नैतिक तत्त्वों का विमर्श प्रस्तुत करती है। श्रीकृष्ण के नैतिक दृष्टिकोण एवं दार्शनिक परिशीलन हेतु प्रधानत: इस गीता का ही आश्रय सुधीजन लेते हैं। गीता में अन्तर्निहित चिन्तन महाभारत तथा उपनिषद् आदि में ज्यों-का-त्यों प्राप्त तो होता है पर विकीर्ण रूप में। गीताकार ने अपनी युक्तियों की स्थापना दृढ़तापूर्वक शास्त्रीय रीति से सम्पन्न की है। यही इस ग्रन्थ का वैलक्षण्य है।
अर्जुनोपाख्यान एवं गीता
महर्षि वाल्मीकि प्रणीत योगवासिष्ठ + (महारामायण) में राम एवं वसिष्ठ के संवाद में 'अर्जुनोपाख्यान' भविष्य में होने वाली घटना के रूप में वर्णित है। त्रिकालदर्शी वसिष्ठ, अर्जुन एवं श्रीकृष्ण के संवाद को 7 अध्यायों तथा 254 श्लोकों में (निर्वाण प्रकरण पूर्वार्द्ध 52-58 अध्याय) श्री राम को अनासक्ति हेतु उपदेश करते हैं। इस अर्जुनोपाख्यान में गीता के 24 श्लोक यथावत् उपस्थित हैं। इस उपाख्यान में आत्मा का अकर्तृत्व इस प्रकार साधित किया है कि प्रकृति या शरीर को कर्ता होने से आत्मा में अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व के कारण अनेकत्व का परिहार होकर ब्रह्मैक्य सिद्ध होता है
"अकर्तृत्वादभोक्तृत्वमभोक्तृत्वात् समैकता। समैकत्वादनन्तत्वं ततो ब्रह्मत्वमाततम्।। नानातामलमुत्सृज्य परमात्मैकतां गतः। कुर्वन कार्यमकार्यञ्च नैव कर्ता त्वमर्जुन।।"
- योगवासिष्ठ 52.31-32 इसी प्रकार निष्काम कर्मयोग के बारे में श्रीकृष्ण युक्ति देते हैं
"न कुर्याद् भोगसंत्यागं न कुर्याद् भोगभावनम्। स्थातव्यं सुसमेनैव यथाप्राप्तानुवर्तिना।।"
- योगवासिष्ठ 55.1 अर्थात् न भोगों का त्याग अभीष्ट है, न भोगों की भावना, इस दोनों की समता या सामरस्य ही कर्मयोग है। इस उपाख्यान का सार है- यह जगत् जीव का स्वप्न है। इसमें असंसक्ति से ही जगत् स्वप्न का नाश होता है। इसलिये वसिष्ठ ने अर्जुनोपाख्यान की अवतारणा की है। अहंकार और उसका त्याग, उपास्य एवं जेय रूप तथा अभेद की व्यस्थिति इसमें वर्णित है। सुख एवं दुःखादि सम्बन्ध, उनका हेतु तथा हानि की परिचर्चा यहाँ की गई है। देह के नाश पर आत्मा का अनाश, मूढ एवं तत्त्वज्ञ के लिए समान है। मूढ जीव भ्रान्ति के कारण जन्मादि को प्राप्त करता है परन्तु ज्ञानी मुक्त होता है जो यहाँ वर्णित है। जीव मुक्ति की प्रतिष्ठा अर्जुन को उपदिष्ट है। चित् का सत्त्वरूप, जगद्प एवं मनश्चित्र यहाँ विस्तार से कहे गये