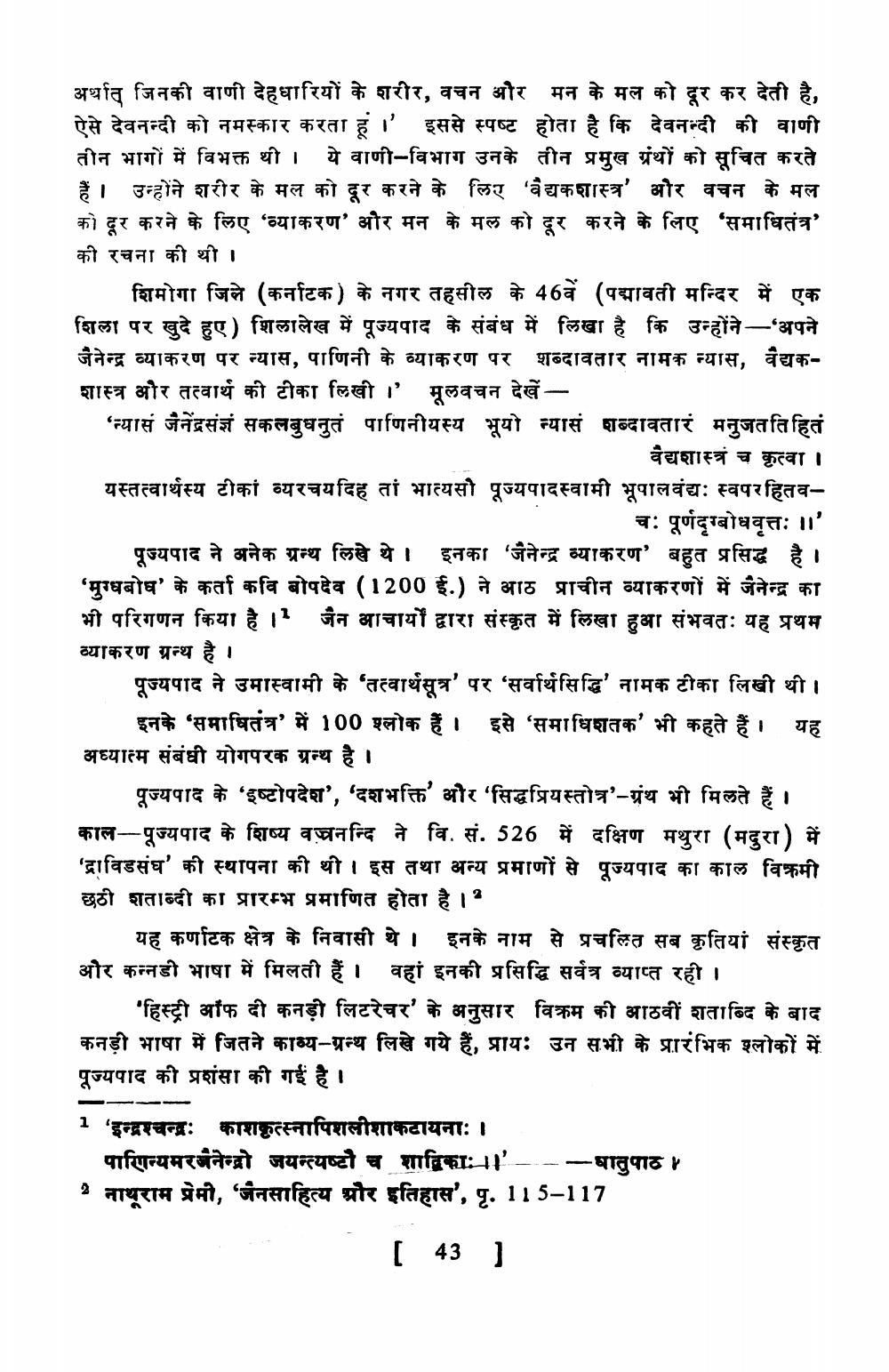________________
अर्थात् जिनकी वाणी देहधारियों के शरीर, वचन और मन के मल को दूर कर देती है, ऐसे देवनन्दी को नमस्कार करता हूं।' इससे स्पष्ट होता है कि देवनन्दी की वाणी तीन भागों में विभक्त थी। ये वाणी-विभाग उनके तीन प्रमुख ग्रंथों को सूचित करते हैं। उन्होंने शरीर के मल को दूर करने के लिए 'वैद्यकशास्त्र' और वचन के मल को दूर करने के लिए 'व्याकरण' और मन के मल को दूर करने के लिए 'समाधितंत्र' की रचना की थी।
शिमोगा जिले (कर्नाटक) के नगर तहसील के 46वें (पद्मावती मन्दिर में एक शिला पर खुदे हुए) शिलालेख में पूज्यपाद के संबंध में लिखा है कि उन्होंने–'अपने जैनेन्द्र व्याकरण पर न्यास, पाणिनी के व्याकरण पर शब्दावतार नामक न्यास, वैद्यकशास्त्र और तत्वार्थ की टीका लिखी।' मूलवचन देखें'न्यासं जैनेंद्रसंज्ञं सकलबुधनुतं पाणिनीयस्य भूयो न्यासं शब्दावतारं मनुजतति हितं
वैद्यशास्त्रं च कृत्वा । यस्तत्वार्थस्य टीकां व्यरचयदिह तां भात्यसौ पूज्यपादस्वामी भूपालवंद्यः स्वपरहितव
चः पूर्णदृग्बोधवृत्तः ॥' पूज्यपाद ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। इनका 'जैनेन्द्र व्याकरण' बहुत प्रसिद्ध है। 'मुग्धबोध' के कर्ता कवि बोपदेव (1200 ई.) ने आठ प्राचीन व्याकरणों में जैनेन्द्र का भी परिगणन किया है । जैन आचार्यों द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ संभवतः यह प्रथम व्याकरण ग्रन्थ है।
पूज्यपाद ने उमास्वामी के 'तत्वार्थसूत्र' पर 'सर्वार्थसिद्धि' नामक टीका लिखी थी।
इनके 'समाधितंत्र' में 100 श्लोक हैं। इसे 'समाधिशतक' भी कहते हैं। यह अध्यात्म संबंधी योगपरक ग्रन्थ है।
पूज्यपाद के 'इष्टोपदेश', 'दशभक्ति' और 'सिद्धप्रियस्तोत्र'-ग्रंथ भी मिलते हैं। काल-पूज्यपाद के शिष्य वज़नन्दि ने वि. सं. 526 में दक्षिण मथुरा (मदुरा) में 'द्राविडसंघ' की स्थापना की थी। इस तथा अन्य प्रमाणों से पूज्यपाद का काल विक्रमी छठी शताब्दी का प्रारम्भ प्रमाणित होता है।'
यह कर्णाटक क्षेत्र के निवासी थे। इनके नाम से प्रचलित सब कृतियां संस्कृत और कन्नडी भाषा में मिलती हैं। वहां इनकी प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त रही।
'हिस्ट्री ऑफ दी कनड़ी लिटरेचर' के अनुसार विक्रम की आठवीं शताब्दि के बाद कनड़ी भाषा में जितने काव्य-ग्रन्थ लिखे गये हैं, प्रायः उन सभी के प्रारंभिक श्लोकों में पूज्यपाद की प्रशंसा की गई है।
1 'इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायनाः ।
पाणिन्यमरजनेन्द्रो जयन्त्यष्टौ च शातिकाः।। ----पातुपाठ । . नाथूराम प्रेमी, 'जनसाहित्य और इतिहास', पृ. 11 5-117
[ 43 ]