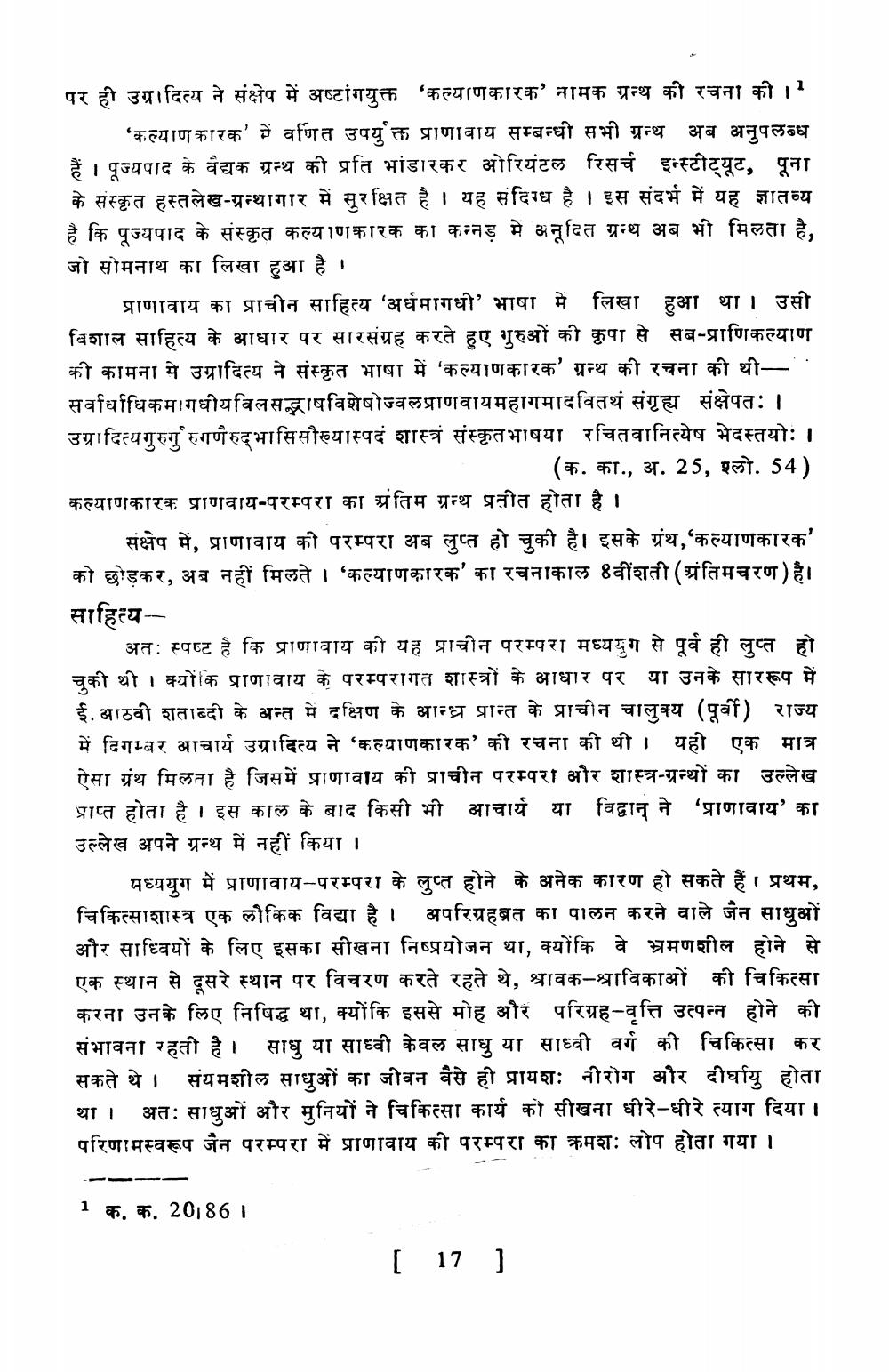________________
पर ही उग्रादित्य ने संक्षेप में अष्टांगयुक्त 'कल्याणकारक' नामक ग्रन्थ की रचना की ।।
'कल्याण कारक' में वर्णित उपयुक्त प्राणावाय सम्बन्धी सभी ग्रन्थ अब अनुपलब्ध हैं । पूज्यपाद के वैद्यक ग्रन्थ की प्रति भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना के संस्कृत हस्तलेख-ग्रन्थागार में सुरक्षित है । यह संदिग्ध है । इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि पूज्यपाद के संस्कृत कल्याणकारक का कन्नड़ में अनूदित ग्रन्थ अब भी मिलता है, जो सोमनाथ का लिखा हुआ है ।
प्राणावाय का प्राचीन साहित्य 'अर्धमागधी' भाषा में लिखा हुआ था। उसी विशाल साहित्य के आधार पर सारसंग्रह करते हुए गुरुओं की कृपा से सब-प्राणिकल्याण की कामना से उग्रादित्य ने संस्कृत भाषा में 'कल्याणकारक' ग्रन्थ की रचना की थीसर्वार्धाधिकमागधीयविलसद्भाषविशेषोज्वलप्राणवायमहागमादवितथं संगृह्य संक्षेपतः । उग्रादित्यगुरुगुरुगणैरुद्भासिसौख्यास्पदं शास्त्रं संस्कृतभाषया रचितवानित्येष भेदस्तयोः ।
(क. का., अ. 25, श्लो. 54) कल्याणकारक प्राणवाय-परम्परा का अंतिम ग्रन्थ प्रतीत होता है ।
संक्षेप में, प्राणावाय की परम्परा अब लुप्त हो चुकी है। इसके ग्रंथ, कल्याणकारक' को छोड़कर, अब नहीं मिलते । 'कल्याणकारक' का रचनाकाल 8वींशती (अंतिमचरण) है। साहित्य
अत: स्पष्ट है कि प्राणावाय की यह प्राचीन परम्परा मध्ययुग से पूर्व ही लुप्त हो चुकी थी। क्योंकि प्राणावाय के परम्परागत शास्त्रों के आधार पर या उनके साररूप में ई. आठवी शताब्दी के अन्त में दक्षिण के आन्ध्र प्रान्त के प्राचीन चालुक्य (पूर्वी) राज्य में दिगम्बर आचार्य उग्रादित्य ने 'कल्याणकारक' की रचना की थी। यही एक मात्र ऐसा ग्रंथ मिलता है जिसमें प्राणावाय की प्राचीन परम्परा और शास्त्र-ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है । इस काल के बाद किसी भी आचार्य या विद्वान ने 'प्राणावाय' का उल्लेख अपने ग्रन्थ में नहीं किया।
मध्ययुग में प्राणावाय-परम्परा के लुप्त होने के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रथम, चिकित्साशास्त्र एक लौकिक विद्या है। अपरिग्रहब्रत का पालन करने वाले जैन साधुओं और साध्वियों के लिए इसका सीखना निष्प्रयोजन था, क्योंकि वे भ्रमणशील होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, श्रावक-श्राविकाओं की चिकित्सा करना उनके लिए निषिद्ध था, क्योंकि इससे मोह और परिग्रह-वृत्ति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। साधु या साध्वी केवल साधु या साध्वी वर्ग की चिकित्सा कर सकते थे। संयमशील साधुओं का जीवन वैसे ही प्रायशः नीरोग और दीर्घायु होता था। अतः साधुओं और मुनियों ने चिकित्सा कार्य को सीखना धीरे-धीरे त्याग दिया। परिणामस्वरूप जैन परम्परा में प्राणावाय की परम्परा का क्रमशः लोप होता गया।
1 क. क. 201861
[ 17 ]