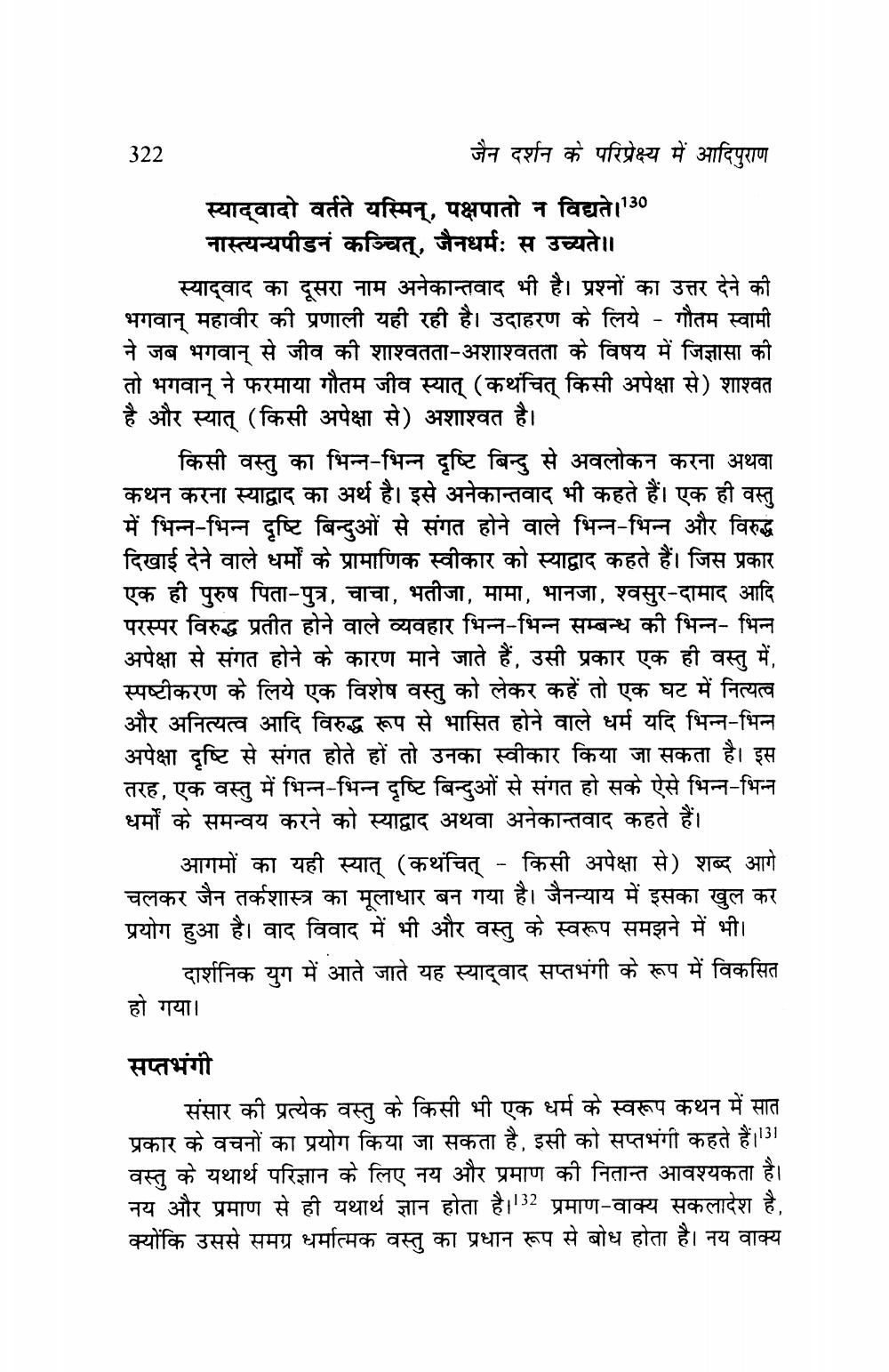________________
322
जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आदिपुराण
स्याद्वादो वर्तते यस्मिन्, पक्षपातो न विद्यते।।30
नास्त्यन्यपीडनं कञ्चित्, जैनधर्मः स उच्यते॥ स्याद्वाद का दूसरा नाम अनेकान्तवाद भी है। प्रश्नों का उत्तर देने की भगवान् महावीर की प्रणाली यही रही है। उदाहरण के लिये - गौतम स्वामी ने जब भगवान् से जीव की शाश्वतता-अशाश्वतता के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान् ने फरमाया गौतम जीव स्यात् (कथंचित् किसी अपेक्षा से) शाश्वत है और स्यात् (किसी अपेक्षा से) अशाश्वत है।
किसी वस्तु का भिन्न-भिन्न दृष्टि बिन्दु से अवलोकन करना अथवा कथन करना स्याद्वाद का अर्थ है। इसे अनेकान्तवाद भी कहते हैं। एक ही वस्तु में भिन्न-भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से संगत होने वाले भिन्न-भिन्न और विरुद्ध दिखाई देने वाले धर्मों के प्रामाणिक स्वीकार को स्याद्वाद कहते हैं। जिस प्रकार एक ही पुरुष पिता-पुत्र, चाचा, भतीजा, मामा, भानजा, श्वसुर-दामाद आदि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले व्यवहार भिन्न-भिन्न सम्बन्ध की भिन्न-भिन्न अपेक्षा से संगत होने के कारण माने जाते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु में, स्पष्टीकरण के लिये एक विशेष वस्तु को लेकर कहें तो एक घट में नित्यत्व और अनित्यत्व आदि विरुद्ध रूप से भासित होने वाले धर्म यदि भिन्न-भिन्न अपेक्षा दृष्टि से संगत होते हों तो उनका स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह, एक वस्तु में भिन्न-भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से संगत हो सके ऐसे भिन्न-भिन्न धर्मों के समन्वय करने को स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद कहते हैं।
आगमों का यही स्यात् (कथंचित् - किसी अपेक्षा से) शब्द आगे चलकर जैन तर्कशास्त्र का मूलाधार बन गया है। जैनन्याय में इसका खुल कर प्रयोग हुआ है। वाद विवाद में भी और वस्तु के स्वरूप समझने में भी। ____दार्शनिक युग में आते जाते यह स्याद्वाद सप्तभंगी के रूप में विकसित हो गया।
सप्तभंगी
संसार की प्रत्येक वस्तु के किसी भी एक धर्म के स्वरूप कथन में सात प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जा सकता है, इसी को सप्तभंगी कहते हैं।।31 वस्तु के यथार्थ परिज्ञान के लिए नय और प्रमाण की नितान्त आवश्यकता है। नय और प्रमाण से ही यथार्थ ज्ञान होता है।132 प्रमाण-वाक्य सकलादेश है, क्योंकि उससे समग्र धर्मात्मक वस्तु का प्रधान रूप से बोध होता है। नय वाक्य