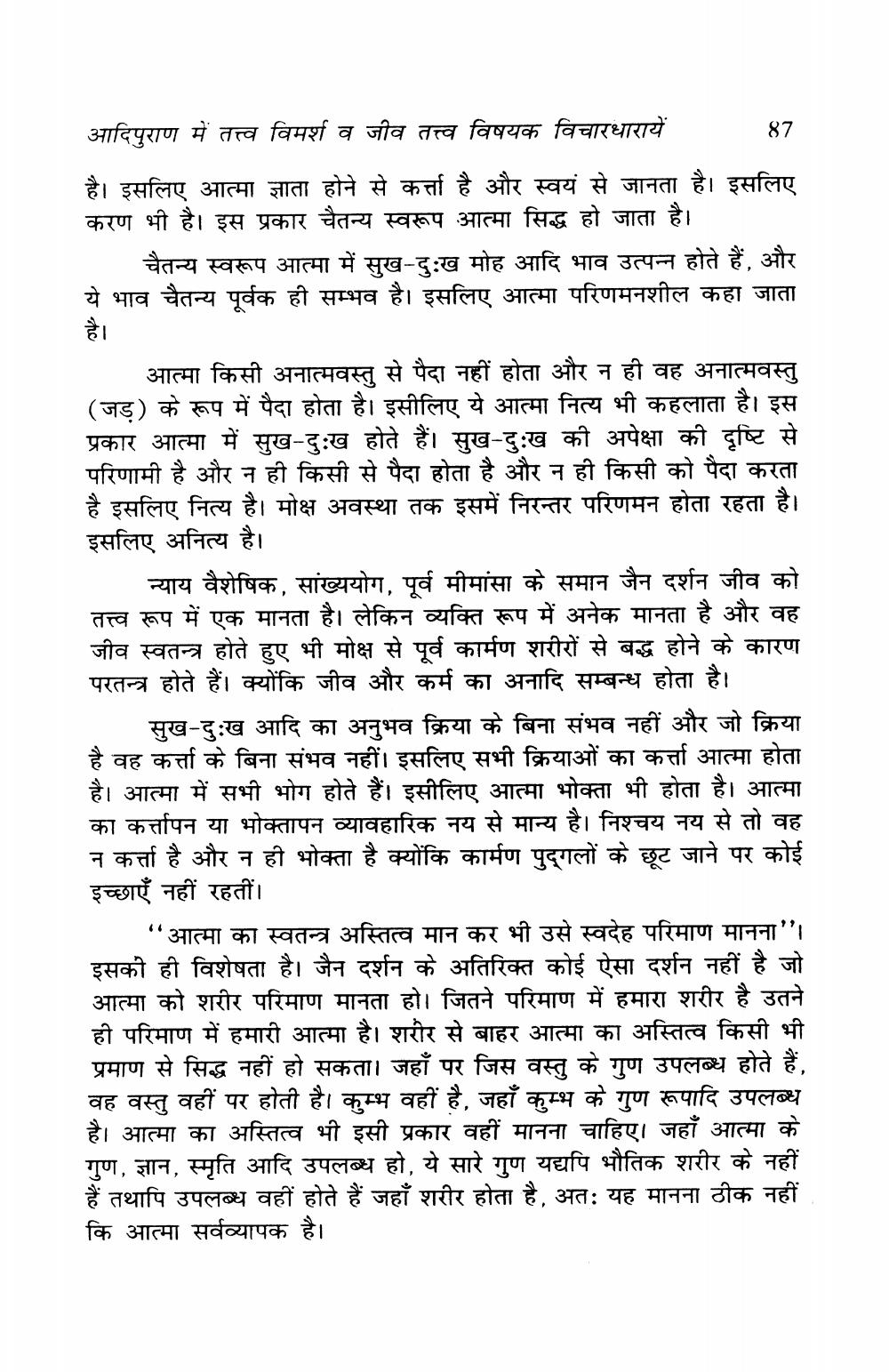________________
आदिपुराण में तत्त्व विमर्श व जीव तत्त्व विषयक विचारधारायें
है। इसलिए आत्मा ज्ञाता होने से कर्त्ता है और स्वयं से जानता है। इसलिए करण भी है। इस प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा सिद्ध हो जाता है।
87
चैतन्य स्वरूप आत्मा में सुख-दुःख मोह आदि भाव उत्पन्न होते हैं, और ये भाव चैतन्य पूर्वक ही सम्भव है। इसलिए आत्मा परिणमनशील कहा जाता है।
आत्मा किसी अनात्मवस्तु से पैदा नहीं होता और न ही वह अनात्मवस्तु (जड़) के रूप में पैदा होता है। इसीलिए ये आत्मा नित्य भी कहलाता है। इस प्रकार आत्मा में सुख - दुःख होते हैं। सुख - दुःख की अपेक्षा की दृष्टि से परिणामी है और न ही किसी से पैदा होता है और न ही किसी को पैदा करता है इसलिए नित्य है। मोक्ष अवस्था तक इसमें निरन्तर परिणमन होता रहता है। इसलिए अनित्य है ।
न्याय वैशेषिक, सांख्ययोग, पूर्व मीमांसा के समान जैन दर्शन जीव को तत्त्व रूप में एक मानता है। लेकिन व्यक्ति रूप में अनेक मानता है और वह जीव स्वतन्त्र होते हुए भी मोक्ष से पूर्व कार्मण शरीरों से बद्ध होने के कारण परतन्त्र होते हैं। क्योंकि जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध होता है।
सुख-दुःख आदि का अनुभव क्रिया के बिना संभव नहीं और जो क्रिया है वह कर्त्ता के बिना संभव नहीं । इसलिए सभी क्रियाओं का कर्त्ता आत्मा होता है। आत्मा में सभी भोग होते हैं। इसीलिए आत्मा भोक्ता भी होता है। आत्मा का कर्त्तापन या भोक्तापन व्यावहारिक नय से मान्य है। निश्चय नय से तो वह न कर्त्ता है और न ही भोक्ता है क्योंकि कार्मण पुद्गलों के छूट जाने पर कोई इच्छाएँ नहीं रहतीं।
44
'आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व मान कर भी उसे स्वदेह परिमाण मानना " । इसकी ही विशेषता है। जैन दर्शन के अतिरिक्त कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो आत्मा को शरीर परिमाण मानता हो । जितने परिमाण में हमारा शरीर है उतने ही परिमाण में हमारी आत्मा है। शरीर से बाहर आत्मा का अस्तित्व किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। जहाँ पर जिस वस्तु के गुण उपलब्ध होते हैं, वह वस्तु वहीं पर होती है। कुम्भ वहीं है, जहाँ कुम्भ के गुण रूपादि उपलब्ध है। आत्मा का अस्तित्व भी इसी प्रकार वहीं मानना चाहिए। जहाँ आत्मा के गुण, ज्ञान, स्मृति आदि उपलब्ध हो, ये सारे गुण यद्यपि भौतिक शरीर के नहीं हैं तथापि उपलब्ध वहीं होते हैं जहाँ शरीर होता है, अतः यह मानना ठीक नहीं कि आत्मा सर्वव्यापक है।