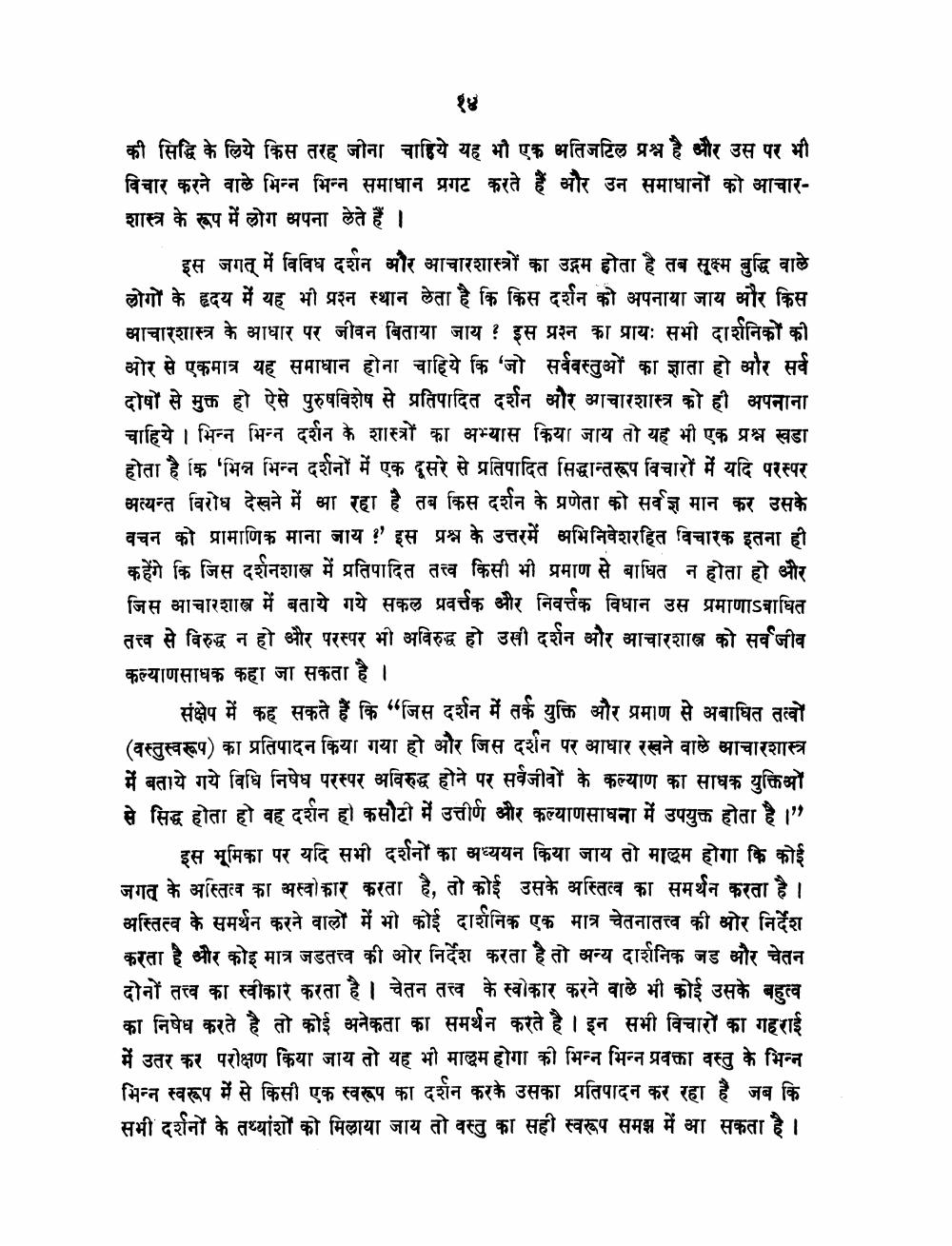________________
१४
की सिद्धि के लिये किस तरह जीना चाहिये यह भी एक भतिजटिल प्रश्न है और उस पर भी विचार करने वाले भिन्न भिन्न समाधान प्रगट करते हैं और उन समाधानों को आचारशास्त्र के रूप में लोग अपना लेते हैं ।
इस जगत् में विविध दर्शन और आचारशास्त्रों का उद्गम होता है तब सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों के हृदय में यह भी प्रश्न स्थान लेता है कि किस दर्शन को अपनाया जाय और किस आचारशास्त्र के आधार पर जीवन बिताया जाय ? इस प्रश्न का प्रायः सभी दार्शनिकों की ओर से एकमात्र यह समाधान होना चाहिये कि 'जो सर्ववस्तुओं का ज्ञाता हो और सर्व दोषों से मुक्त हो ऐसे पुरुषविशेष से प्रतिपादित दर्शन और आचारशास्त्र को ही अपनाना चाहिये । भिन्न भिन्न दर्शन के शास्त्रों का अभ्यास किया जाय तो यह भी एक प्रश्न खडा होता है कि 'भिन्न भिन्न दर्शनों में एक दूसरे से प्रतिपादित सिद्धान्तरूप विचारों में यदि परस्पर अत्यन्त विरोध देखने में आ रहा है तब किस दर्शन के प्रणेता को सर्वज्ञ मान कर उसके वचन को प्रामाणिक माना जाय ?' इस प्रश्न के उत्तरमें अभिनिवेशरहित विचारक इतना ही कहेंगे कि जिस दर्शनशास्त्र में प्रतिपादित तत्त्व किसी भी प्रमाण से बाधित न होता हो और जिस आचारशास्त्र में बताये गये सकल प्रवर्तक और निवर्त्तक विधान उस प्रमाणाऽबाधित तत्त्व से विरुद्ध न हो और परस्पर भी अविरुद्ध हो उसी दर्शन और आचारशास्त्र को सर्व जीव कल्याणसाधक कहा जा सकता है ।
संक्षेप में कह सकते हैं कि "जिस दर्शन में तर्क युक्ति और प्रमाण से अबाधित तत्वों (वस्तुस्वरूप) का प्रतिपादन किया गया हो और जिस दर्शन पर आधार रखने वाले आचारशास्त्र में बताये गये विधि निषेध परस्पर अविरुद्ध होने पर सर्वजीवों के कल्याण का साधक युक्तिओं से सिद्ध होता हो वह दर्शन हो कसौटी में उत्तीर्ण और कल्याणसाधना में उपयुक्त होता है।"
इस भूमिका पर यदि सभी दर्शनों का अध्ययन किया जाय तो मालूम होगा कि कोई जगत् के अस्तित्व का अस्वीकार करता है, तो कोई उसके अस्तित्व का समर्थन करता है। अस्तित्व के समर्थन करने वालों में भी कोई दार्शनिक एक मात्र चेतनातत्त्व की ओर निर्देश करता है और कोइ मात्र जडतत्त्व की ओर निर्देश करता है तो अन्य दार्शनिक जड और चेतन दोनों तत्त्व का स्वीकार करता है। चेतन तत्त्व के स्वीकार करने वाले भी कोई उसके बहुत्व का निषेध करते है तो कोई अनेकता का समर्थन करते है । इन सभी विचारों का गहराई में उतर कर परोक्षण किया जाय तो यह भी मालूम होगा की भिन्न भिन्न प्रवक्ता वस्तु के भिन्न भिन्न स्वरूप में से किसी एक स्वरूप का दर्शन करके उसका प्रतिपादन कर रहा है जब कि सभी दर्शनों के तथ्यांशों को मिलाया जाय तो वस्तु का सही स्वरूप समझ में आ सकता है।