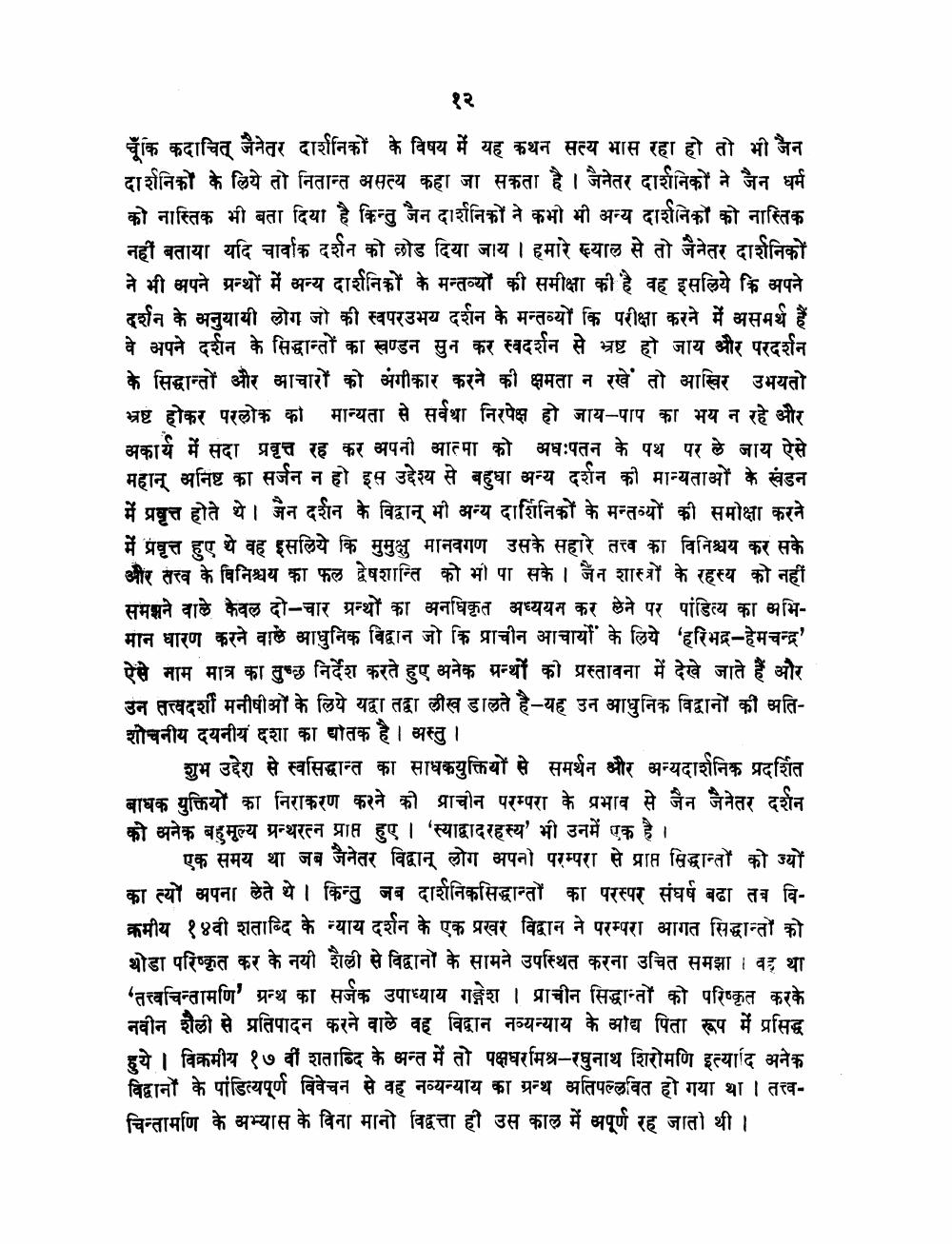________________
१२
चूँकि कदाचित् जैनेतर दार्शनिकों के विषय में यह कथन सत्य भास रहा हो तो भी जैन दार्शनिकों के लिये तो नितान्त असत्य कहा जा सकता है । जैनेतर दार्शनिकों ने जैन धर्म को नास्तिक भी बता दिया है किन्तु जैन दार्शनिकों ने कभी भी अन्य दार्शनिकों को नास्तिक नहीं बताया यदि चार्वाक दर्शन को छोड दिया जाय । हमारे ख्याल से तो जैनेतर दार्शनिकों ने भी अपने ग्रन्थों में अन्य दार्शनिकों के मन्तव्यों की समीक्षा की है वह इसलिये कि अपने दर्शन के अनुयायी लोग जो की स्वपरउभय दर्शन के मन्तव्यों कि परीक्षा करने में असमर्थ हैं वे अपने दर्शन के सिद्धान्तों का खण्डन सुन कर स्वदर्शन से भ्रष्ट हो जाय और परदर्शन के सिद्धान्तों और आचारों को अंगीकार करने की क्षमता न रखें तो आखिर उभयतो भ्रष्ट होकर परलोक को मान्यता से सर्वथा निरपेक्ष हो जाय - पाप का भय न रहे और कार्य में सदा प्रवृत्त रह कर अपनी आत्मा को अधःपतन के पथ पर ले जाय ऐसे महान् अनिष्ट का सर्जन न हो इस उद्देश्य से बहुधा अन्य दर्शन की मान्यताओं के खंडन
प्रवृत्त होते थे। जैन दर्शन के विद्वान् भी अन्य दार्शिनिकों के मन्तव्यों की समोक्षा करने में प्रवृत्त हुए थे वह इसलिये कि मुमुक्षु मानवगण उसके सहारे तत्त्व का विनिश्चय कर सके और तत्व के विनिश्चय का फल द्वेषशान्ति को भी पा सके । जैन शास्त्रों के रहस्य को नहीं समझने वाले केवल दो-चार ग्रन्थों का अनधिकृत अध्ययन कर लेने पर पांडित्य का अभिमान धारण करने वाले आधुनिक विद्वान जो कि प्राचीन आचार्यों के लिये 'हरिभद्र - हेमचन्द्र ' ऐसे नाम मात्र का तुच्छ निर्देश करते हुए अनेक ग्रन्थों को प्रस्तावना में देखे जाते हैं और उन तत्त्वदर्शी मनीषीओं के लिये यद्वा तद्वा लीख डालते है - यह उन आधुनिक विद्वानों की अतिशोचनीय दयनीय दशा का द्योतक है । अस्तु ।
शुभ उद्देश से स्वसिद्धान्त का साधकयुक्तियों से समर्थन और अन्यदार्शनिक प्रदर्शित aran युक्तियों का निराकरण करने की प्राचीन परम्परा के प्रभाव से जैन जैनेतर दर्शन को अनेक बहुमुल्य ग्रन्थरत्न प्राप्त हुए । 'स्याद्वाद रहस्य' भी उनमें एक है ।
एक समय था जब जैनेतर विद्वान् लोग अपनो परम्परा से प्राप्त सिद्धान्तों को ज्यों का त्यों अपना लेते थे । किन्तु जब दार्शनिकसिद्धान्तों का परस्पर संघर्ष बढा तत्र विक्रमीय १४वी शताब्दि के न्याय दर्शन के एक प्रखर विद्वान ने परम्परा आगत सिद्धान्तों को थोडा परिष्कृत कर के नयी शैली से विद्वानों के सामने उपस्थित करना उचित समझा। वह था 'तत्त्वचिन्तामणि' ग्रन्थ का सर्जक उपाध्याय गङ्गेश । प्राचीन सिद्धान्तों को परिष्कृत करके नवीन शैली से प्रतिपादन करने वाले वह विद्वान नव्यन्याय के औध पिता रूप में प्रसिद्ध हुये । विक्रमी १७ वीं शताब्दि के अन्त में तो पक्षधर मिश्र - रघुनाथ शिरोमणि इत्यादि अनेक विद्वानों के पांडित्यपूर्ण विवेचन से वह नव्यन्याय का ग्रन्थ अतिपल्लवित हो गया था । तत्त्वचिन्तामणि के अभ्यास के विना मानो विद्वत्ता ही उस काल में अपूर्ण रह जाती थी ।