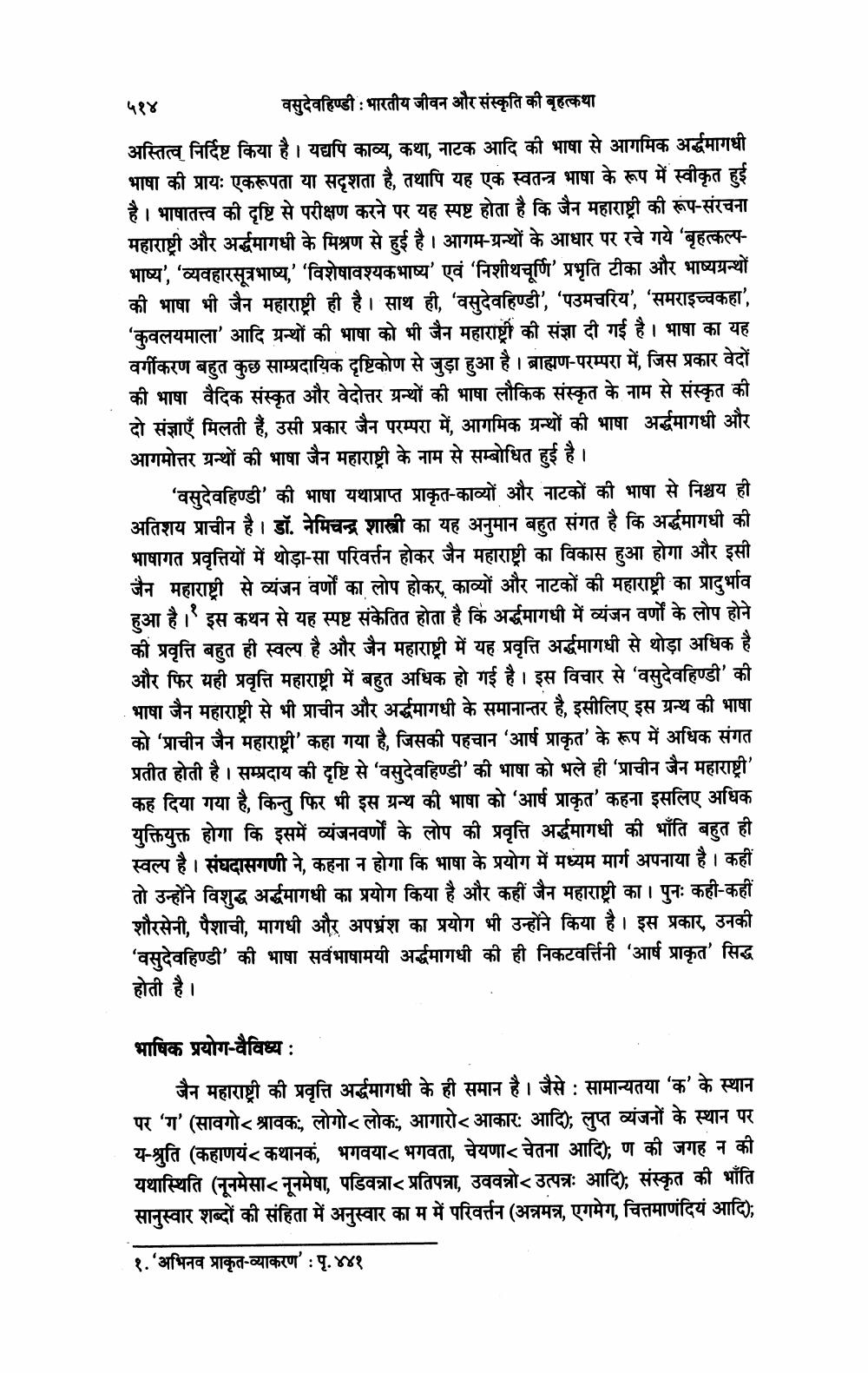________________
५१४
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा अस्तित्व निर्दिष्ट किया है। यद्यपि काव्य, कथा, नाटक आदि की भाषा से आगमिक अर्द्धमागधी भाषा की प्रायः एकरूपता या सदृशता है, तथापि यह एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। भाषातत्त्व की दृष्टि से परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैन महाराष्ट्री की रूप-संरचना महाराष्ट्री और अर्द्धमागधी के मिश्रण से हुई है। आगम-ग्रन्थों के आधार पर रचे गये 'बृहत्कल्पभाष्य', 'व्यवहारसूत्रभाष्य,' 'विशेषावश्यकभाष्य' एवं 'निशीथचूर्णि' प्रभृति टीका और भाष्यग्रन्थों की भाषा भी जैन महाराष्ट्री ही है। साथ ही, 'वसुदेवहिण्डी', 'पउमचरिय', 'समराइच्चकहा', 'कुवलयमाला' आदि ग्रन्थों की भाषा को भी जैन महाराष्ट्री की संज्ञा दी गई है। भाषा का यह वर्गीकरण बहुत कुछ साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण-परम्परा में, जिस प्रकार वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत और वेदोत्तर ग्रन्थों की भाषा लौकिक संस्कृत के नाम से संस्कृत की दो संज्ञाएँ मिलती हैं, उसी प्रकार जैन परम्परा में, आगमिक ग्रन्थों की भाषा अर्धमागधी और आगमोत्तर ग्रन्थों की भाषा जैन महाराष्ट्री के नाम से सम्बोधित हुई है।
'वसुदेवहिण्डी' की भाषा यथाप्राप्त प्राकृत-काव्यों और नाटकों की भाषा से निश्चय ही अतिशय प्राचीन है। डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री का यह अनुमान बहुत संगत है कि अर्द्धमागधी की भाषागत प्रवृत्तियों में थोड़ा-सा परिवर्तन होकर जैन महाराष्ट्री का विकास हुआ होगा और इसी
जैन महाराष्ट्री से व्यंजन वर्णों का लोप होकर, काव्यों और नाटकों की महाराष्ट्री का प्रादुर्भाव हुआ है। इस कथन से यह स्पष्ट संकेतित होता है कि अर्द्धमागधी में व्यंजन वर्गों के लोप होने की प्रवृत्ति बहुत ही स्वल्प है और जैन महाराष्ट्री में यह प्रवृत्ति अर्द्धमागधी से थोड़ा अधिक है
और फिर यही प्रवृत्ति महाराष्ट्री में बहुत अधिक हो गई है। इस विचार से 'वसुदेवहिण्डी' की भाषा जैन महाराष्ट्री से भी प्राचीन और अर्द्धमागधी के समानान्तर है, इसीलिए इस ग्रन्थ की भाषा को 'प्राचीन जैन महाराष्ट्री' कहा गया है, जिसकी पहचान 'आर्ष प्राकृत' के रूप में अधिक संगत प्रतीत होती है। सम्प्रदाय की दृष्टि से 'वसुदेवहिण्डी' की भाषा को भले ही 'प्राचीन जैन महाराष्ट्री' कह दिया गया है, किन्तु फिर भी इस ग्रन्थ की भाषा को 'आर्ष प्राकृत' कहना इसलिए अधिक युक्तियुक्त होगा कि इसमें व्यंजनवर्गों के लोप की प्रवृत्ति अर्द्धमागधी की भाँति बहुत ही स्वल्प है। संघदासगणी ने, कहना न होगा कि भाषा के प्रयोग में मध्यम मार्ग अपनाया है। कहीं तो उन्होंने विशुद्ध अर्धमागधी का प्रयोग किया है और कहीं जैन महाराष्ट्री का। पुनः कही-कहीं शौरसेनी, पैशाची, मागधी और अपभ्रंश का प्रयोग भी उन्होंने किया है। इस प्रकार, उनकी 'वसुदेवहिण्डी' की भाषा सर्वभाषामयी अर्द्धमागधी की ही निकटवर्तिनी 'आर्ष प्राकृत' सिद्ध होती है।
भाषिक प्रयोग-वैविध्य :
जैन महाराष्ट्री की प्रवृत्ति अर्द्धमागधी के ही समान है। जैसे : सामान्यतया 'क' के स्थान पर 'ग' (सावगो< श्रावक, लोगो< लोकः, आगारो< आकार: आदि); लुप्त व्यंजनों के स्थान पर य-श्रुति (कहाणयं< कथानकं, भगवया< भगवता, चेयणा< चेतना आदि); ण की जगह न की यथास्थिति (नूनमेसा< नूनमेषा, पडिवन्ना< प्रतिपन्ना, उववन्नो< उत्पन्नः आदि); संस्कृत की भाँति सानुस्वार शब्दों की संहिता में अनुस्वार का म में परिवर्तन (अन्नमन्न, एगमेग, चित्तमाणंदियं आदि);
१. अभिनव प्राकृत-व्याकरण' : पृ.४४१