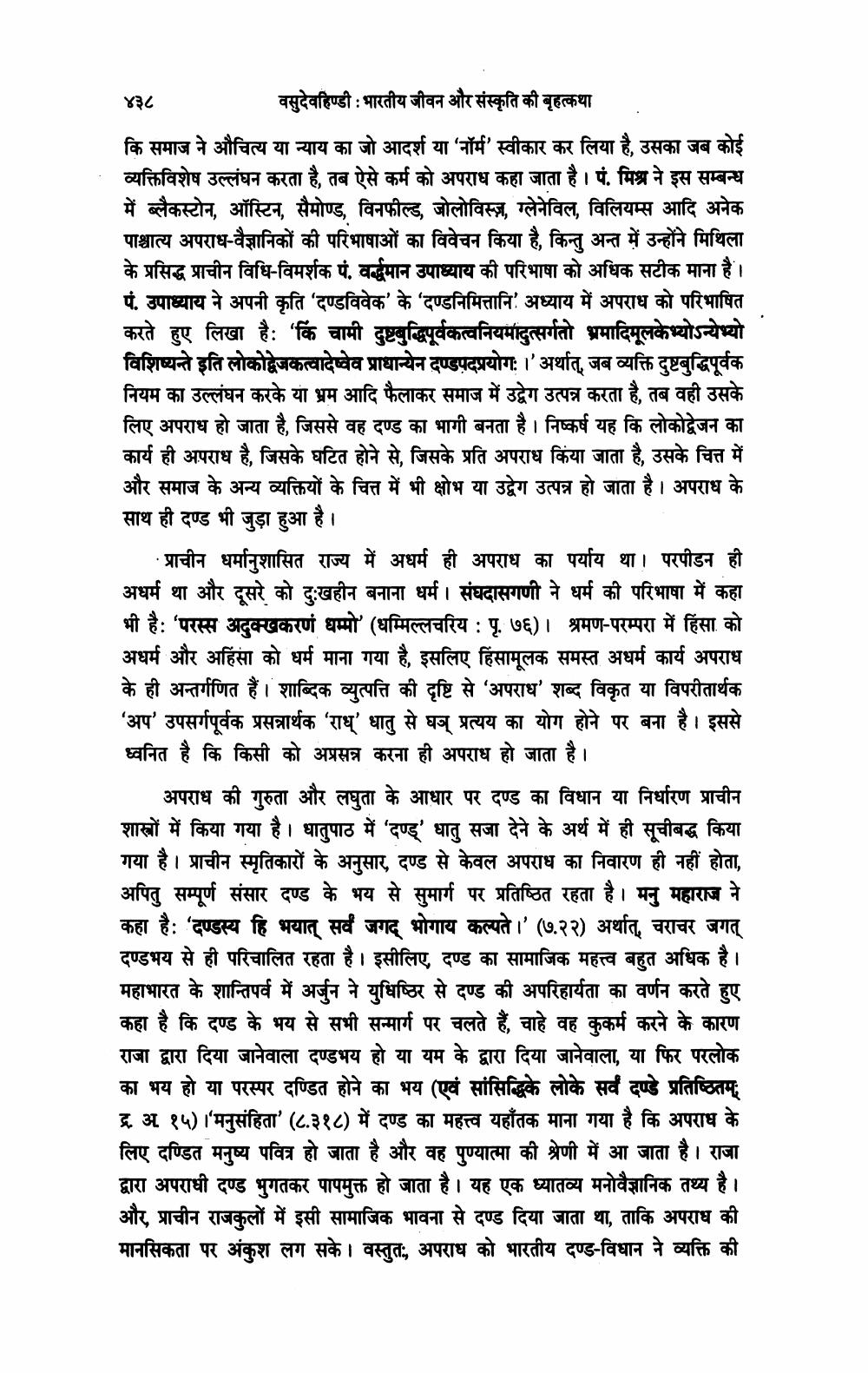________________
४३८
वसुदेवहिण्डी : भारतीय जीवन और संस्कृति की बृहत्कथा कि समाज ने औचित्य या न्याय का जो आदर्श या 'नॉर्म' स्वीकार कर लिया है, उसका जब कोई व्यक्तिविशेष उल्लंघन करता है, तब ऐसे कर्म को अपराध कहा जाता है। पं. मिश्र ने इस सम्बन्ध में ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन, सैमोण्ड, विनफील्ड, जोलोविस्ज़, ग्लेनेविल, विलियम्स आदि अनेक पाश्चात्य अपराध-वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का विवेचन किया है, किन्तु अन्त में उन्होंने मिथिला के प्रसिद्ध प्राचीन विधि-विमर्शक पं. वर्द्धमान उपाध्याय की परिभाषा को अधिक सटीक माना है। पं. उपाध्याय ने अपनी कृति 'दण्डविवेक' के 'दण्डनिमित्तानि' अध्याय में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है: “किं चामी दुष्टबुद्धिपूर्वकत्वनियमादुत्सर्गतो प्रमादिमूलकेभ्योऽन्येभ्यो विशिष्यन्ते इति लोकोद्वेजकत्वादेष्वेव प्राधान्येन दण्डपदप्रयोगः ।' अर्थात्, जब व्यक्ति दुष्टबुद्धिपूर्वक नियम का उल्लंघन करके या भ्रम आदि फैलाकर समाज में उद्वेग उत्पन्न करता है, तब वही उसके लिए अपराध हो जाता है, जिससे वह दण्ड का भागी बनता है। निष्कर्ष यह कि लोकोद्वेजन का कार्य ही अपराध है, जिसके घटित होने से, जिसके प्रति अपराध किया जाता है, उसके चित्त में
और समाज के अन्य व्यक्तियों के चित्त में भी क्षोभ या उद्वेग उत्पन्न हो जाता है। अपराध के साथ ही दण्ड भी जुड़ा हुआ है।
प्राचीन धर्मानुशासित राज्य में अधर्म ही अपराध का पर्याय था। परपीडन ही अधर्म था और दूसरे को दुःखहीन बनाना धर्म । संघदासगणी ने धर्म की परिभाषा में कहा भी है: 'परस्स अदुक्खकरणं धम्मो' (धम्मिल्लचरिय : पृ. ७६)। श्रमण-परम्परा में हिंसा को अधर्म और अहिंसा को धर्म माना गया है, इसलिए हिंसामूलक समस्त अधर्म कार्य अपराध के ही अन्तर्गणित हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'अपराध' शब्द विकृत या विपरीतार्थक 'अप' उपसर्गपूर्वक प्रसन्नार्थक ‘राध्' धातु से घञ् प्रत्यय का योग होने पर बना है। इससे ध्वनित है कि किसी को अप्रसन्न करना ही अपराध हो जाता है।
__ अपराध की गुरुता और लघुता के आधार पर दण्ड का विधान या निर्धारण प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। धातुपाठ में 'दण्ड्' धातु सजा देने के अर्थ में ही सूचीबद्ध किया गया है। प्राचीन स्मृतिकारों के अनुसार, दण्ड से केवल अपराध का निवारण ही नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण संसार दण्ड के भय से सुमार्ग पर प्रतिष्ठित रहता है। मनु महाराज ने कहा है: 'दण्डस्य हि भयात् सर्व जगद् भोगाय कल्पते।' (७.२२) अर्थात्, चराचर जगत् दण्डभय से ही परिचालित रहता है। इसीलिए, दण्ड का सामाजिक महत्त्व बहुत अधिक है। महाभारत के शान्तिपर्व में अर्जुन ने युधिष्ठिर से दण्ड की अपरिहार्यता का वर्णन करते हुए कहा है कि दण्ड के भय से सभी सन्मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह कुकर्म करने के कारण राजा द्वारा दिया जानेवाला दण्डभय हो या यम के द्वारा दिया जानेवाला, या फिर परलोक का भय हो या परस्पर दण्डित होने का भय (एवं सांसिद्धिके लोके सर्व दण्डे प्रतिष्ठितम्। द्र. अ १५)। मनुसंहिता' (८.३१८) में दण्ड का महत्त्व यहाँतक माना गया है कि अपराध के लिए दण्डित मनुष्य पवित्र हो जाता है और वह पुण्यात्मा की श्रेणी में आ जाता है। राजा द्वारा अपराधी दण्ड भुगतकर पापमुक्त हो जाता है। यह एक ध्यातव्य मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
और, प्राचीन राजकुलों में इसी सामाजिक भावना से दण्ड दिया जाता था, ताकि अपराध की मानसिकता पर अंकुश लग सके। वस्तुतः, अपराध को भारतीय दण्ड-विधान ने व्यक्ति की