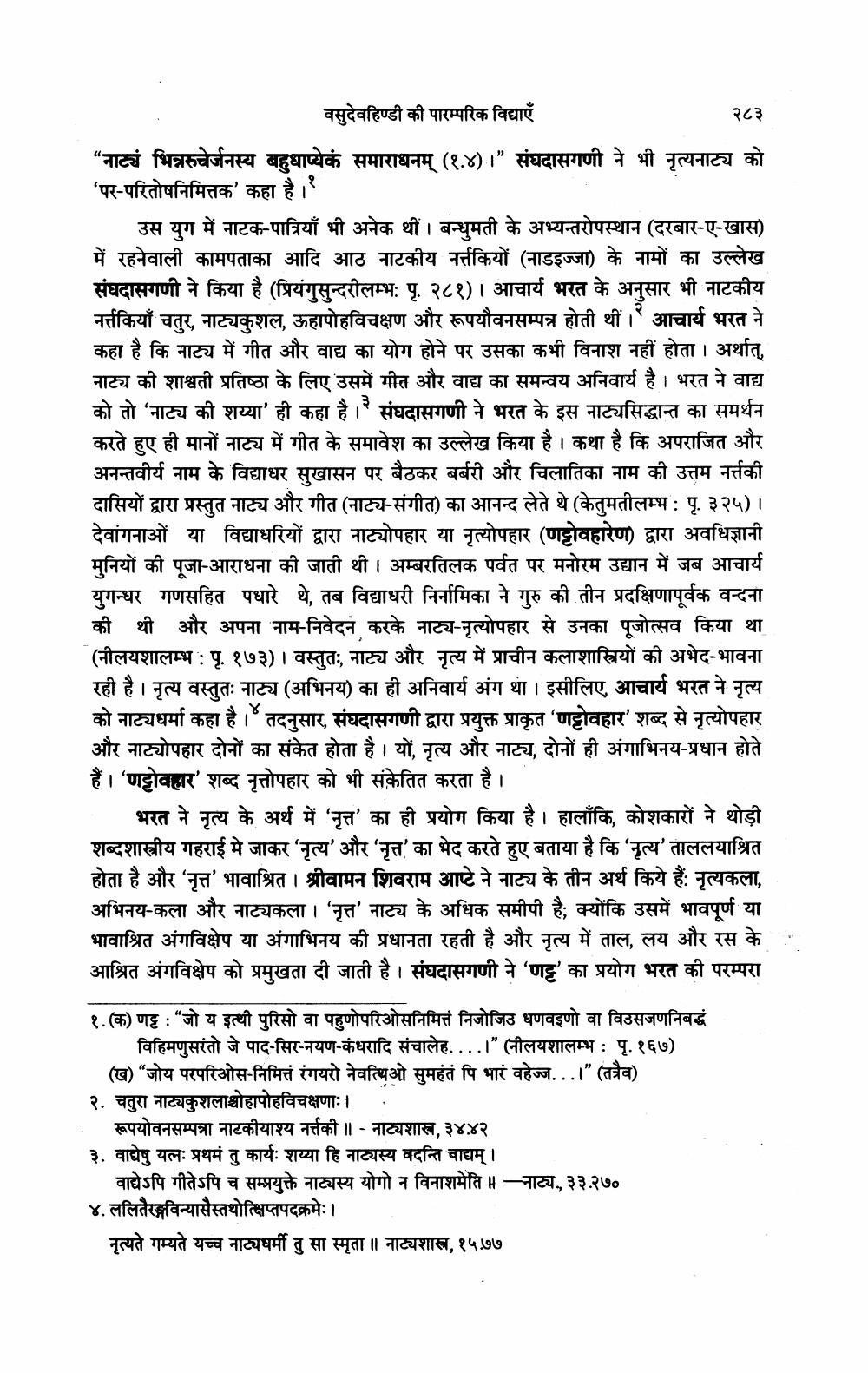________________
वसुदेवहिण्डी की पारम्परिक विद्याएँ
२८३ “नाट्वं भित्ररुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम् (१.४)।" संघदासगणी ने भी नृत्यनाट्य को ‘पर-परितोषनिमित्तक' कहा है।
उस युग में नाटक-पात्रियाँ भी अनेक थीं। बन्धुमती के अभ्यन्तरोपस्थान (दरबार-ए-खास) में रहनेवाली कामपताका आदि आठ नाटकीय नर्तकियों (नाडइज्जा) के नामों का उल्लेख संघदासगणी ने किया है (प्रियंगुसुन्दरीलम्भ: पृ. २८१)। आचार्य भरत के अनुसार भी नाटकीय नर्तकियाँ चतुर, नाट्यकुशल, ऊहापोहविचक्षण और रूपयौवनसम्पन्न होती थीं। आचार्य भरत ने कहा है कि नाट्य में गीत और वाद्य का योग होने पर उसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात्, नाट्य की शाश्वती प्रतिष्ठा के लिए उसमें गीत और वाद्य का समन्वय अनिवार्य है। भरत ने वाद्य को तो 'नाट्य की शय्या' ही कहा है। संघदासगणी ने भरत के इस नाट्यसिद्धान्त का समर्थन करते हुए ही मानों नाट्य में गीत के समावेश का उल्लेख किया है। कथा है कि अपराजित और अनन्तवीर्य नाम के विद्याधर सुखासन पर बैठकर बर्बरी और चिलातिका नाम की उत्तम नर्तकी दासियों द्वारा प्रस्तुत नाट्य और गीत (नाट्य-संगीत) का आनन्द लेते थे (केतुमतीलम्भ : पृ. ३२५) । देवांगनाओं या विद्याधरियों द्वारा नाट्योपहार या नृत्योपहार (णट्टोवहारेण) द्वारा अवधिज्ञानी मुनियों की पूजा-आराधना की जाती थी। अम्बरतिलक पर्वत पर मनोरम उद्यान में जब आचार्य युगन्धर गणसहित पधारे थे, तब विद्याधरी निर्नामिका ने गुरु की तीन प्रदक्षिणापूर्वक वन्दना की थी और अपना नाम-निवेदनं करके नाट्य-नृत्योपहार से उनका पूजोत्सव किया था (नीलयशालम्भ : पृ. १७३)। वस्तुतः, नाट्य और नृत्य में प्राचीन कलाशास्त्रियों की अभेद-भावना रही है । नृत्य वस्तुतः नाट्य (अभिनय) का ही अनिवार्य अंग था । इसीलिए, आचार्य भरत ने नृत्य को नाट्यधर्मा कहा है। तदनुसार, संघदासगणी द्वारा प्रयुक्त प्राकृत ‘णट्टोवहार' शब्द से नृत्योपहार
और नाट्योपहार दोनों का संकेत होता है। यों, नृत्य और नाट्य, दोनों ही अंगाभिनय-प्रधान होते हैं। ‘णट्टोवहार' शब्द नृत्तोपहार को भी संकेतित करता है।
भरत ने नृत्य के अर्थ में 'नृत्त' का ही प्रयोग किया है। हालाँकि, कोशकारों ने थोड़ी शब्दशास्त्रीय गहराई मे जाकर 'नृत्य' और 'नृत्त' का भेद करते हुए बताया है कि 'नृत्य' ताललयाश्रित होता है और 'नृत्त' भावाश्रित । श्रीवामन शिवराम आप्टे ने नाट्य के तीन अर्थ किये हैं: नृत्यकला, अभिनय-कला और नाट्यकला। 'नृत्त' नाट्य के अधिक समीपी है; क्योंकि उसमें भावपूर्ण या भावाश्रित अंगविक्षेप या अंगाभिनय की प्रधानता रहती है और नृत्य में ताल, लय और रस के आश्रित अंगविक्षेप को प्रमुखता दी जाती है। संघदासगणी ने ‘णट्ट' का प्रयोग भरत की परम्परा
१.(क) णट्ट : “जो य इत्थी पुरिसो वा पहुणोपरिओसनिमित्तं निजोजिउ धणवइणो वा विउसजणनिबद्धं
विहिमणुसरंतो जे पाद-सिर-नयण-कंधरादि संचालेह....।” (नीलयशालम्भ : पृ. १६७) (ख) “जोय परपरिओस-निमित्तं रंगयरो नेवत्यिओ सुमहंतं पि भारं वहेज्ज...।" (तत्रैव) २. चतुरा नाट्यकुशलाश्चोहापोहविचक्षणाः। . . रूपयोवनसम्पन्ना नाटकीयाश्य नर्तकी ॥ - नाट्यशास्त्र, ३४.४२ ३. वाद्येषु यत्नः प्रथमं तु कार्यः शय्या हि नाट्यस्य वदन्ति वाद्यम् ।
वाद्येऽपि गीतेऽपि च सम्प्रयुक्ते नाट्यस्य योगो न विनाशमेति । –नाट्य,, ३३.२७० ४. ललितैरङ्गविन्यासैस्तथोत्क्षिप्तपदक्रमेः ।
नृत्यते गम्यते यच्च नाट्यधर्मी तु सा स्मृता ॥ नाट्यशास्त्र, १५.७७