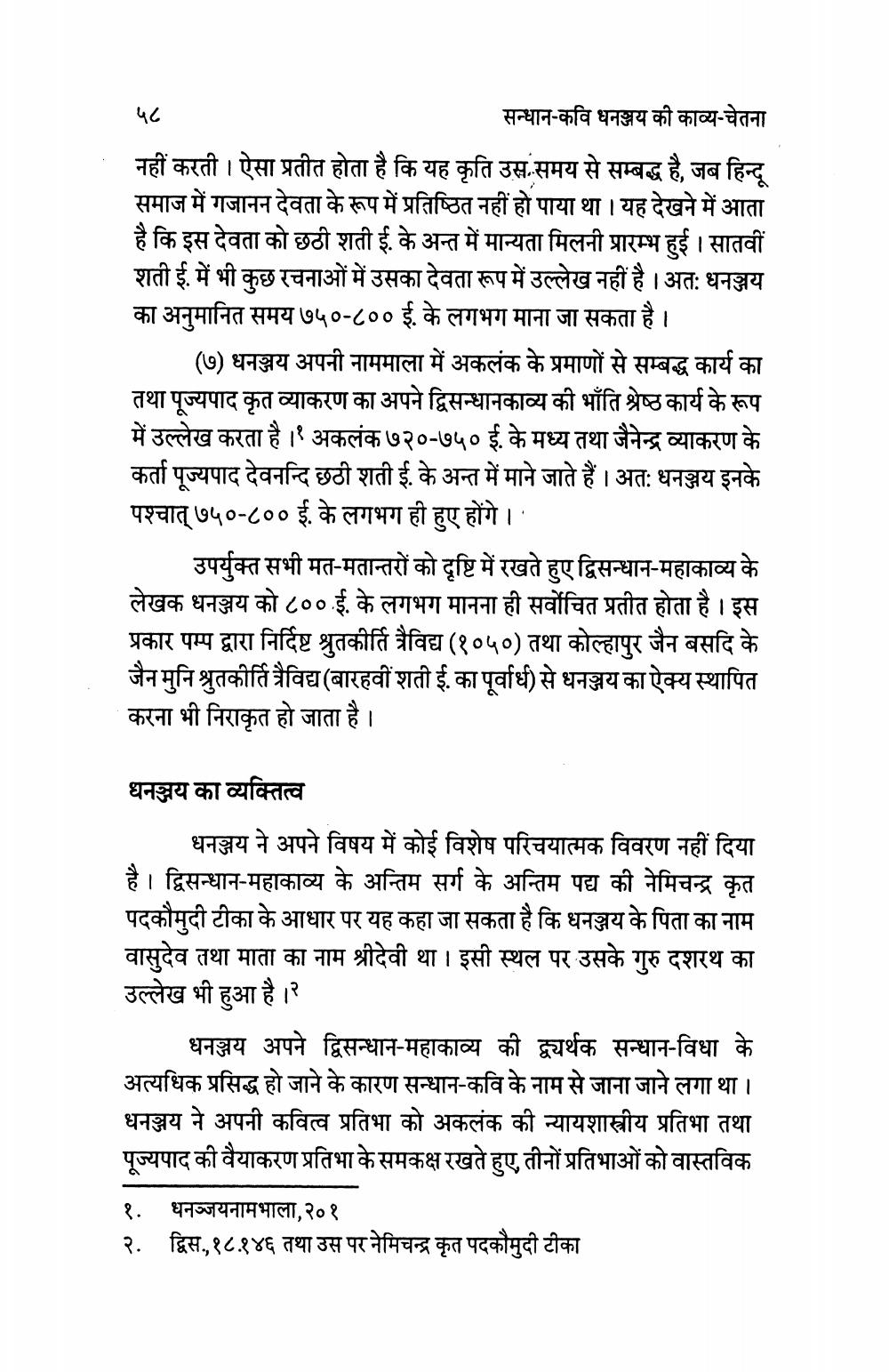________________
सन्धान-कवि धनञ्जय की काव्य-चेतना नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कृति उस समय से सम्बद्ध है, जब हिन्दू समाज में गजानन देवता के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। यह देखने में आता है कि इस देवता को छठी शती ई. के अन्त में मान्यता मिलनी प्रारम्भ हुई । सातवीं शती ई. में भी कुछ रचनाओं में उसका देवता रूप में उल्लेख नहीं है । अत: धनञ्जय का अनुमानित समय ७५०-८०० ई. के लगभग माना जा सकता है।
(७) धनञ्जय अपनी नाममाला में अकलंक के प्रमाणों से सम्बद्ध कार्य का तथा पूज्यपाद कृत व्याकरण का अपने द्विसन्धानकाव्य की भाँति श्रेष्ठ कार्य के रूप में उल्लेख करता है । अकलंक ७२०-७५० ई. के मध्य तथा जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि छठी शती ई. के अन्त में माने जाते हैं । अत: धनञ्जय इनके पश्चात् ७५०-८०० ई. के लगभग ही हुए होंगे।
उपर्युक्त सभी मत-मतान्तरों को दृष्टि में रखते हुए द्विसन्धान-महाकाव्य के लेखक धनञ्जय को ८०० ई. के लगभग मानना ही सर्वाचित प्रतीत होता है । इस प्रकार पम्प द्वारा निर्दिष्ट श्रुतकीर्ति त्रैविद्य (१०५०) तथा कोल्हापुर जैन बसदि के जैन मुनि श्रुतकीर्ति विद्य (बारहवीं शती ई. का पूर्वार्ध) से धनञ्जय का ऐक्य स्थापित करना भी निराकृत हो जाता है।
धनञ्जय का व्यक्तित्व
धनञ्जय ने अपने विषय में कोई विशेष परिचयात्मक विवरण नहीं दिया है। द्विसन्धान-महाकाव्य के अन्तिम सर्ग के अन्तिम पद्य की नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी टीका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धनञ्जय के पिता का नाम वासुदेव तथा माता का नाम श्रीदेवी था। इसी स्थल पर उसके गुरु दशरथ का उल्लेख भी हुआ है।
धनञ्जय अपने द्विसन्धान-महाकाव्य की व्यर्थक सन्धान-विधा के अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण सन्धान-कवि के नाम से जाना जाने लगा था। धनञ्जय ने अपनी कवित्व प्रतिभा को अकलंक की न्यायशास्त्रीय प्रतिभा तथा पूज्यपाद की वैयाकरण प्रतिभा के समकक्ष रखते हुए तीनों प्रतिभाओं को वास्तविक १. धनञ्जयनामभाला,२०१ २. द्विस,१८.१४६ तथा उस पर नेमिचन्द्र कृत पदकौमुदी टीका