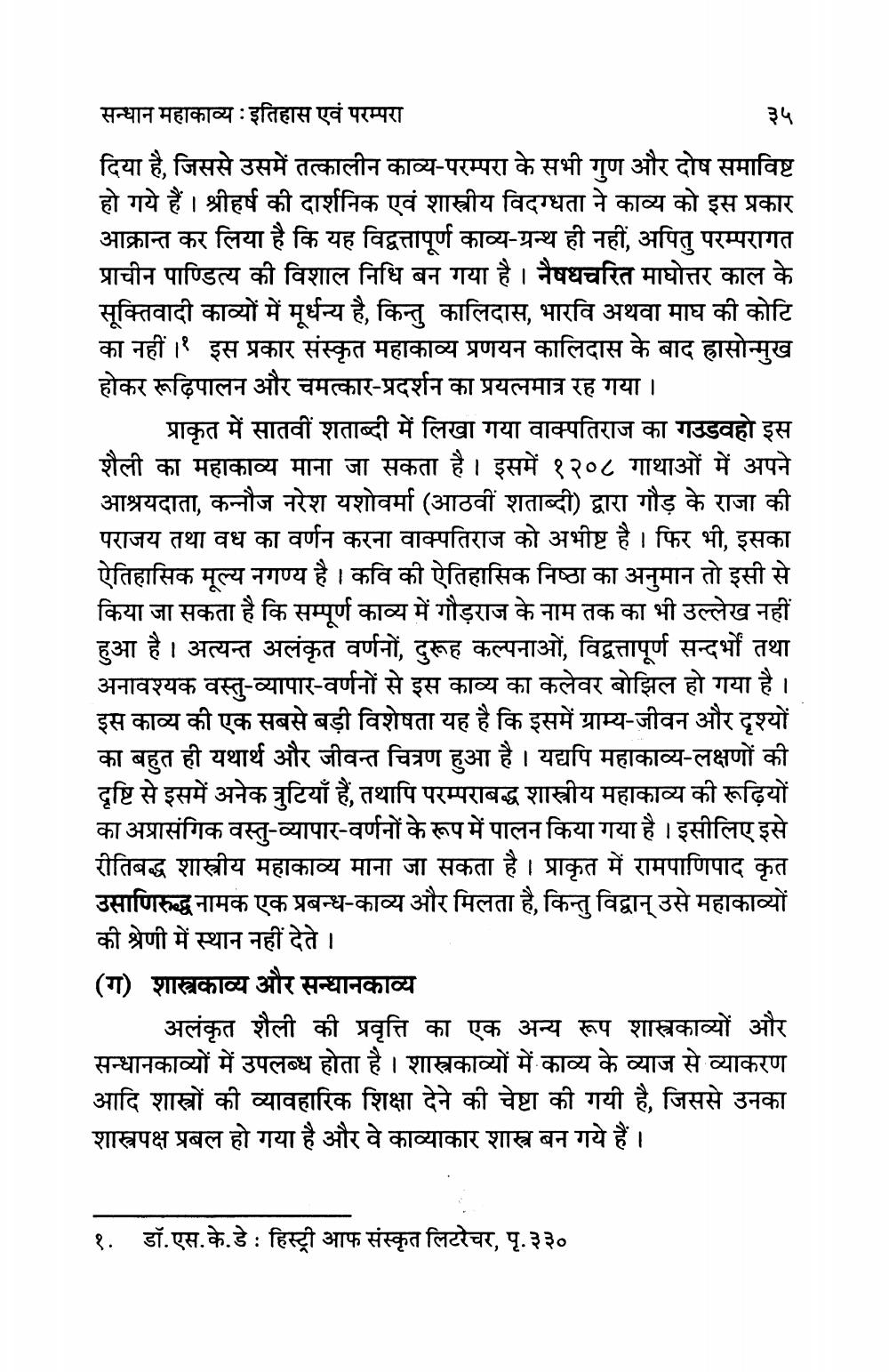________________
सन्धान महाकाव्य इतिहास एवं परम्परा दिया है, जिससे उसमें तत्कालीन काव्य-परम्परा के सभी गुण और दोष समाविष्ट हो गये हैं। श्रीहर्ष की दार्शनिक एवं शास्त्रीय विदग्धता ने काव्य को इस प्रकार आक्रान्त कर लिया है कि यह विद्वत्तापूर्ण काव्य-ग्रन्थ ही नहीं, अपितु परम्परागत प्राचीन पाण्डित्य की विशाल निधि बन गया है । नैषधचरित माघोत्तर काल के सूक्तिवादी काव्यों में मूर्धन्य है, किन्तु कालिदास, भारवि अथवा माघ की कोटि का नहीं। इस प्रकार संस्कृत महाकाव्य प्रणयन कालिदास के बाद ह्रासोन्मुख होकर रूढ़िपालन और चमत्कार-प्रदर्शन का प्रयत्नमात्र रह गया।
प्राकृत में सातवीं शताब्दी में लिखा गया वाक्पतिराज का गउडवहो इस शैली का महाकाव्य माना जा सकता है। इसमें १२०८ गाथाओं में अपने आश्रयदाता, कन्नौज नरेश यशोवर्मा (आठवीं शताब्दी) द्वारा गौड़ के राजा की पराजय तथा वध का वर्णन करना वाक्पतिराज को अभीष्ट है। फिर भी, इसका ऐतिहासिक मूल्य नगण्य है। कवि की ऐतिहासिक निष्ठा का अनुमान तो इसी से किया जा सकता है कि सम्पूर्ण काव्य में गौड़राज के नाम तक का भी उल्लेख नहीं हुआ है । अत्यन्त अलंकृत वर्णनों, दुरूह कल्पनाओं, विद्वत्तापूर्ण सन्दर्भो तथा अनावश्यक वस्तु-व्यापार-वर्णनों से इस काव्य का कलेवर बोझिल हो गया है। इस काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्राम्य-जीवन और दृश्यों का बहुत ही यथार्थ और जीवन्त चित्रण हुआ है। यद्यपि महाकाव्य-लक्षणों की दृष्टि से इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं, तथापि परम्पराबद्ध शास्त्रीय महाकाव्य की रूढ़ियों का अप्रासंगिक वस्तु-व्यापार-वर्णनों के रूप में पालन किया गया है । इसीलिए इसे रीतिबद्ध शास्त्रीय महाकाव्य माना जा सकता है। प्राकृत में रामपाणिपाद कृत उसाणिरुद्ध नामक एक प्रबन्ध-काव्य और मिलता है, किन्तु विद्वान् उसे महाकाव्यों की श्रेणी में स्थान नहीं देते। (ग) शास्त्रकाव्य और सन्धानकाव्य
अलंकृत शैली की प्रवृत्ति का एक अन्य रूप शास्त्रकाव्यों और सन्धानकाव्यों में उपलब्ध होता है। शास्त्रकाव्यों में काव्य के व्याज से व्याकरण आदि शास्त्रों की व्यावहारिक शिक्षा देने की चेष्टा की गयी है, जिससे उनका शास्त्रपक्ष प्रबल हो गया है और वे काव्याकार शास्त्र बन गये हैं।
१. डॉ.एस.के.डे : हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ.३३०