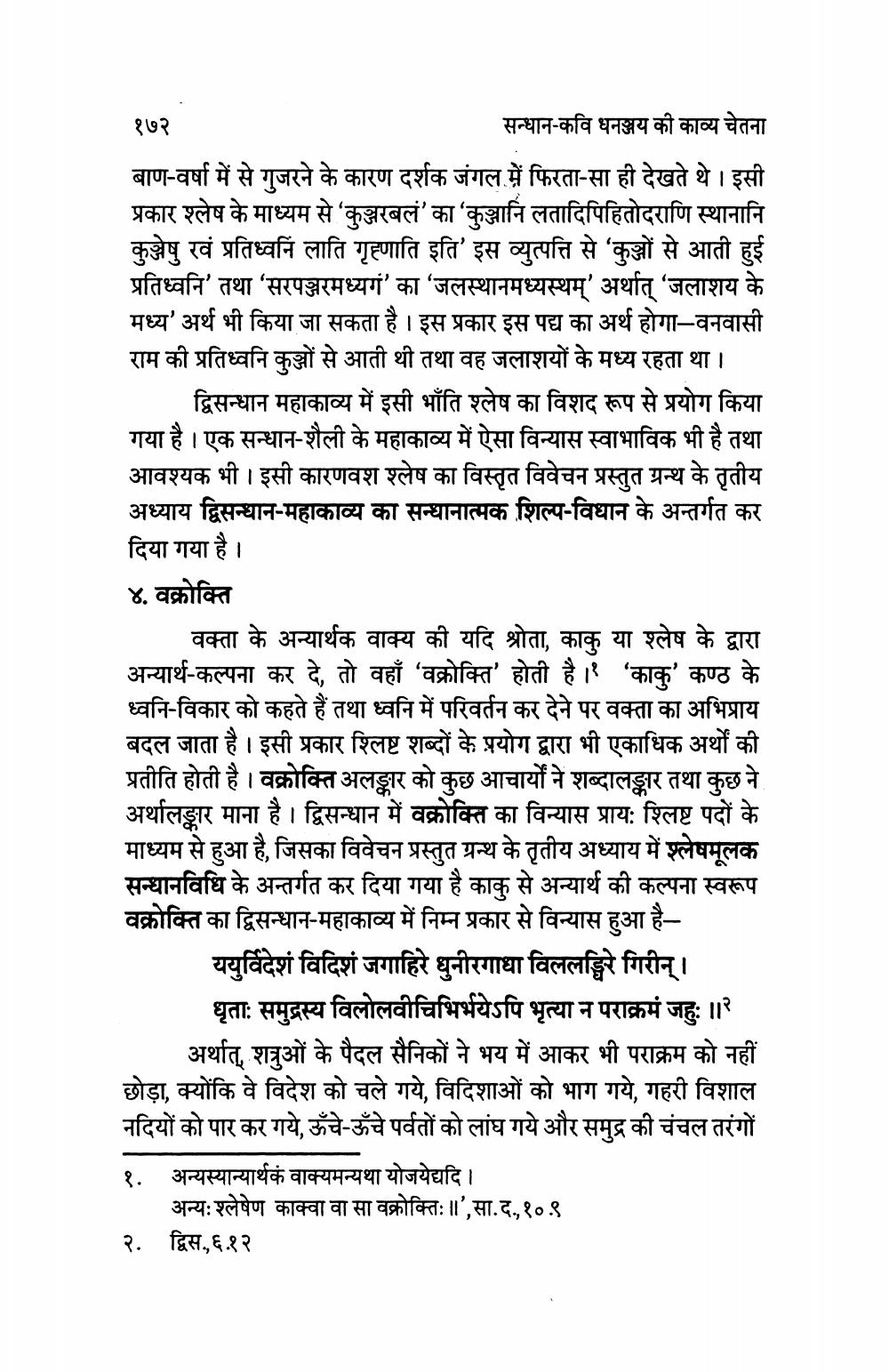________________
१७२
सन्धान-कवि धनञ्जय की काव्य चेतना बाण-वर्षा में से गुजरने के कारण दर्शक जंगल में फिरता-सा ही देखते थे। इसी प्रकार श्लेष के माध्यम से 'कुञ्जरबलं' का 'कुञ्जानि लतादिपिहितोदराणि स्थानानि कुञ्जेषु रवं प्रतिध्वनि लाति गृह्णाति इति' इस व्युत्पत्ति से 'कुञ्जों से आती हुई प्रतिध्वनि' तथा 'सरपञ्जरमध्यगं' का 'जलस्थानमध्यस्थम्' अर्थात् ‘जलाशय के मध्य' अर्थ भी किया जा सकता है । इस प्रकार इस पद्य का अर्थ होगा-वनवासी राम की प्रतिध्वनि कुञ्जों से आती थी तथा वह जलाशयों के मध्य रहता था।।
द्विसन्धान महाकाव्य में इसी भाँति श्लेष का विशद रूप से प्रयोग किया गया है । एक सन्धान-शैली के महाकाव्य में ऐसा विन्यास स्वाभाविक भी है तथा आवश्यक भी। इसी कारणवश श्लेष का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय द्विसन्धान-महाकाव्य का सन्धानात्मक शिल्प-विधान के अन्तर्गत कर दिया गया है। ४. वक्रोक्ति
वक्ता के अन्यार्थक वाक्य की यदि श्रोता, काकु या श्लेष के द्वारा अन्यार्थ-कल्पना कर दे, तो वहाँ 'वक्रोक्ति' होती है। 'काकु' कण्ठ के ध्वनि-विकार को कहते हैं तथा ध्वनि में परिवर्तन कर देने पर वक्ता का अभिप्राय बदल जाता है । इसी प्रकार श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग द्वारा भी एकाधिक अर्थों की प्रतीति होती है । वक्रोक्ति अलङ्कार को कुछ आचार्यों ने शब्दालङ्कार तथा कुछ ने अर्थालङ्कार माना है। द्विसन्धान में वक्रोक्ति का विन्यास प्राय: श्लिष्ट पदों के माध्यम से हुआ है, जिसका विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में श्लेषमूलक सन्धानविधि के अन्तर्गत कर दिया गया है काकु से अन्यार्थ की कल्पना स्वरूप वक्रोक्ति का द्विसन्धान-महाकाव्य में निम्न प्रकार से विन्यास हुआ है
ययुर्विदेशं विदिशं जगाहिरे धुनीरगाधा विललविरे गिरीन् ।
धृता: समुद्रस्य विलोलवीचिभिर्भयेऽपि भृत्या न पराक्रमं जहुः ।।
अर्थात्, शत्रुओं के पैदल सैनिकों ने भय में आकर भी पराक्रम को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे विदेश को चले गये, विदिशाओं को भाग गये, गहरी विशाल नदियों को पार कर गये, ऊँचे-ऊँचे पर्वतों को लांघ गये और समुद्र की चंचल तरंगों १. अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि ।
अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिः ॥',सा.द.१०.९ २. द्विस,६.१२